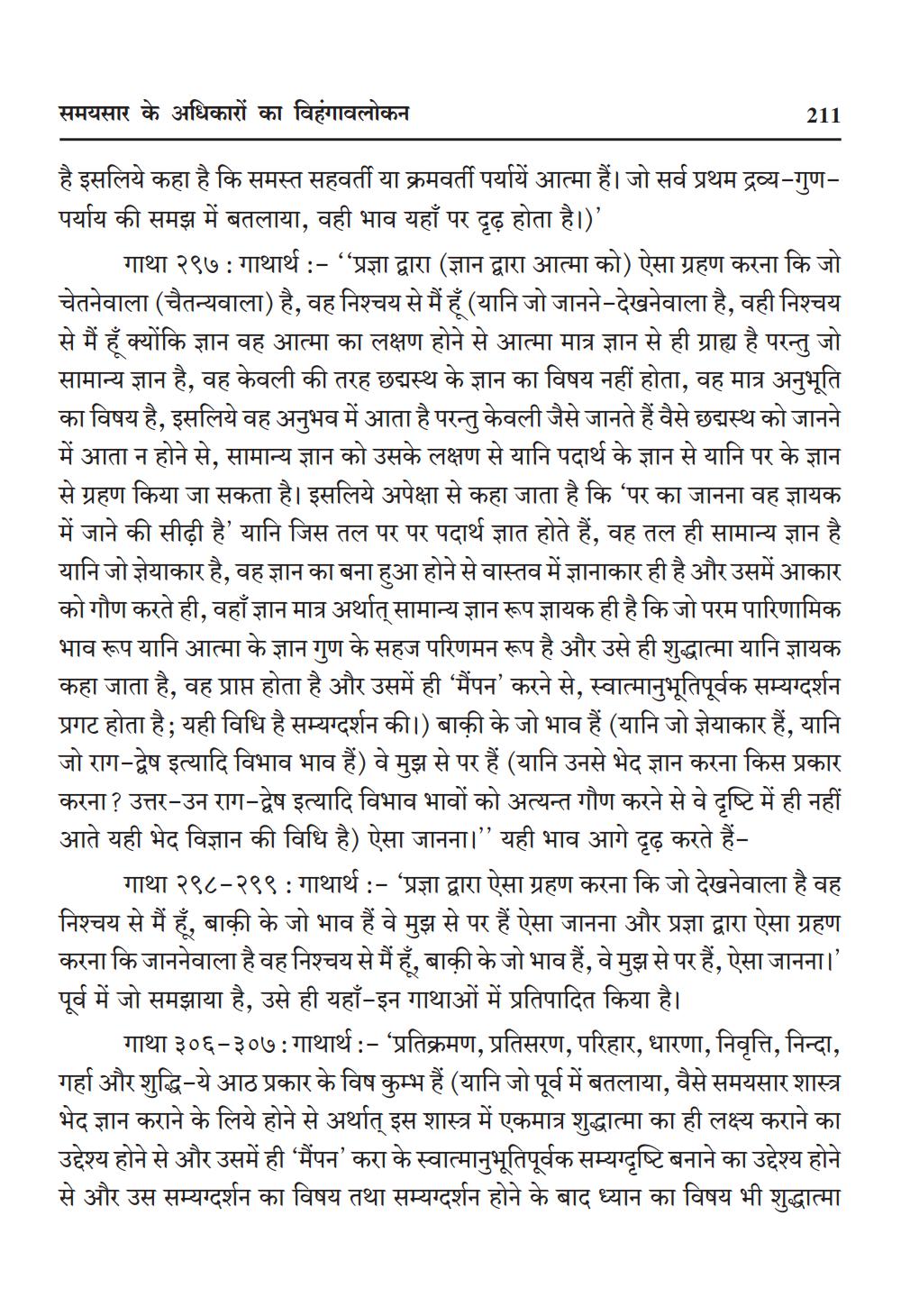________________
समयसार के अधिकारों का विहंगावलोकन
211
है इसलिये कहा है कि समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्यायें आत्मा हैं। जो सर्व प्रथम द्रव्य-गुणपर्याय की समझ में बतलाया, वही भाव यहाँ पर दृढ़ होता है।)'
गाथा २९७ : गाथार्थ :- “प्रज्ञा द्वारा (ज्ञान द्वारा आत्मा को) ऐसा ग्रहण करना कि जो चेतनेवाला (चैतन्यवाला) है, वह निश्चय से मैं हँ (यानि जो जानने-देखनेवाला है, वही निश्चय से मैं हूँ क्योंकि ज्ञान वह आत्मा का लक्षण होने से आत्मा मात्र ज्ञान से ही ग्राह्य है परन्तु जो सामान्य ज्ञान है, वह केवली की तरह छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं होता, वह मात्र अनुभूति का विषय है, इसलिये वह अनुभव में आता है परन्तु केवली जैसे जानते हैं वैसे छद्मस्थ को जानने में आता न होने से, सामान्य ज्ञान को उसके लक्षण से यानि पदार्थ के ज्ञान से यानि पर के ज्ञान से ग्रहण किया जा सकता है। इसलिये अपेक्षा से कहा जाता है कि ‘पर का जानना वह ज्ञायक में जाने की सीढ़ी है' यानि जिस तल पर पर पदार्थ ज्ञात होते हैं, वह तल ही सामान्य ज्ञान है यानि जो ज्ञेयाकार है, वह ज्ञान का बना हुआ होने से वास्तव में ज्ञानाकार ही है और उसमें आकार को गौण करते ही, वहाँ ज्ञान मात्र अर्थात् सामान्य ज्ञान रूप ज्ञायक ही है कि जो परम पारिणामिक भाव रूप यानि आत्मा के ज्ञान गुण के सहज परिणमन रूप है और उसे ही शुद्धात्मा यानि ज्ञायक कहा जाता है, वह प्राप्त होता है और उसमें ही 'मैंपन' करने से, स्वात्मानुभूतिपूर्वक सम्यग्दर्शन प्रगट होता है; यही विधि है सम्यग्दर्शन की।) बाक़ी के जो भाव हैं (यानि जो ज्ञेयाकार हैं, यानि जो राग-द्वेष इत्यादि विभाव भाव हैं) वे मुझ से पर हैं (यानि उनसे भेद ज्ञान करना किस प्रकार करना? उत्तर-उन राग-द्वेष इत्यादि विभाव भावों को अत्यन्त गौण करने से वे दृष्टि में ही नहीं आते यही भेद विज्ञान की विधि है) ऐसा जानना।” यही भाव आगे दृढ़ करते हैं
गाथा २९८-२९९ : गाथार्थ :- 'प्रज्ञा द्वारा ऐसा ग्रहण करना कि जो देखनेवाला है वह निश्चय से मैं हूँ, बाकी के जो भाव हैं वे मुझ से पर हैं ऐसा जानना और प्रज्ञा द्वारा ऐसा ग्रहण करना कि जाननेवाला है वह निश्चय से मैं हूँ, बाक़ी के जो भाव हैं, वे मुझ से पर हैं, ऐसा जानना।' पूर्व में जो समझाया है, उसे ही यहाँ-इन गाथाओं में प्रतिपादित किया है।
गाथा ३०६-३०७ : गाथार्थ :- 'प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि-ये आठ प्रकार के विष कुम्भ हैं (यानि जो पूर्व में बतलाया, वैसे समयसार शास्त्र भेद ज्ञान कराने के लिये होने से अर्थात् इस शास्त्र में एकमात्र शुद्धात्मा का ही लक्ष्य कराने का उद्देश्य होने से और उसमें ही 'मैंपन' करा के स्वात्मानुभूतिपूर्वक सम्यग्दृष्टि बनाने का उद्देश्य होने से और उस सम्यग्दर्शन का विषय तथा सम्यग्दर्शन होने के बाद ध्यान का विषय भी शुद्धात्मा