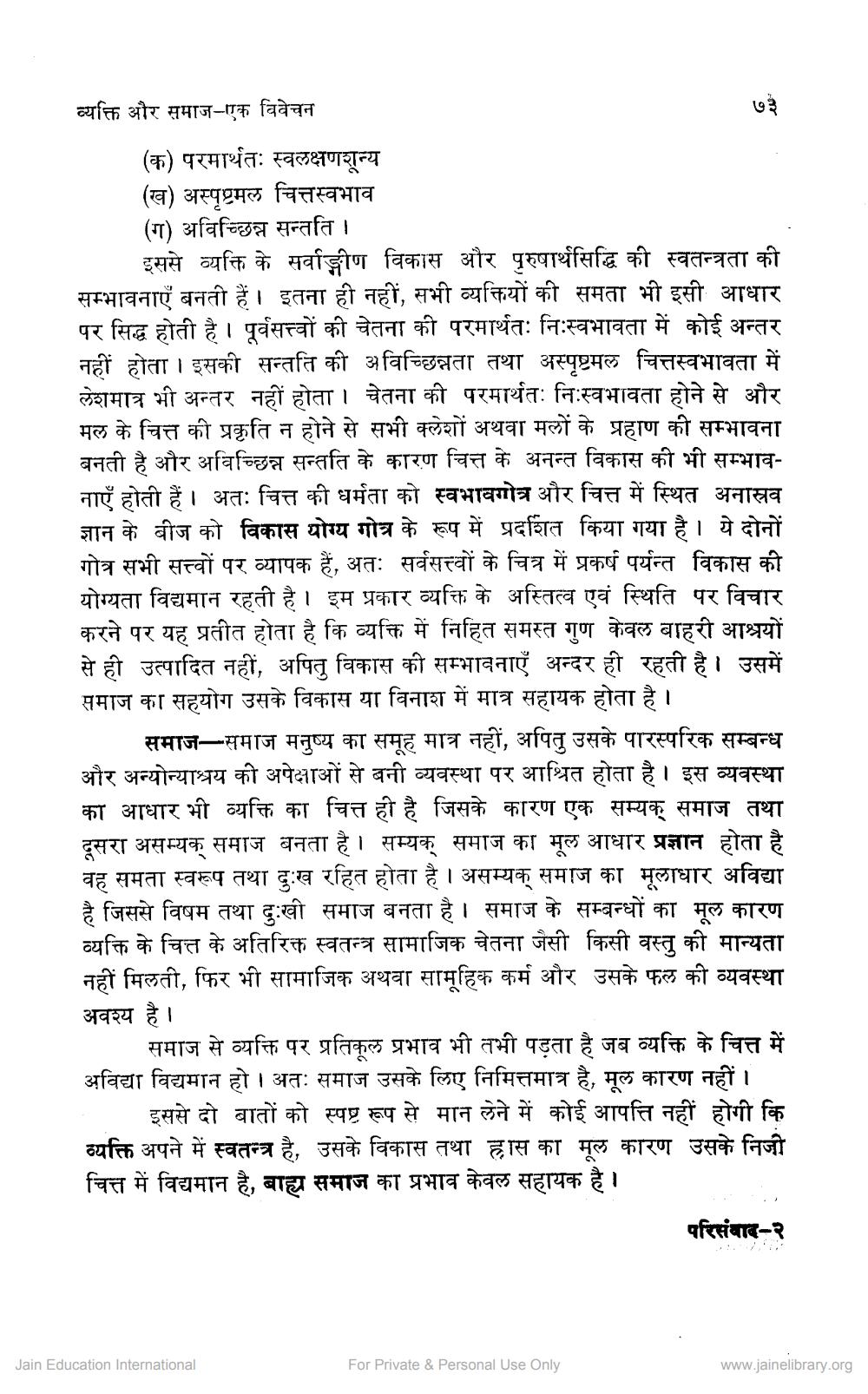________________
व्यक्ति और समाज-एक विवेचन
(क) परमार्थतः स्वलक्षणशून्य (ख) अस्पृष्टमल चित्तस्वभाव (ग) अविच्छिन्न सन्तति ।
इससे व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास और पुरुषार्थसिद्धि की स्वतन्त्रता की सम्भावनाएँ बनती हैं। इतना ही नहीं, सभी व्यक्तियों की समता भी इसी आधार पर सिद्ध होती है। पूर्वसत्त्वों की चेतना की परमार्थतः निःस्वभावता में कोई अन्तर नहीं होता। इसकी सन्तति की अविच्छिन्नता तथा अस्पृष्टमल चित्तस्वभावता में लेशमात्र भी अन्तर नहीं होता। चेतना की परमार्थतः निःस्वभावता होने से और मल के चित्त की प्रकृति न होने से सभी क्लेशों अथवा मलों के प्रहाण की सम्भावना बनती है और अविच्छिन्न सन्तति के कारण चित्त के अनन्त विकास की भी सम्भावनाएँ होती हैं। अतः चित्त की धर्मता को स्वभावगोत्र और चित्त में स्थित अनास्रव ज्ञान के बीज को विकास योग्य गोत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों गोत्र सभी सत्त्वों पर व्यापक हैं, अतः सर्वसत्त्वों के चित्र में प्रकर्ष पर्यन्त विकास की योग्यता विद्यमान रहती है। इम प्रकार व्यक्ति के अस्तित्व एवं स्थिति पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति में निहित समस्त गुण केवल बाहरी आश्रयों से ही उत्पादित नहीं, अपितु विकास की सम्भावनाएँ अन्दर ही रहती है। उसमें समाज का सहयोग उसके विकास या विनाश में मात्र सहायक होता है।
समाज-समाज मनुष्य का समूह मात्र नहीं, अपितु उसके पारस्परिक सम्बन्ध और अन्योन्याश्रय की अपेक्षाओं से बनी व्यवस्था पर आश्रित होता है। इस व्यवस्था का आधार भी व्यक्ति का चित्त ही है जिसके कारण एक सम्यक् समाज तथा दूसरा असम्यक् समाज बनता है। सम्यक् समाज का मूल आधार प्रज्ञान होता है वह समता स्वरूप तथा दुःख रहित होता है । असम्यक् समाज का मूलाधार अविद्या है जिससे विषम तथा दुःखी समाज बनता है। समाज के सम्बन्धों का मूल कारण व्यक्ति के चित्त के अतिरिक्त स्वतन्त्र सामाजिक चेतना जैसी किसी वस्तु की मान्यता नहीं मिलती, फिर भी सामाजिक अथवा सामूहिक कर्म और उसके फल की व्यवस्था अवश्य है।
समाज से व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव भी तभी पड़ता है जब व्यक्ति के चित्त में अविद्या विद्यमान हो । अतः समाज उसके लिए निमित्तमात्र है, मूल कारण नहीं।
इससे दो बातों को स्पष्ट रूप से मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि व्यक्ति अपने में स्वतन्त्र है, उसके विकास तथा ह्रास का मूल कारण उसके निजी चित्त में विद्यमान है, बाह्य समाज का प्रभाव केवल सहायक है।
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org