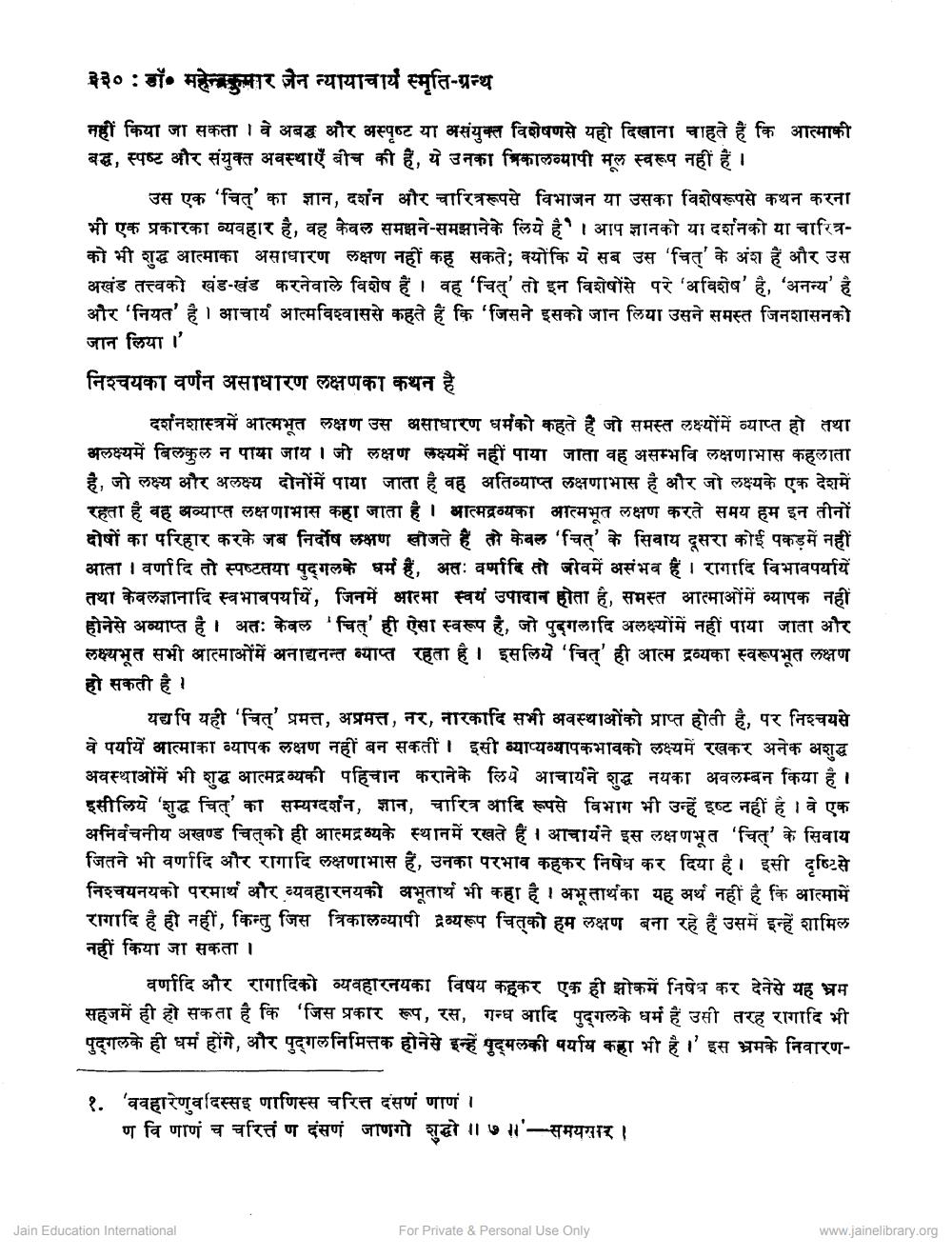________________
३३० : डॉ. महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
नहीं किया जा सकता । वे अबद्ध और अस्पृष्ट या असंयुक्त विशेषणसे यहो दिखाना चाहते हैं कि आत्माकी बद्ध, स्पष्ट और संयुक्त अवस्थाएँ बीच की हैं, ये उनका त्रिकालव्यापी मूल स्वरूप नहीं हैं।
उस एक 'चित्' का ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपसे विभाजन या उसका विशेषरूपसे कथन करना भी एक प्रकारका व्यवहार है, वह केवल समझने-समझानेके लिये है। आप ज्ञानको या दर्शनको या चारित्रको भी शुद्ध आत्माका असाधारण लक्षण नहीं कह सकते; क्योंकि ये सब उस 'चित्' के अंश हैं और उस अखंड तत्त्वको खंड-खंड करनेवाले विशेष है । वह 'चित्' तो इन विशेषोंसे परे 'अविशेष' है, 'अनन्य' है और 'नियत' है । आचार्य आत्मविश्वाससे कहते हैं कि 'जिसने इसको जान लिया उसने समस्त जिनशासनको जान लिया।' निश्चयका वर्णन असाधारण लक्षणका कथन है
दर्शनशास्त्रमें आत्मभूत लक्षण उस असाधारण धर्मको कहते है जो समस्त लक्ष्योंमें व्याप्त हो तथा अलक्ष्यमें बिलकुल न पाया जाय । जो लक्षण लक्ष्यमें नहीं पाया जाता वह असम्भवि लक्षणाभास कहलाता है, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनोंमें पाया जाता है वह अतिव्याप्त लक्षणाभास है और जो लक्ष्यके एक देशमें रहता है वह अव्याप्त लक्षणाभास कहा जाता है । आत्मद्रव्यका आत्मभूत लक्षण करते समय हम इन तीनों दोषों का परिहार करके जब निर्दोष लक्षण खोजते है तो केवल 'चित्' के सिवाय दूसरा कोई पकड़में नहीं आता । वर्णादि तो स्पष्टतया पुद्गलके धर्म है, अतः वर्णादि तो जीवमें असंभव है। रागादि विभावपर्याय तथा केवलज्ञानादि स्वभावपर्यायें, जिनमें भात्मा स्वयं उपादान होता है, समस्त आत्माओंमें व्यापक नहीं होनेसे अव्याप्त है। अतः केवल 'चित्' ही ऐसा स्वरूप है, जो पुद्गलादि अलक्ष्योंमें नहीं पाया जाता और लक्ष्यभूत सभी आत्माओंमें अनाद्यनन्त ब्याप्त रहता है। इसलिये 'चित्' ही आत्म द्रव्यका स्वरूपभूत लक्षण हो सकती है।
यद्यपि यही 'चित' प्रमत्त, अप्रमत्त, नर, नारकादि सभी अवस्थाओंको प्राप्त होती है, पर निश्चयसे वे पर्याय आत्माका व्यापक लक्षण नहीं बन सकतीं। इसी व्याप्यव्यापकभावको लक्ष्यमें रखकर अनेक अशुद्ध अवस्थाओंमें भी शुद्ध आत्मद्रव्यको पहिचान कराने के लिये आचार्यने शुद्ध नयका अवलम्बन किया है। इसीलिये 'शुद्ध चित्' का सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि रूपसे विभाग भी उन्हें इष्ट नहीं है । वे एक अनिर्वचनीय अखण्ड चित्को ही आत्मद्रव्यके स्थानमें रखते हैं । आचार्यने इस लक्षणभूत 'चित्' के सिवाय जितने भी वर्णादि और रागादि लक्षणाभास हैं, उनका परभाव कहकर निषेध कर दिया है। इसी दृष्टिसे निश्चयनयको परमार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ भी कहा है । अभूतार्थका यह अर्थ नहीं है कि आत्मामें रागादि है ही नहीं, किन्तु जिस त्रिकालव्यापी द्रव्यरूप चितको हम लक्षण बना रहे हैं उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता।
वर्णादि और रागादिको व्यवहारनयका विषय कहकर एक ही झोकमें निषेध कर देनेसे यह भ्रम सहजमें ही हो सकता है कि 'जिस प्रकार रूप, रस, गन्ध आदि पुद्गलके धर्म है उसी तरह रागादि भी पदगलके ही धर्म होंगे, और पुद्गलनिमित्तक होनेसे इन्हें पदमलकी पर्याय कहा भी है।' इस भ्रमके निवारण
१. 'ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्त दसणं णाणं ।
ण वि णाणं च चरित्तं ण दंसणं जाणगो शुद्धो ॥ ७॥'-समयसार ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org