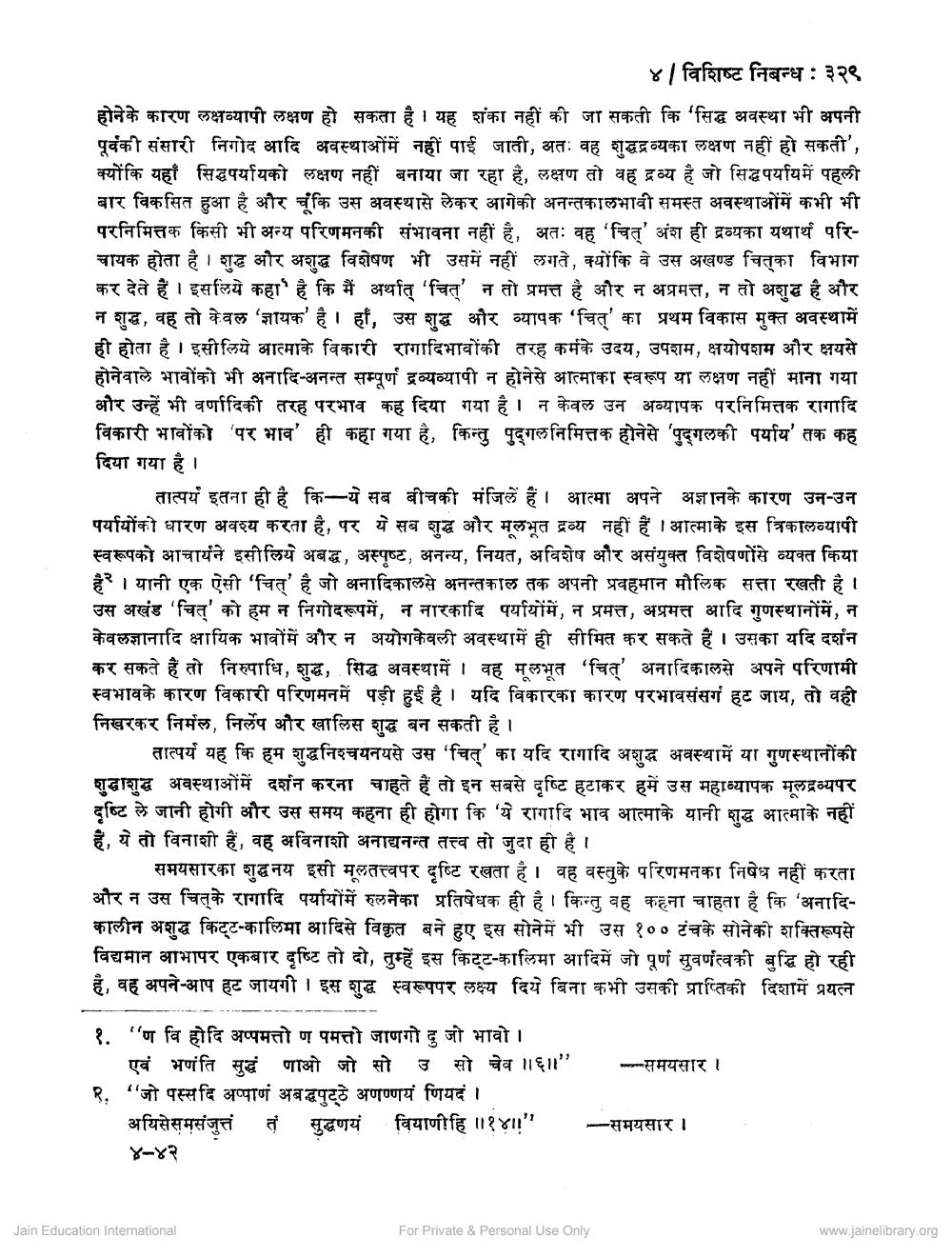________________
४/ विशिष्ट निबन्ध : ३२९
होने के कारण लक्षव्यापी लक्षण हो सकता है । यह शंका नहीं की जा सकती कि "सिद्ध अवस्था भी अपनी पूर्वकी संसारी निगोद आदि अवस्थाओंमें नहीं पाई जाती, अतः वह शुद्धद्रव्यका लक्षण नहीं हो सकती', क्योंकि यहाँ सिद्धपर्यायको लक्षण नहीं बनाया जा रहा है, लक्षण तो वह द्रव्य है जो सिद्ध पर्यायमें पहली बार विकसित हुआ है और चूंकि उस अवस्थासे लेकर आगेकी अनन्तकालभावी समस्त अवस्थाओंमें कभी भी परनिमित्तक किसी भी अन्य परिणमनकी संभावना नहीं है, अतः वह 'चित' अंश ही द्रव्यका यथार्थ परिचायक होता है । शुद्ध और अशुद्ध विशेषण भी उसमें नहीं लगते, क्योंकि वे उस अखण्ड चित्का विभाग कर देते हैं । इसलिये कहा है कि मैं अर्थात् 'चित्' न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त, न तो अशुद्ध है और न शुद्ध, वह तो केवल 'ज्ञायक' है । हाँ, उस शुद्ध और व्यापक 'चित्' का प्रथम विकास मुक्त अवस्थामें ही होता है । इसीलिये आत्माके विकारी रागादिभावोंकी तरह कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षयसे होनेवाले भावोंको भी अनादि-अनन्त सम्पूर्ण द्रव्यव्यापी न होनेसे आत्माका स्वरूप या लक्षण नहीं माना गया
और उन्हें भी वर्णादिकी तरह परभाव कह दिया गया है। न केवल उन अव्यापक परनिमित्तक रागादि विकारी भावोंको पर भाव' ही कहा गया है, किन्तु पुद्गलनिमित्तक होनेसे 'पुद्गलकी पर्याय' तक कह दिया गया है।
तात्पर्य इतना ही है कि ये सब बीचकी मंजिलें हैं। आत्मा अपने अज्ञानके कारण उन-उन पर्यायोंको धारण अवश्य करता है, पर ये सब शद्ध और मलभत द्रव्य नहीं है । आत्माके इस स्वरूपको आचार्यने इसीलिये अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त विशेषणोंसे व्यक्त किया है । यानी एक ऐसी 'चित्' है जो अनादिकालसे अनन्तकाल तक अपनी प्रवहमान मौलिक सत्ता रखती है। उस अखंड 'चित्' को हम न निगोदरूपमें, न नारकादि पर्यायोंमें, न प्रमत्त, अप्रमत्त आदि गुणस्थानोंमें, न केवलज्ञानादि क्षायिक भावोंमें और न अयोगकेवली अवस्थामें ही सीमित कर सकते हैं । उसका यदि दर्शन कर सकते है तो निरुपाधि, शद्ध, सिद्ध अवस्थामें । वह मलभत 'चित' अनादिकालसे अपने परिणामी स्वभावके कारण विकारी परिणमनमें पड़ी हुई है। यदि विकारका कारण परभावसंसर्ग हट जाय, तो वही निखरकर निर्मल, निर्लेप और खालिस शुद्ध बन सकती है।
तात्पर्य यह कि हम शुद्धनिश्चयनयसे उस 'चित्' का यदि रागादि अशुद्ध अवस्थामें या गणस्थानोंकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाओं में दर्शन करना चाहते हैं तो इन सबसे दृष्टि हटाकर हमें उस महाव्यापक मूलद्रव्यपर दृष्टि ले जानी होगी और उस समय कहना ही होगा कि 'ये रागादि भाव आत्माके यानी शद्ध आत्माके नहीं है, ये तो विनाशी हैं, वह अविनाशी अनाद्यनन्त तत्त्व तो जुदा ही है।
समयसारका शुद्ध नय इसी मूलतत्त्वपर दृष्टि रखता है। वह वस्तुके परिणमनका निषेध नहीं करता और न उस चित्के रागादि पर्यायोंमें रुलनेका प्रतिषेधक ही है। किन्तु वह कहना चाहता है कि 'अनादिकालीन अशुद्ध किट्ट-कालिमा आदिसे विकृत बने हए इस सोने में भी उस १०० टंचके सोनेकी शक्तिरूपसे विद्यमान आभापर एकबार दृष्टि तो दो, तुम्हें इस किट्ट-कालिमा आदिमें जो पूर्ण सुवर्णत्वकी बुद्धि हो रही है, वह अपने-आप हट जायगी। इस शुद्ध स्वरूपपर लक्ष्य दिये बिना कभी उसकी प्राप्तिको दिशामें प्रयत्न
-समयसार।
१. "ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो।
एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥६॥" २. "जो पस्स दि अप्पाणं अबद्धपुछे अणण्णयं णियदं ।
अयिसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥"
-समयसार।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org