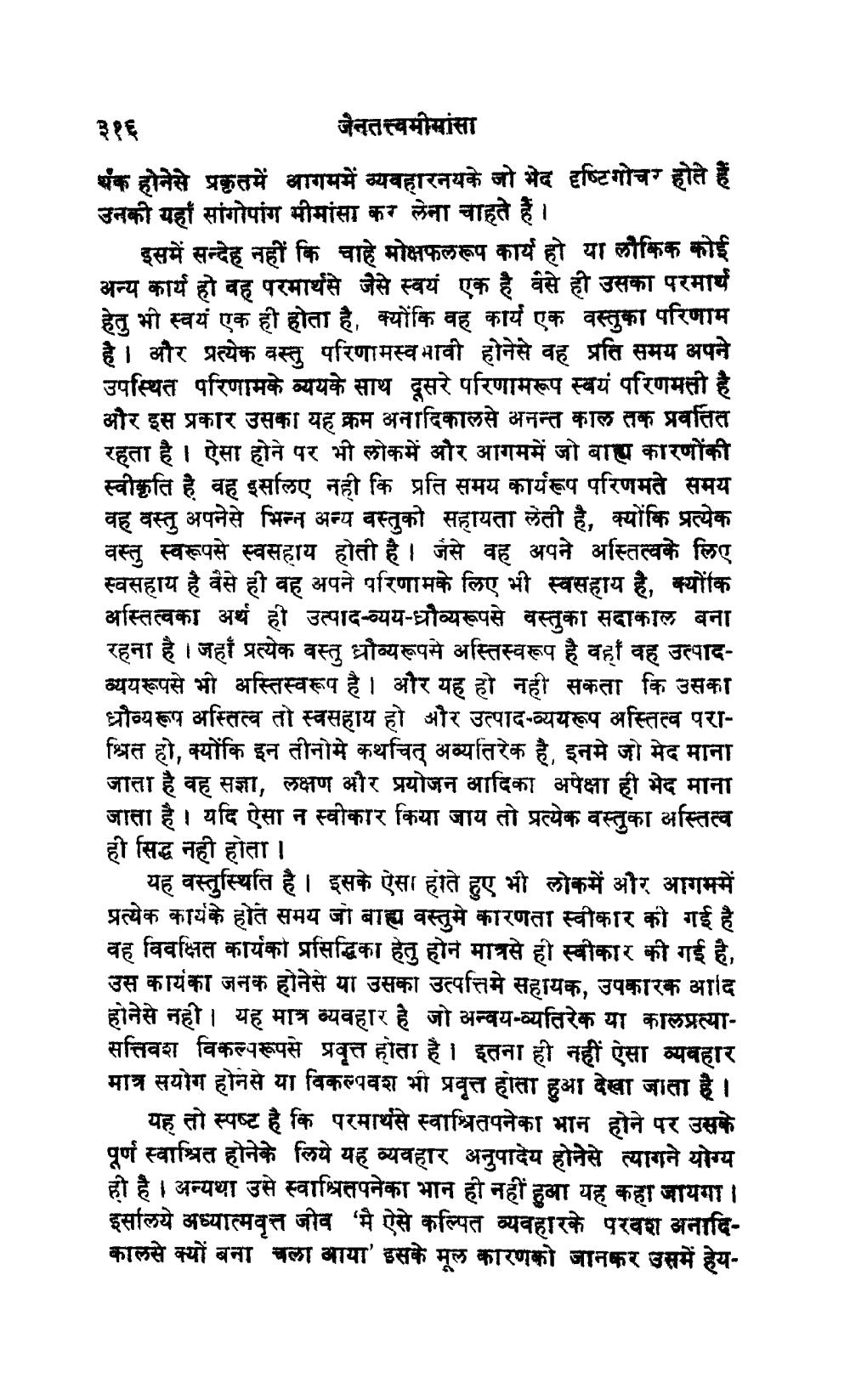________________
३१६
जैनतत्त्वमीमांसा थंक होनेसे प्रकृतमें आगममें व्यवहारनयके जो भेद दृष्टिगोचर होते हैं उनकी यहाँ सांगोपांग मीमांसा कर लेना चाहते हैं।
इसमें सन्देह नहीं कि चाहे मोक्षफलरूप कार्य हो या लौकिक कोई अन्य कार्य हो वह परमार्थसे जैसे स्वयं एक है वैसे ही उसका परमार्थ हेतु भी स्वयं एक ही होता है, क्योंकि वह कार्य एक वस्तुका परिणाम है। और प्रत्येक वस्तु परिणामस्वभावी होनेसे वह प्रति समय अपने उपस्थित परिणामके व्ययके साथ दूसरे परिणामरूप स्वयं परिणमती है और इस प्रकार उसका यह क्रम अनादिकालसे अनन्त काल तक प्रवर्तित रहता है । ऐसा होने पर भी लोकमें और आगममें जो बाह्य कारणोंकी स्वीकृति है वह इसलिए नही कि प्रति समय कार्यरूप परिणमते समय वह वस्तु अपनेसे भिन्न अन्य वस्तुको सहायता लेती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वरूपसे स्वसहाय होती है। जैसे वह अपने अस्तित्वके लिए स्वसहाय है वैसे ही वह अपने परिणामके लिए भी स्वसहाय है, क्योंकि अस्तित्वका अर्थ ही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूपसे वस्तुका सदाकाल बना रहना है। जहाँ प्रत्येक वस्तु ध्रौव्यरूपसे अस्तिस्वरूप है वहाँ वह उत्पादव्ययरूपसे भी अस्तिस्वरूप है। और यह हो नहीं सकता कि उसका ध्रौव्यरूप अस्तित्व तो स्वसहाय हो और उत्पाद-व्ययरूप अस्तित्व पराश्रित हो, क्योंकि इन तीनोमे कचित् अव्यतिरेक है, इनमे जो मेद माना जाता है वह सज्ञा, लक्षण और प्रयोजन आदिका अपेक्षा ही भेद माना जाता है। यदि ऐसा न स्वीकार किया जाय तो प्रत्येक वस्तुका अस्तित्व ही सिद्ध नही होता।
यह वस्तुस्थिति है। इसके ऐसा होते हुए भी लोकमें और आगममें प्रत्येक कार्यके होत समय जो बाह्य वस्तुमे कारणता स्वीकार की गई है वह विवक्षित कार्यको प्रसिद्धिका हेतु होने मात्रसे ही स्वीकार की गई है, उस कार्यका जनक होनेसे या उसका उत्पत्तिमे सहायक, उपकारक आदि होनेसे नहीं। यह मात्र व्यवहार है जो अन्वय-व्यतिरेक या कालप्रत्यासत्तिवश विकल्परूपसे प्रवृत्त होता है। इतना ही नहीं ऐसा व्यवहार मात्र सयोग होनसे या विकल्पवश भी प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है। ___ यह तो स्पष्ट है कि परमार्थसे स्वाश्रितपनेका भान होने पर उसके पूर्ण स्वाश्रित होनेके लिये यह व्यवहार अनुपादेय होनेसे त्यागने योग्य ही है । अन्यथा उसे स्वाश्रितपनेका भान ही नहीं हुआ यह कहा जायगा। इसलिये अध्यात्मवृत्त जीव 'मैं ऐसे कल्पित व्यवहारके परवश अनादिकालसे क्यों बना चला आया' इसके मूल कारणको जानकर उसमें हेय