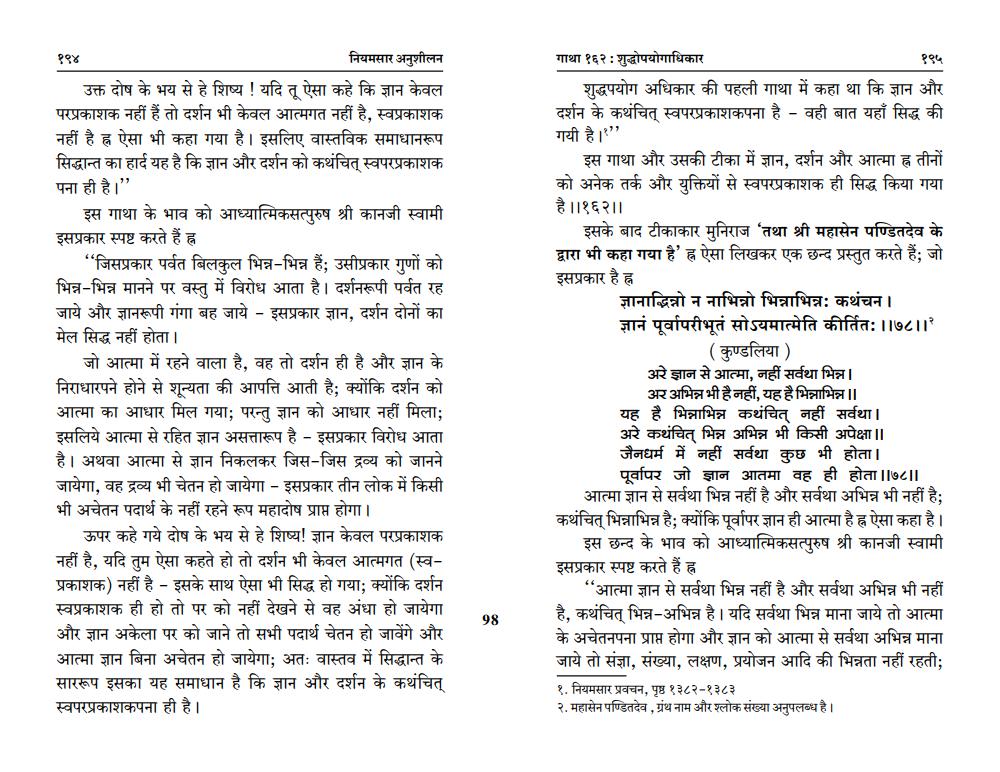________________
नियमसार अनुशीलन
उक्त दोष के भय से हे शिष्य ! यदि तू ऐसा कहे कि ज्ञान केवल परप्रकाशक नहीं हैं तो दर्शन भी केवल आत्मगत नहीं है, स्वप्रकाशक नहीं है ह्र ऐसा भी कहा गया है। इसलिए वास्तविक समाधानरूप सिद्धान्त का हार्द यह है कि ज्ञान और दर्शन को कथंचित् स्वपरप्रकाशक पना ही है।"
१९४
इस गाथा के भाव को आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
" जिसप्रकार पर्वत बिलकुल भिन्न भिन्न हैं; उसीप्रकार गुणों को भिन्न-भिन्न मानने पर वस्तु में विरोध आता है। दर्शनरूपी पर्वत रह जाये और ज्ञानरूपी गंगा बह जाये इसप्रकार ज्ञान, दर्शन दोनों का मेल सिद्ध नहीं होता ।
-
जो आत्मा में रहने वाला है, वह तो दर्शन ही है और ज्ञान के निराधारपने होने से शून्यता की आपत्ति आती है; क्योंकि दर्शन को आत्मा का आधार मिल गया; परन्तु ज्ञान को आधार नहीं मिला; इसलिये आत्मा से रहित ज्ञान असत्तारूप है इसप्रकार विरोध आता है । अथवा आत्मा से ज्ञान निकलकर जिस-जिस द्रव्य को जानने जायेगा, वह द्रव्य भी चेतन हो जायेगा इसप्रकार तीन लोक में किसी भी अचेतन पदार्थ के नहीं रहने रूप महादोष प्राप्त होगा ।
ऊपर कहे गये दोष के भय से हे शिष्य! ज्ञान केवल परप्रकाशक नहीं है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो दर्शन भी केवल आत्मगत (स्वप्रकाशक) नहीं है - इसके साथ ऐसा भी सिद्ध हो गया; क्योंकि दर्शन स्वप्रकाशक ही हो तो पर को नहीं देखने से वह अंधा हो जायेगा और ज्ञान अकेला पर को जाने तो सभी पदार्थ चेतन हो जावेंगे और आत्मा ज्ञान बिना अचेतन हो जायेगा; अतः वास्तव में सिद्धान्त के साररूप इसका यह समाधान है कि ज्ञान और दर्शन के कथंचित् स्वपरप्रकाशकपना ही है ।
98
गाथा १६२ : शुद्धोपयोगाधिकार
१९५
शुद्धपयोग अधिकार की पहली गाथा में कहा था कि ज्ञान और दर्शन के कथंचित् स्वपरप्रकाशकपना है - वही बात यहाँ सिद्ध की गयी है। "
इस गाथा और उसकी टीका में ज्ञान, दर्शन और आत्मा ह्न तीनों को अनेक तर्क और युक्तियों से स्वपरप्रकाशक ही सिद्ध किया गया है ।। १६२।।
इसके बाद टीकाकार मुनिराज 'तथा श्री महासेन पण्डितदेव के द्वारा भी कहा गया है' ह्र ऐसा लिखकर एक छन्द प्रस्तुत करते हैं; जो इसप्रकार है ह्र
ज्ञानाद्भिन्नो न नाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथंचन । ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः । । ७८ ।। ( कुण्डलिया )
अरे ज्ञान से आत्मा, नहीं सर्वथा भिन्न अभिन्न भी है नहीं, यह है भिन्नाभिन्न ॥
यह है भिन्नाभिन्न कथंचित् नहीं सर्वथा । अरे कथंचित् भिन्न अभिन्न भी किसी अपेक्षा || जैनधर्म में नहीं सर्वथा कुछ भी होता । पूर्वापर जो ज्ञान आत्मा वह ही होता ॥ ७८ ॥ आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है; कथंचित् भिन्नाभिन्न है; क्योंकि पूर्वापर ज्ञान ही आत्मा है ह्न ऐसा कहा है।
इस छन्द के भाव को आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
"आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, कथंचित् भिन्न- अभिन्न है । यदि सर्वथा भिन्न माना जाये तो आत्मा के अचेतनपना प्राप्त होगा और ज्ञान को आत्मा से सर्वथा अभिन्न माना जाये तो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की भिन्नता नहीं रहती;
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १३८२-१३८३
२. महासेन पण्डितदेव, ग्रंथ नाम और श्लोक संख्या अनुपलब्ध है।