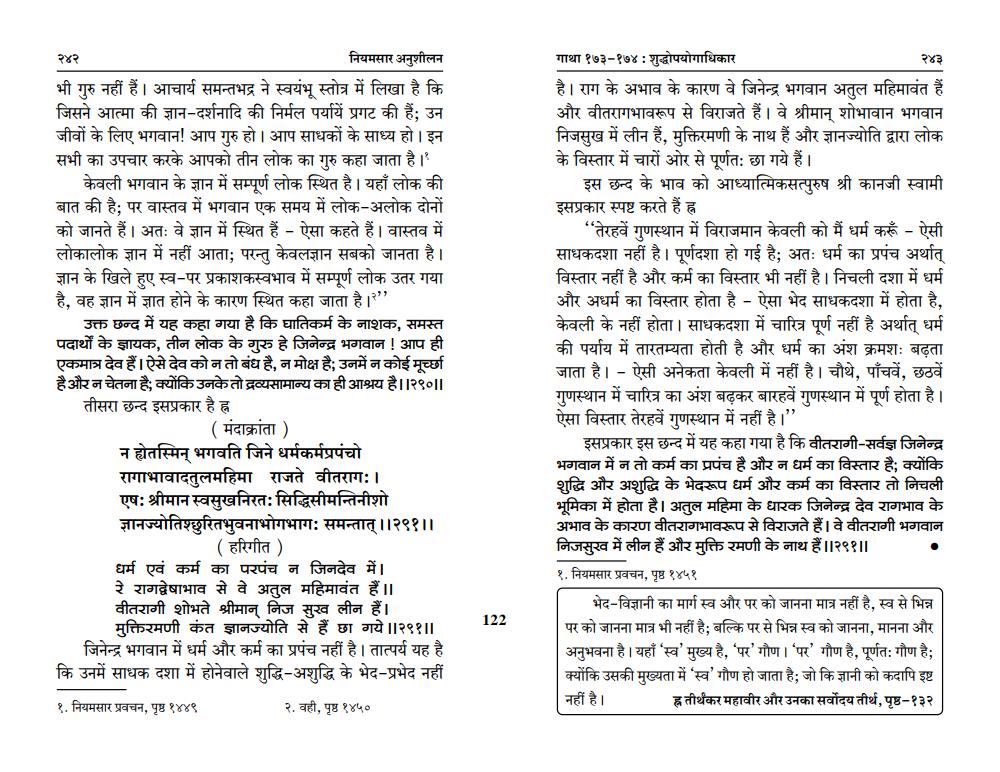________________
नियमसार अनुशीलन
२४२
भी गुरु नहीं हैं। आचार्य समन्तभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है कि जिसने आत्मा की ज्ञान दर्शनादि की निर्मल पर्यायें प्रगट की हैं; उन जीवों के लिए भगवान! आप गुरु हो। आप साधकों के साध्य हो। इन सभी का उपचार करके आपको तीन लोक का गुरु कहा जाता है। "
केवली भगवान के ज्ञान में सम्पूर्ण लोक स्थित है। यहाँ लोक की बात की है; पर वास्तव में भगवान एक समय में लोक- अलोक दोनों को जानते हैं। अतः वे ज्ञान में स्थित हैं- ऐसा कहते हैं। वास्तव में लोकालोक ज्ञान में नहीं आता; परन्तु केवलज्ञान सबको जानता है। ज्ञान के खिले हुए स्व-पर प्रकाशकस्वभाव में सम्पूर्ण लोक उतर गया है, वह ज्ञान में ज्ञात होने के कारण स्थित कहा जाता है। २"
उक्त छन्द में यह कहा गया है कि घातिकर्म के नाशक, समस्त पदार्थों के ज्ञायक, तीन लोक के गुरु हे जिनेन्द्र भगवान ! आप ही एकमात्र देव हैं। ऐसे देव को न तो बंध है, न मोक्ष है; उनमें न कोई मूर्च्छा है और न चेतना है; क्योंकि उनके तो द्रव्यसामान्य का ही आश्रय है ।। २९०॥ तीसरा छन्द इसप्रकार है ह्र
( मंदाक्रांता )
न ह्येतस्मिन् भगवति जिने धर्मकर्मप्रपंचो रागाभावादतुलमहिमा राजते वीतरागः । एषः श्रीमान स्वसुखनिरतः सिद्धिसीमन्तिनीशो ज्ञानज्योतिश्छुरितभुवनाभोगभागः समन्तात् ।। २९१ । । ( हरिगीत )
धर्म एवं कर्म का परपंच न जिनदेव में । रे रागद्वेषाभाव से वे अतुल महिमावंत हैं । वीतरागी शोभते श्रीमान् निज सुख लीन हैं। मुक्तिरमणी कंत ज्ञानज्योति से हैं छा गये ।। २९१ || जिनेन्द्र भगवान में धर्म और कर्म का प्रपंच नहीं है। तात्पर्य यह है कि उनमें साधक दशा में होनेवाले शुद्धि - अशुद्धि के भेद - प्रभेद नहीं
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १४४९
२. वही, पृष्ठ १४५०
122
गाथा १७३ - १७४ : शुद्धोपयोगाधिकार
है। राग के अभाव के कारण वे जिनेन्द्र भगवान अतुल महिमावंत हैं। और वीतरागभावरूप से विराजते हैं। वे श्रीमान् शोभावान भगवान निजसुख में लीन हैं, मुक्तिरमणी के नाथ हैं और ज्ञानज्योति द्वारा लोक के विस्तार में चारों ओर से पूर्णत: छा गये हैं ।
२४३
इस छन्द के भाव को आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
" तेरहवें गुणस्थान में विराजमान केवली को मैं धर्म करूँ - ऐसी साधकदशा नहीं है। पूर्णदशा हो गई है; अतः धर्म का प्रपंच अर्थात् विस्तार नहीं है और कर्म का विस्तार भी नहीं है। निचली दशा में धर्म और अधर्म का विस्तार होता है ऐसा भेद साधकदशा में होता है, केवली के नहीं होता । साधकदशा में चारित्र पूर्ण नहीं है अर्थात् धर्म की पर्याय में तारतम्यता होती है और धर्म का अंश क्रमशः बढ़ता जाता है। - ऐसी अनेकता केवली में नहीं है। चौथे, पाँचवें, छठवें गुणस्थान में चारित्र का अंश बढ़कर बारहवें गुणस्थान में पूर्ण होता है। ऐसा विस्तार तेरहवें गुणस्थान में नहीं है । "
इसप्रकार इस छन्द में यह कहा गया है कि वीतरागी - सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान में न तो कर्म का प्रपंच है और न धर्म का विस्तार है; क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि के भेदरूप धर्म और कर्म का विस्तार तो निचली भूमिका में होता है। अतुल महिमा के धारक जिनेन्द्र देव रागभाव अभाव के कारण वीतरागभावरूप से विराजते हैं। वे वीतरागी भगवान निजसुख में लीन हैं और मुक्ति रमणी के नाथ हैं ।।२९१ ॥
·
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १४५१
भेद - विज्ञानी का मार्ग स्व और पर को जानना मात्र नहीं है, स्व से भिन्न पर को जानना मात्र भी नहीं है; बल्कि पर से भिन्न स्व को जानना, मानना और अनुभवना है। यहाँ 'स्व' मुख्य है, 'पर' गौण 'पर' गौण है, पूर्णत: गौण है; क्योंकि उसकी मुख्यता में 'स्व' गौण हो जाता है; जो कि ज्ञानी को कदापि इष्ट नहीं है। ह्न तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ- १३२