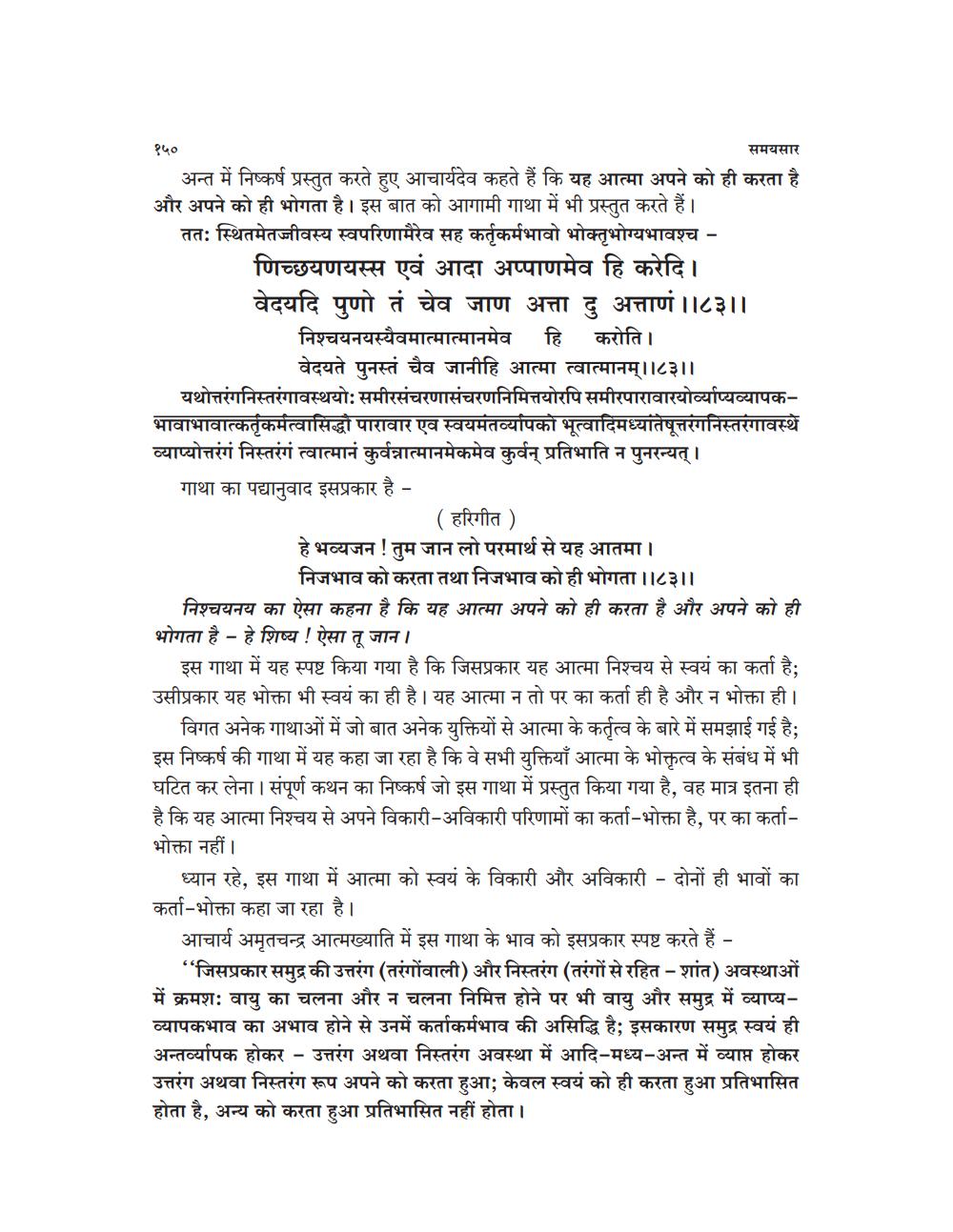________________
समयसार
१५० ___अन्त में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। इस बात को आगामी गाथा में भी प्रस्तुत करते हैं। तत: स्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च -
णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि। वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ।।८३।।
निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति।
वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम्।।८३।। यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयो: समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमतव्यापको भूत्वादिमध्यातेषूत्तरंगनिस्तरगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् ।
गाथा का पद्यानुवाद इसप्रकार है -
___ (हरिगीत )
हे भव्यजन ! तुम जान लो परमार्थ से यह आतमा।
निजभाव को करता तथा निजभाव कोही भोगता ।।८।। निश्चयनय का ऐसा कहना है कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है - हे शिष्य ! ऐसा तू जान ।
इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जिसप्रकार यह आत्मा निश्चय से स्वयं का कर्ता है; उसीप्रकार यह भोक्ता भी स्वयं का ही है। यह आत्मा न तो पर का कर्ता ही है और न भोक्ता ही।
विगत अनेक गाथाओं में जो बात अनेक युक्तियों से आत्मा के कर्तृत्व के बारे में समझाई गई है; इस निष्कर्ष की गाथा में यह कहा जा रहा है कि वे सभी युक्तियाँ आत्मा के भोक्तृत्व के संबंध में भी घटित कर लेना । संपूर्ण कथन का निष्कर्ष जो इस गाथा में प्रस्तुत किया गया है, वह मात्र इतना ही है कि यह आत्मा निश्चय से अपने विकारी-अविकारी परिणामों का कर्ता-भोक्ता है, पर का कर्ताभोक्ता नहीं।
ध्यान रहे, इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी और अविकारी - दोनों ही भावों का कर्ता-भोक्ता कहा जा रहा है।
आचार्य अमृतचन्द्र आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -
"जिसप्रकार समुद्र की उत्तरंग (तरंगोंवाली) और निस्तरंग (तरंगों से रहित - शांत) अवस्थाओं में क्रमश: वायु का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होने से उनमें कर्ताकर्मभाव की असिद्धि है; इसकारण समुद्र स्वयं ही अन्तर्व्यापक होकर - उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में आदि-मध्य-अन्त में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ; केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता।