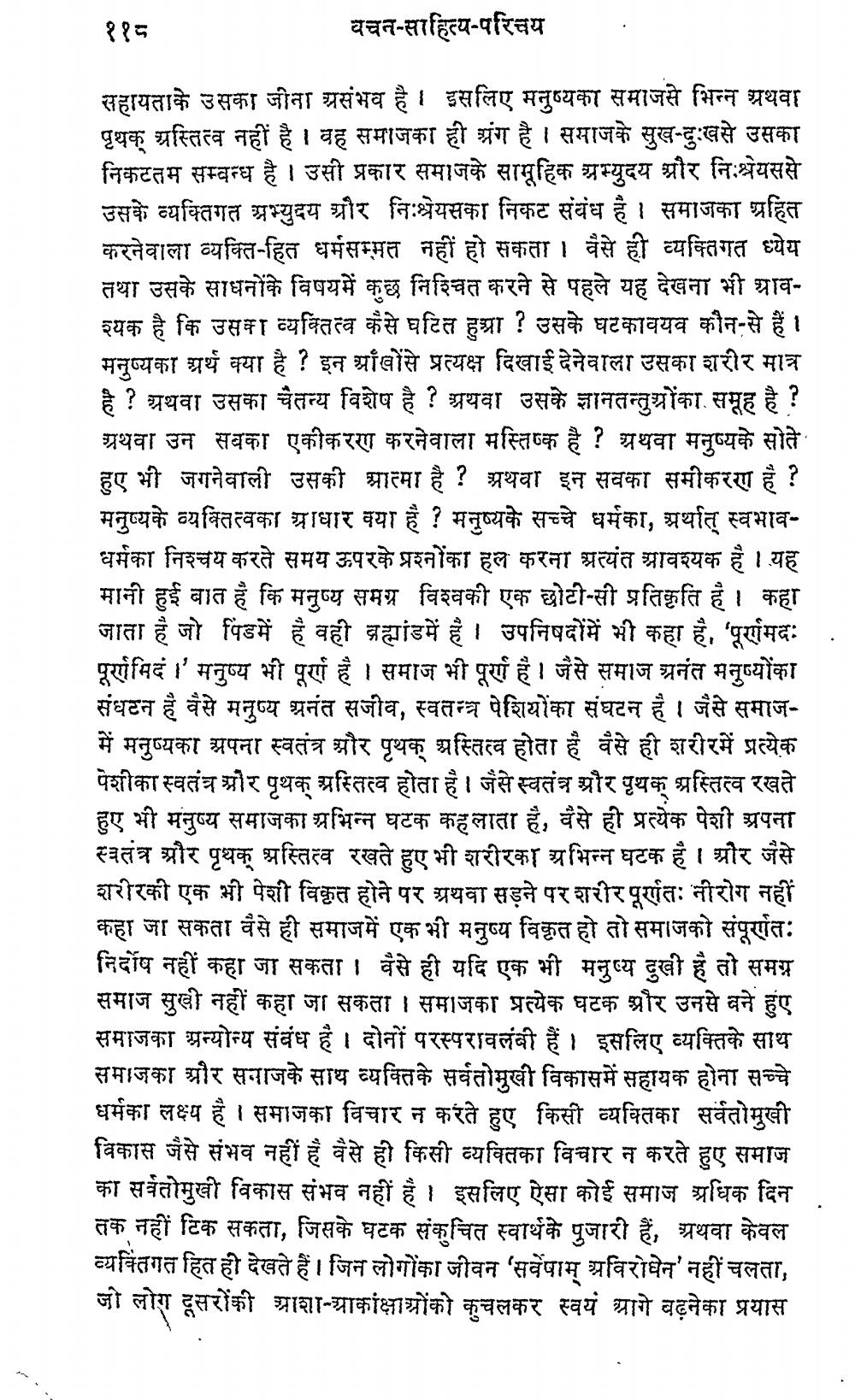________________
११८
वचन-साहित्य-परिचय
सहायताके उसका जीना असंभव है। इसलिए मनुष्यका समाजसे भिन्न अथवा पृथक् अस्तित्व नहीं है । वह समाजका ही अंग है । समाजके सुख-दुःखसे उसका निकटतम सम्बन्ध है । उसी प्रकार समाजके सामूहिक अभ्युदय और निःश्रेयससे उसके व्यक्तिगत अभ्युदय और निःश्रेयसका निकट संबंध है । समाजका अहित करनेवाला व्यक्ति-हित धर्मसम्मत नहीं हो सकता। वैसे ही व्यक्तिगत ध्येय तथा उसके साधनोंके विषयमें कुछ निश्चित करने से पहले यह देखना भी प्रावश्यक है कि उसका व्यक्तित्व कैसे घटित हुआ ? उसके घटकावयव कौन-से हैं । मनुष्यका अर्थ क्या है ? इन आँखोंसे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला उसका शरीर मात्र है ? अथवा उसका चैतन्य विशेष है ? अथवा उसके ज्ञानतन्तुनोंका समूह है ? अथवा उन सबका एकीकरण करनेवाला मस्तिष्क है ? अथवा मनुष्यके सोते हुए भी जगनेवाली उसकी आत्मा है ? अथवा इन सबका समीकरण है ? मनुष्यके व्यक्तित्वका आधार क्या है ? मनुष्यके सच्चे धर्मका, अर्थात् स्वभावधर्मका निश्चय करते समय ऊपरके प्रश्नोंका हल करना अत्यंत आवश्यक है । यह मानी हुई बात है कि मनुष्य समग्र विश्वकी एक छोटी-सी प्रतिकृति है। कहा जाता है जो पिंडमें है वही ब्रह्मांडमें है। उपनिषदोंमें भी कहा है, 'पूर्णमदः पूर्णमिदं ।' मनुष्य भी पूर्ण है । समाज भी पूर्ण है। जैसे समाज अनंत मनुष्योंका संघटन है वैसे मनुष्य अनंत सजीव, स्वतन्त्र पेशियोंका संघटन है। जैसे समाजमें मनुष्यका अपना स्वतंत्र और पृथक् अस्तित्व होता है वैसे ही शरीर में प्रत्येक पेशीका स्वतंत्र और पृथक् अस्तित्व होता है। जैसे स्वतंत्र और पृथक् अस्तित्व रखते हुए भी मनुष्य समाजका अभिन्न घटक कहलाता है, वैसे ही प्रत्येक पेशी अपना स्वतंत्र और पृथक् अस्तित्व रखते हुए भी शरीरका अभिन्न घटक है । और जैसे शरीरकी एक भी पेशी विकृत होने पर अथवा सड़ने पर शरीर पूर्णतः नीरोग नहीं कहा जा सकता वैसे ही समाज में एक भी मनुष्य विकृत हो तो समाजको संपूर्णतः निर्दोष नहीं कहा जा सकता। वैसे ही यदि एक भी मनुष्य दुखी है तो समग्न समाज सुखी नहीं कहा जा सकता । समाजका प्रत्येक घटक और उनसे बने हुए समाजका अन्योन्य संबंध है। दोनों परस्परावलंबी हैं। इसलिए व्यक्तिके साथ समाजका और समाजके साथ व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकासमें सहायक होना सच्चे धर्मका लक्ष्य है । समाजका विचार न करते हुए किसी व्यक्तिका सर्वतोमुखी विकास जैसे संभव नहीं है वैसे ही किसी व्यक्तिका विचार न करते हुए समाज का सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कोई समाज अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, जिसके घटक संकुचित स्वार्थ के पुजारी हैं, अथवा केवल व्यक्तिगत हित ही देखते हैं। जिन लोगोंका जीवन 'सर्वेषाम् अविरोधेन' नहीं चलता, जो लोग दूसरोंकी आशा-आकांक्षाओंको कुचलकर स्वयं आगे बढ़नेका प्रयास