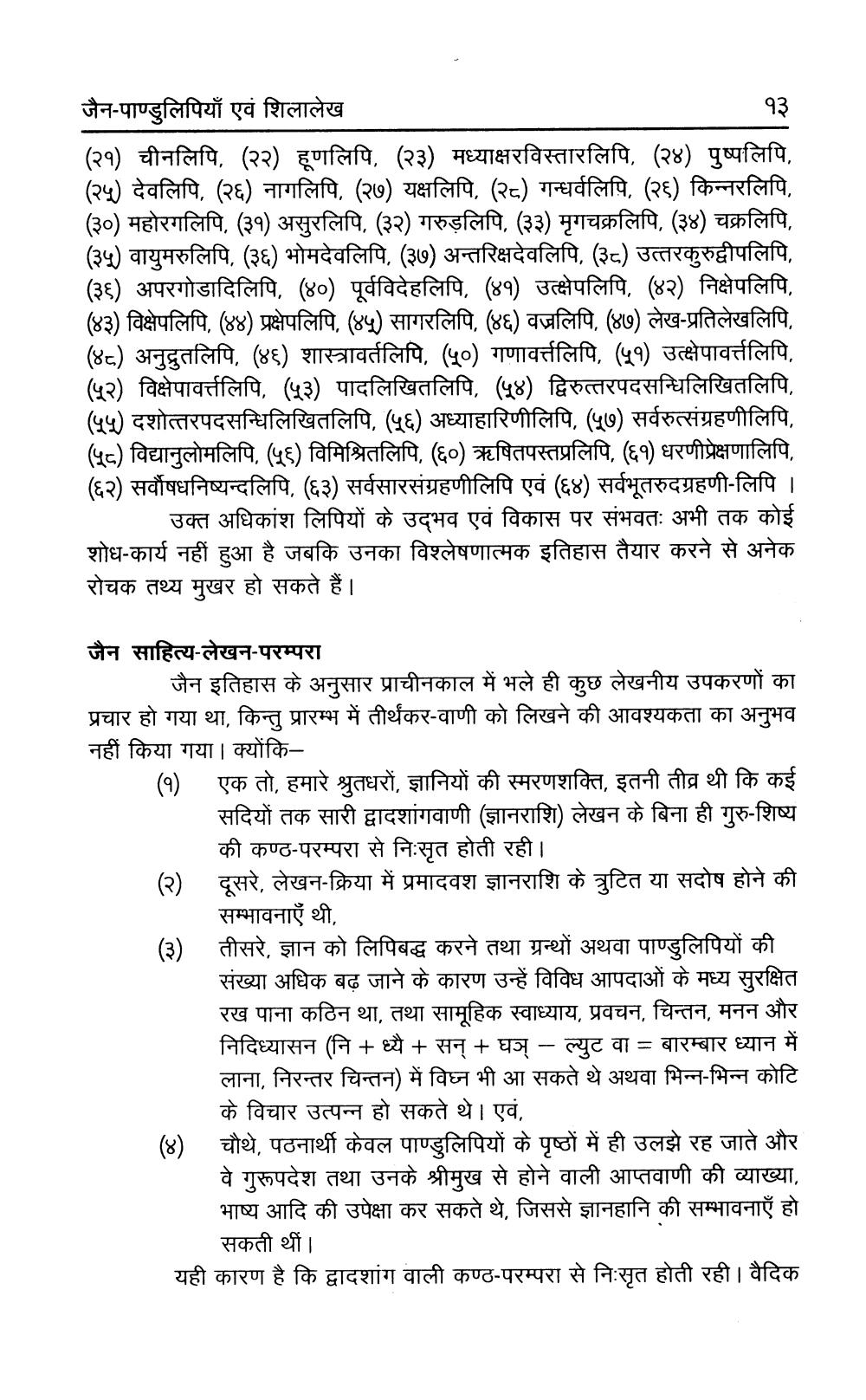________________
जैन-पाण्डुलिपियाँ एवं शिलालेख (२१) चीनलिपि, (२२) हूणलिपि, (२३) मध्याक्षरविस्तारलिपि, (२४) पुष्पलिपि, (२५) देवलिपि, (२६) नागलिपि, (२७) यक्षलिपि, (२८) गन्धर्वलिपि, (२६) किन्नरलिपि, (३०) महोरगलिपि, (३१) असुरलिपि, (३२) गरुड़लिपि, (३३) मृगचक्रलिपि, (३४) चक्रलिपि, (३५) वायुमरुलिपि, (३६) भोमदेवलिपि, (३७) अन्तरिक्षदेवलिपि, (३८) उत्तरकुरुद्वीपलिपि, (३६) अपरगोडादिलिपि, (४०) पूर्वविदेहलिपि, (४१) उत्क्षेपलिपि, (४२) निक्षेपलिपि, (४३) विक्षेपलिपि, (४४) प्रक्षेपलिपि, (४५) सागरलिपि, (४६) वज्रलिपि, (४७) लेख-प्रतिलेखलिपि, (४८) अनुद्रुतलिपि, (४६) शास्त्रावर्तलिपि, (५०) गणावर्तलिपि, (५१) उत्क्षेपावर्त्तलिपि, (५२) विक्षेपावर्त्तलिपि, (५३) पादलिखितलिपि, (५४) द्विरुत्तरपदसन्धिलिखितलिपि, (५५) दशोत्तरपदसन्धिलिखितलिपि, (५६) अध्याहारिणीलिपि, (५७) सर्वरुत्संग्रहणीलिपि, (५८) विद्यानुलोमलिपि, (५६) विमिश्रितलिपि, (६०) ऋषितपस्तप्रलिपि, (६१) धरणीप्रेक्षणालिपि, (६२) सर्वौषधनिष्यन्दलिपि, (६३) सर्वसारसंग्रहणीलिपि एवं (६४) सर्वभूतरुदग्रहणी-लिपि ।
उक्त अधिकांश लिपियों के उद्भव एवं विकास पर संभवतः अभी तक कोई शोध-कार्य नहीं हुआ है जबकि उनका विश्लेषणात्मक इतिहास तैयार करने से अनेक रोचक तथ्य मुखर हो सकते हैं।
जैन साहित्य-लेखन-परम्परा
जैन इतिहास के अनुसार प्राचीनकाल में भले ही कुछ लेखनीय उपकरणों का प्रचार हो गया था, किन्तु प्रारम्भ में तीर्थंकर-वाणी को लिखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया। क्योंकि(१) एक तो, हमारे श्रुतधरों, ज्ञानियों की स्मरणशक्ति, इतनी तीव्र थी कि कई
सदियों तक सारी द्वादशांगवाणी (ज्ञानराशि) लेखन के बिना ही गुरु-शिष्य की कण्ठ-परम्परा से निःसृत होती रही। दूसरे, लेखन-क्रिया में प्रमादवश ज्ञानराशि के त्रुटित या सदोष होने की सम्भावनाएँ थी, तीसरे, ज्ञान को लिपिबद्ध करने तथा ग्रन्थों अथवा पाण्डुलिपियों की संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण उन्हें विविध आपदाओं के मध्य सुरक्षित रख पाना कठिन था, तथा सामूहिक स्वाध्याय, प्रवचन, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन (नि + ध्यै + सन् + घञ् - ल्युट वा = बारम्बार ध्यान में लाना, निरन्तर चिन्तन) में विघ्न भी आ सकते थे अथवा भिन्न-भिन्न कोटि के विचार उत्पन्न हो सकते थे। एवं, चौथे, पठनार्थी केवल पाण्डुलिपियों के पृष्ठों में ही उलझे रह जाते और वे गुरूपदेश तथा उनके श्रीमुख से होने वाली आप्तवाणी की व्याख्या, भाष्य आदि की उपेक्षा कर सकते थे, जिससे ज्ञानहानि की सम्भावनाएँ हो
सकती थीं। यही कारण है कि द्वादशांग वाली कण्ठ-परम्परा से निःसृत होती रही। वैदिक