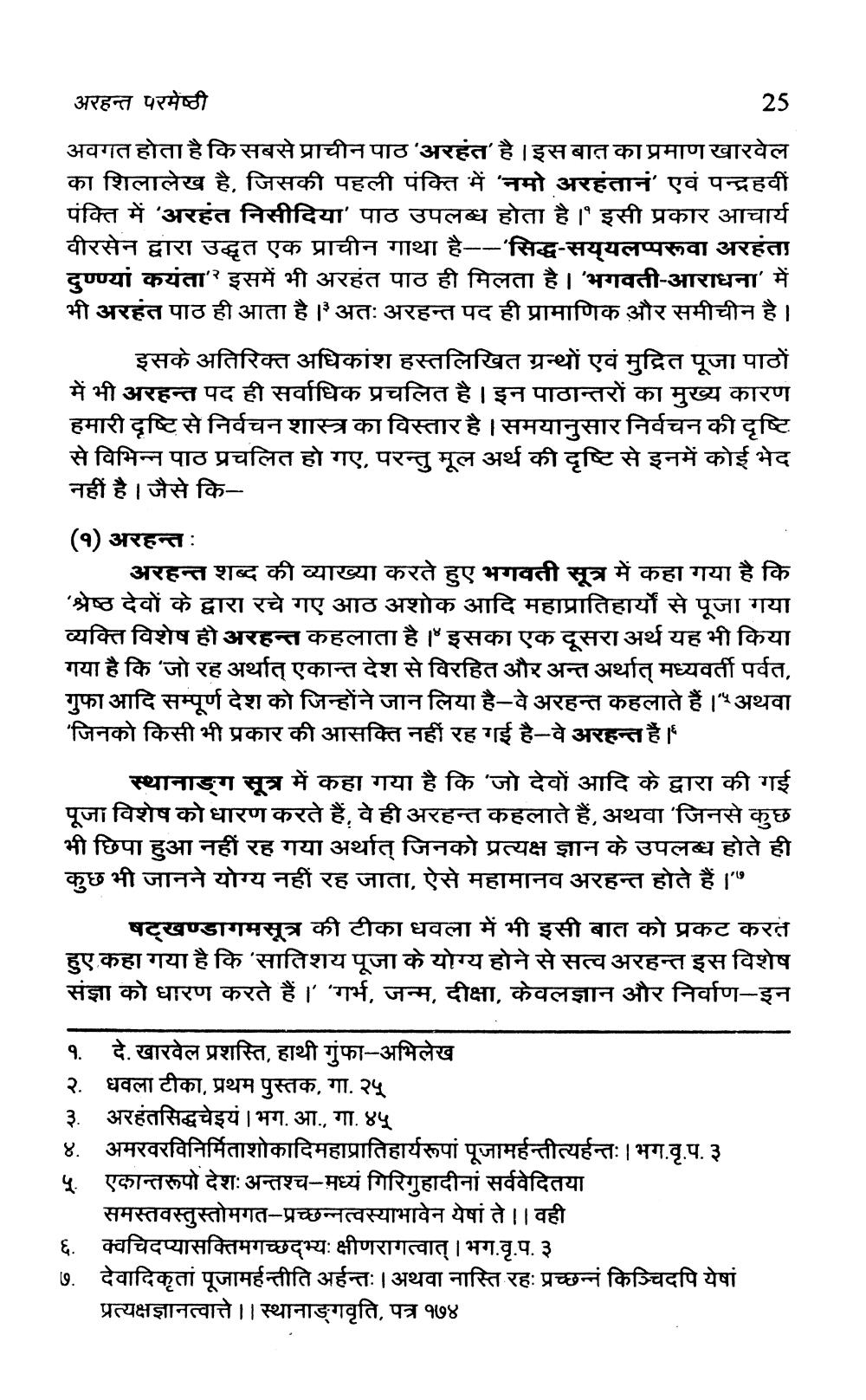________________ अरहन्त परमेष्ठी 25 अवगत होता है कि सबसे प्राचीन पाठ 'अरहंत' है। इस बात का प्रमाण खारवेल का शिलालेख है, जिसकी पहली पंक्ति में 'नमो अरहतानं' एवं पन्द्रहवीं पंक्ति में 'अरहंत निसीदिया' पाठ उपलब्ध होता है। इसी प्रकार आचार्य वीरसेन द्वारा उद्धृत एक प्राचीन गाथा है--'सिद्ध-सय्यलप्परूवा अरहंता दुण्ण्यां कयंता इसमें भी अरहंत पाठ ही मिलता है। 'भगवती-आराधना' में भी अरहंत पाठ ही आता है। अतः अरहन्त पद ही प्रामाणिक और समीचीन है। - इसके अतिरिक्त अधिकांश हस्तलिखित ग्रन्थों एवं मुद्रित पूजा पाठों में भी अरहन्त पद ही सर्वाधिक प्रचलित है। इन पाठान्तरों का मुख्य कारण हमारी दृष्टि से निर्वचन शास्त्र का विस्तार है। समयानुसार निर्वचन की दृष्टि से विभिन्न पाठ प्रचलित हो गए, परन्तु मूल अर्थ की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे कि(१) अरहन्तः अरहन्त शब्द की व्याख्या करते हुए भगवती सूत्र में कहा गया है कि 'श्रेष्ठ देवों के द्वारा रचे गए आठ अशोक आदि महाप्रातिहार्यों से पूजा गया व्यक्ति विशेष हो अरहन्त कहलाता है। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि 'जो रह अर्थात् एकान्त देश से विरहित और अन्त अर्थात् मध्यवर्ती पर्वत, गुफा आदि सम्पूर्ण देश को जिन्होंने जान लिया है-वे अरहन्त कहलाते हैं / अथवा "जिनको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह गई है-वे अरहन्त हैं। स्थानाङ्ग सूत्र में कहा गया है कि 'जो देवों आदि के द्वारा की गई पूजा विशेष को धारण करते हैं, वे ही अरहन्त कहलाते हैं, अथवा 'जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह गया अर्थात् जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान के उपलब्ध होते ही कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता, ऐसे महामानव अरहन्त होते हैं।" षट्खण्डागमसूत्र की टीका धवला में भी इसी बात को प्रकट करत हुए कहा गया है कि 'सातिशय पूजा के योग्य होने से सत्व अरहन्त इस विशेष संज्ञा को धारण करते हैं।' 'गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण-इन 1. दे. खारवेल प्रशस्ति, हाथी गुंफा-अभिलेख 2. धवला टीका, प्रथम पुस्तक, गा. 25 3. अरहंतसिद्धचेइयं / भग. आ., गा. 45 4. अमरवरविनिर्मिताशोकादिमहाप्रातिहार्यरूपां पूजामहन्तीत्यर्हन्तः / भग.वृ.प.३ 5. एकान्तरूपो देशः अन्तश्च-मध्यं गिरिगुहादीनां सर्ववेदितया समस्तवस्तुस्तोमगत-प्रच्छन्नत्वस्याभावेन येषां ते।। वही 6. क्वचिदप्यासक्तिमगच्छद्भ्यः क्षीणरागत्वात् / भग.वृ.प.३ 7. देवादिकृतां पूजामर्हन्तीति अर्हन्तः / अथवा नास्ति रहः प्रच्छन्नं किञ्चिदपि येषां प्रत्यक्षज्ञानत्वात्ते / / स्थानाङ्गवृति, पत्र 174