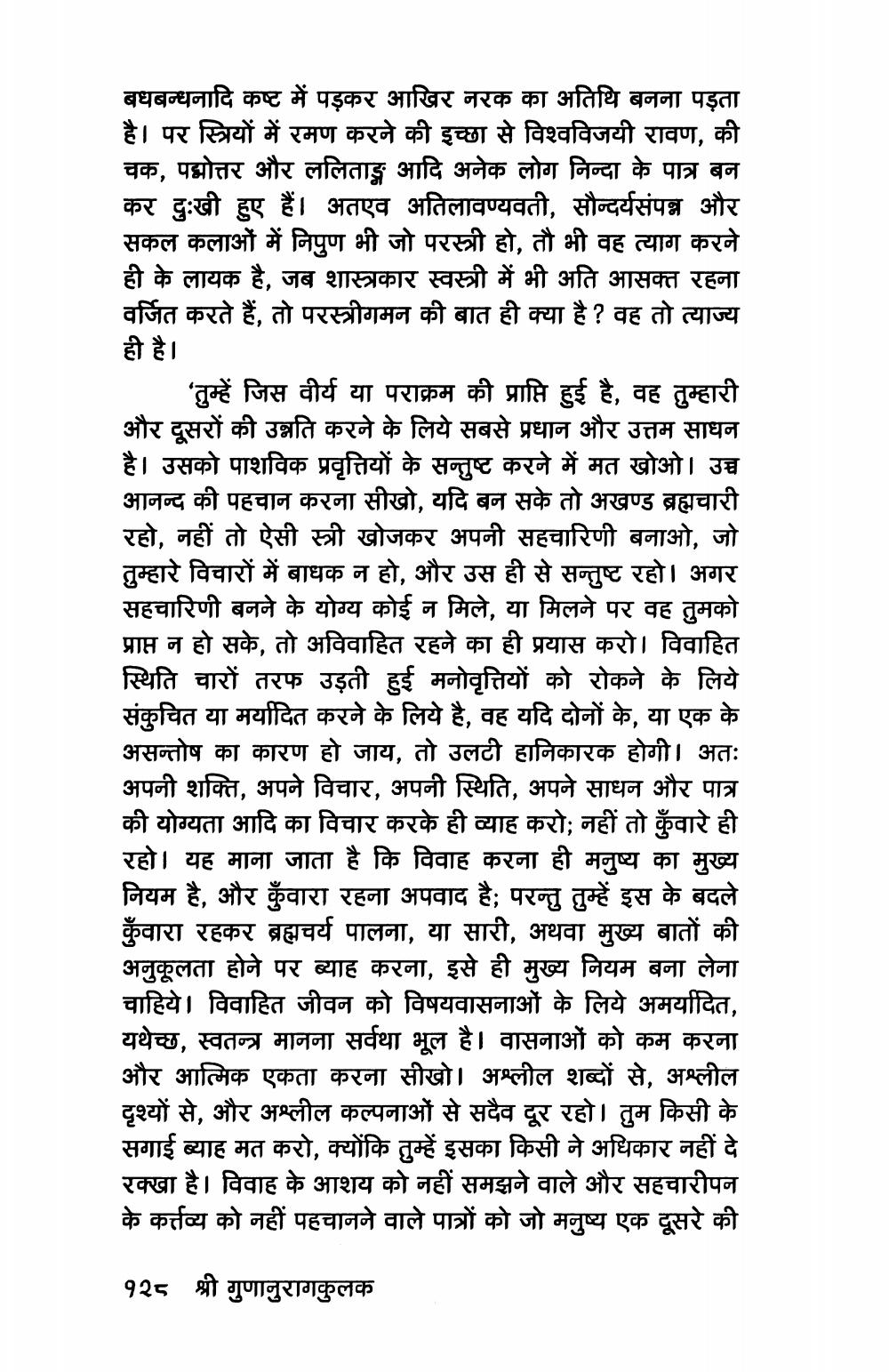________________
बधबन्धनादि कष्ट में पड़कर आखिर नरक का अतिथि बनना पड़ता है। पर स्त्रियों में रमण करने की इच्छा से विश्वविजयी रावण, की चक, पद्मोत्तर और ललिताङ्ग आदि अनेक लोग निन्दा के पात्र बन कर दुःखी हुए हैं। अतएव अतिलावण्यवती, सौन्दर्यसंपन्न और सकल कलाओं में निपुण भी जो परस्त्री हो, तो भी वह त्याग करने ही के लायक है, जब शास्त्रकार स्वस्त्री में भी अति आसक्त रहना वर्जित करते हैं, तो परस्त्रीगमन की बात ही क्या है ? वह तो त्याज्य ही है।
'तम्हें जिस वीर्य या पराक्रम की प्राप्ति हुई है, वह तुम्हारी और दूसरों की उन्नति करने के लिये सबसे प्रधान और उत्तम साधन है। उसको पाशविक प्रवृत्तियों के सन्तुष्ट करने में मत खोओ। उच्च आनन्द की पहचान करना सीखो, यदि बन सके तो अखण्ड ब्रह्मचारी रहो, नहीं तो ऐसी स्त्री खोजकर अपनी सहचारिणी बनाओ, जो तुम्हारे विचारों में बाधक न हो, और उस ही से सन्तुष्ट रहो। अगर सहचारिणी बनने के योग्य कोई न मिले, या मिलने पर वह तुमको प्राप्त न हो सके, तो अविवाहित रहने का ही प्रयास करो। विवाहित स्थिति चारों तरफ उड़ती हुई मनोवृत्तियों को रोकने के लिये संकुचित या मर्यादित करने के लिये है, वह यदि दोनों के, या एक के असन्तोष का कारण हो जाय, तो उलटी हानिकारक होगी। अतः अपनी शक्ति, अपने विचार, अपनी स्थिति, अपने साधन और पात्र की योग्यता आदि का विचार करके ही व्याह करो; नहीं तो कुँवारे ही रहो। यह माना जाता है कि विवाह करना ही मनुष्य का मुख्य नियम है, और कुँवारा रहना अपवाद है; परन्तु तुम्हें इस के बदले कुँवारा रहकर ब्रह्मचर्य पालना, या सारी, अथवा मुख्य बातों की अनुकूलता होने पर ब्याह करना, इसे ही मुख्य नियम बना लेना चाहिये। विवाहित जीवन को विषयवासनाओं के लिये अमर्यादित, यथेच्छ, स्वतन्त्र मानना सर्वथा भूल है। वासनाओं को कम करना और आत्मिक एकता करना सीखो। अश्लील शब्दों से, अश्लील दृश्यों से, और अश्लील कल्पनाओं से सदैव दूर रहो। तुम किसी के सगाई ब्याह मत करो, क्योंकि तुम्हें इसका किसी ने अधिकार नहीं दे रक्खा है। विवाह के आशय को नहीं समझने वाले और सहचारीपन के कर्तव्य को नहीं पहचानने वाले पात्रों को जो मनुष्य एक दूसरे की
१२८ श्री गुणानुरागकुलक