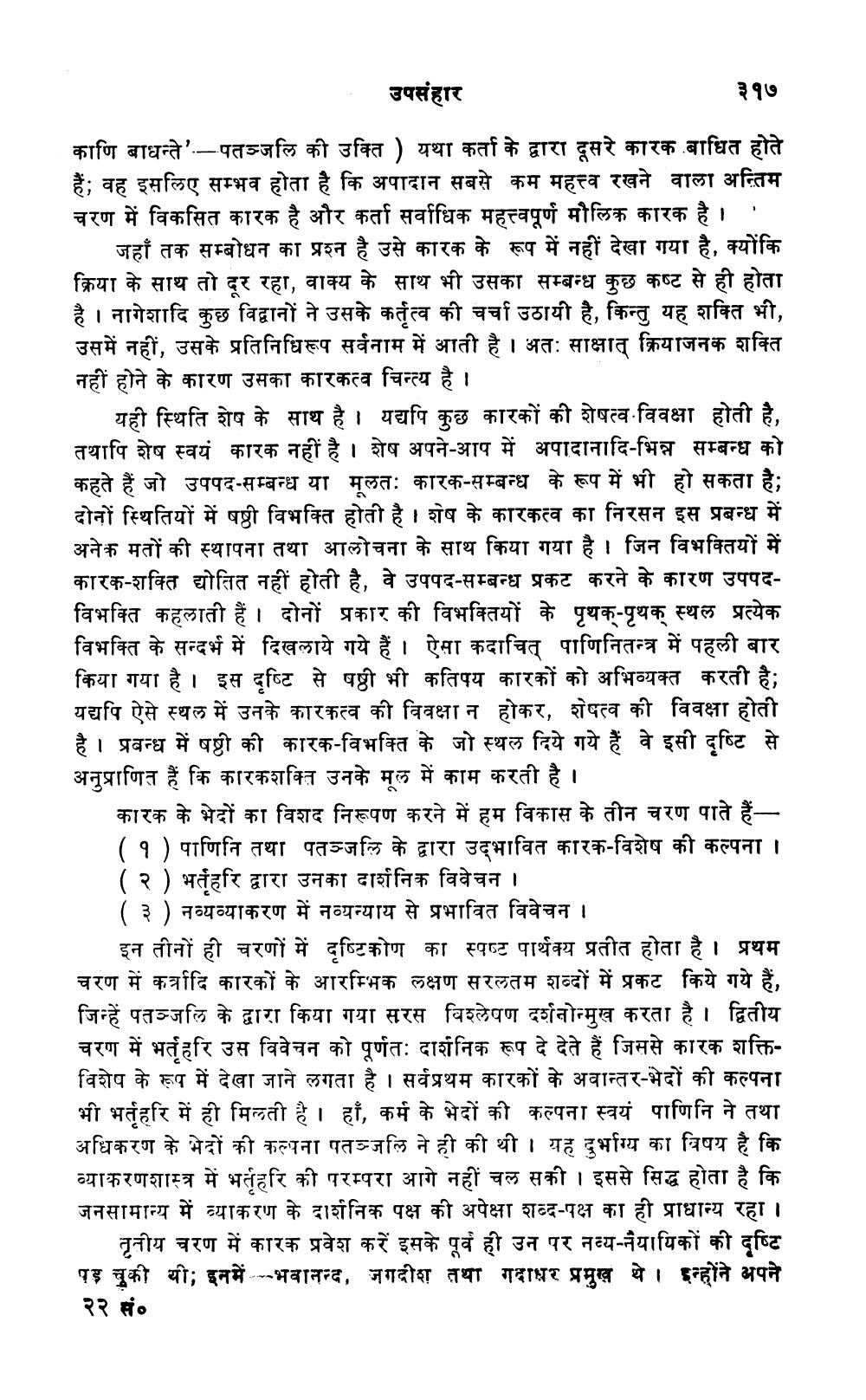________________
उपसंहार
३१७ काणि बाधन्ते'.-पतञ्जलि की उक्ति ) यथा कर्ता के द्वारा दूसरे कारक बाधित होते हैं; वह इसलिए सम्भव होता है कि अपादान सबसे कम महत्त्व रखने वाला अन्तिम चरण में विकसित कारक है और कर्ता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मौलिक कारक है। ' ___ जहाँ तक सम्बोधन का प्रश्न है उसे कारक के रूप में नहीं देखा गया है, क्योंकि क्रिया के साथ तो दूर रहा, वाक्य के साथ भी उसका सम्बन्ध कुछ कष्ट से ही होता है । नागेशादि कुछ विद्वानों ने उसके कर्तृत्व की चर्चा उठायी है, किन्तु यह शक्ति भी, उसमें नहीं, उसके प्रतिनिधिरूप सर्वनाम में आती है । अतः साक्षात् क्रियाजनक शक्ति नहीं होने के कारण उसका कारकत्व चिन्त्य है।
यही स्थिति शेष के साथ है। यद्यपि कुछ कारकों की शेषत्व विवक्षा होती है, तथापि शेष स्वयं कारक नहीं है । शेष अपने-आप में अपादानादि-भिन्न सम्बन्ध को कहते हैं जो उपपद-सम्बन्ध या मलतः कारक-सम्बन्ध के रूप में भी हो सकता है; दोनों स्थितियों में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष के कारकत्व का निरसन इस प्रबन्ध में अनेक मतों की स्थापना तथा आलोचना के साथ किया गया है । जिन विभक्तियों में कारक-शक्ति द्योतित नहीं होती है, वे उपपद-सम्बन्ध प्रकट करने के कारण उपपदविभक्ति कहलाती हैं। दोनों प्रकार की विभक्तियों के पृथक्-पृथक् स्थल प्रत्येक विभक्ति के सन्दर्भ में दिखलाये गये हैं। ऐसा कदाचित् पाणिनितन्त्र में पहली बार किया गया है। इस दृष्टि से षष्ठी भी कतिपय कारकों को अभिव्यक्त करती है; यद्यपि ऐसे स्थल में उनके कारकत्व की विवक्षा न होकर, शेषत्व की विवक्षा होती है। प्रबन्ध में षष्ठी की कारक-विभक्ति के जो स्थल दिये गये हैं वे इसी दृष्टि से अनुप्राणित हैं कि कारकशक्ति उनके मूल में काम करती है।
कारक के भेदों का विशद निरूपण करने में हम विकास के तीन चरण पाते हैं( १ ) पाणिनि तथा पतञ्जलि के द्वारा उद्भावित कारक-विशेष की कल्पना । ( २ ) भर्तहरि द्वारा उनका दार्शनिक विवेचन । ( ३ ) नव्यव्याकरण में नव्यन्याय से प्रभावित विवेचन ।
इन तीनों ही चरणों में दृष्टिकोण का स्पष्ट पार्थक्य प्रतीत होता है। प्रथम चरण में कादि कारकों के आरम्भिक लक्षण सरलतम शब्दों में प्रकट किये गये हैं, जिन्हें पतञ्जलि के द्वारा किया गया सरस विश्लेपण दर्शनोन्मुख करता है। द्वितीय चरण में भर्तृहरि उस विवेचन को पूर्णतः दार्शनिक रूप दे देते हैं जिससे कारक शक्तिविशेष के रूप में देखा जाने लगता है । सर्वप्रथम कारकों के अवान्तर-भेदों की कल्पना भी भर्तृहरि में ही मिलती है। हाँ, कर्म के भेदों की कल्पना स्वयं पाणिनि ने तथा अधिकरण के भेदों की कल्पना पतञ्जलि ने ही की थी। यह दुर्भाग्य का विषय है कि व्याकरणशास्त्र में भर्तृहरि की परम्परा आगे नहीं चल सकी। इससे सिद्ध होता है कि जनसामान्य में व्याकरण के दार्शनिक पक्ष की अपेक्षा शब्द-पक्ष का ही प्राधान्य रहा।
तृतीय चरण में कारक प्रवेश करें इसके पूर्व ही उन पर नव्य-नैयायिकों की दृष्टि पड़ चुकी थी; इनमें - भवानन्द, जगदीश तथा गदाधर प्रमुख थे। इन्होंने अपने २२ सं०