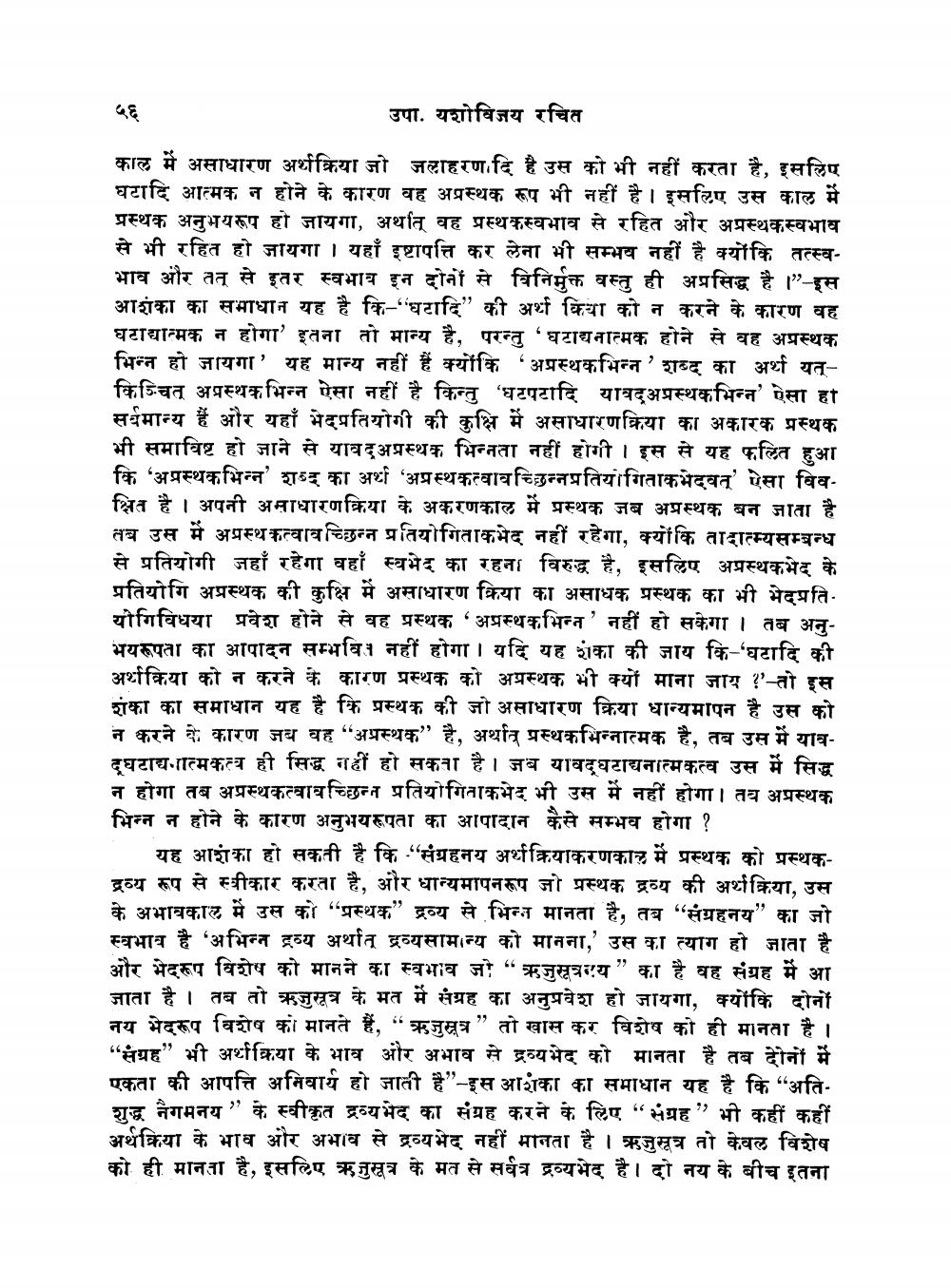________________
५६
उपा. यशोविजय रचित काल में असाधारण अर्थक्रिया जो जलाहरण दि है उस को भी नहीं करता है, इसलिए घटादि आत्मक न होने के कारण वह अप्रस्थक रूप भी नहीं है। इसलिए उस काल में प्रस्थक अनुभयरूप हो जायगा, अर्थात् वह प्रस्थकस्वभाव से रहित और अप्रस्थकस्वभाव से भी रहित हो जायगा । यहाँ इष्टापत्ति कर लेना भी सम्भव नहीं है क्योंकि तत्स्वभाव और तत् से इतर स्वभाव इन दोनों से विनिर्मुक्त वस्तु ही अप्रसिद्ध है ।" इस आशंका का समाधान यह है कि-"घटादि" की अर्थ किया को न करने के कारण वह घटाद्यात्मक न होगा' इतना तो मान्य है, परन्तु 'घटाद्यनात्मक होने से वह अप्रस्थक भिन्न हो जायगा' यह मान्य नहीं हैं क्योंकि 'अप्रस्थकभिन्न' शब्द का अर्थ यत्किञ्चित् अप्रस्थक भिन्न ऐसा नहीं है किन्तु 'धटपटादि यावदअप्रस्थकभिन्न' ऐसा हो सर्वमान्य हैं और यहाँ भेदप्रतियोगी की कुक्षि में असाधारण क्रिया का अकारक प्रस्थक भी समाविष्ट हो जाने से यावदअप्रस्थक भिन्नता नहीं होगी। इस से यह फलित हुआ कि 'अप्रस्थकभिन्न' शब्द का अर्थ 'अप्रस्थकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत' ऐसा विवक्षित है । अपनी असाधारण क्रिया के अकरणकाल में प्रस्थक जब अप्रस्थक बन जाता है तब उस में अप्रस्थकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद नहीं रहेगा, क्योंकि तादात्म्यसम्बन्ध से प्रतियोगी जहाँ रहेगा वहाँ स्वभेद का रहना विरुद्ध है, इसलिए अप्रस्थकभेद के प्रतियोगि अप्रस्थक की कुक्षि में असाधारण क्रिया का असाधक प्रस्थक का भी भेदप्रति. योगिविधया प्रवेश होने से वह प्रस्थक 'अप्रस्थकभिन्न' नहीं हो सकेगा। तब अनुभयरूपता का आपादन सम्भवित नहीं होगा। यदि यह शंका की जाय कि-'घटादि की अर्थकिया को न करने के कारण प्रस्थक को अप्रस्थक भी क्यों माना जाय ?' तो इस शंका का समाधान यह है कि प्रस्थक की जो असाधारण क्रिया धान्यमापन है उस को न करने के कारण जब वह "अप्रस्थक" है, अर्थात् प्रस्थकभिन्नात्मक है, तब उस में यावदघटाद्य-नात्मकत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता है। जब यावघटाद्यनात्मकत्व उस में सिद्ध न होगा तब अप्रस्थकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद भी उस में नहीं होगा। तब अप्रस्थक भिन्न न होने के कारण अनुभयरूपता का आपादान कैसे सम्भव होगा ?
यह आशंका हो सकती है कि "संग्रहनय अर्थक्रियाकरणकाल में प्रस्थक को प्रस्थकद्रव्य रूप से स्वीकार करता है, और धान्यमापनरूप जो प्रस्थक द्रव्य की अर्थक्रिया, उस के अभावकाल में उस को "प्रस्थक” द्रव्य से भिन्न मानता है, तब "संग्रहनय” का जो स्वभाव है 'अभिन्न द्रव्य अर्थात् द्रव्यसामान्य को मानना, उस का त्याग हो जाता है और भेदरूप विशेष को मानने का स्वभाव जो "ऋजसूत्ररय” का है वह संग्रह में आ जाता है। तब तो ऋजुसूत्र के मत में संग्रह का अनुप्रवेश हो जायगा, क्योंकि दोनों नय भेदरूप विशेष को मानते हैं, "ऋजुसूत्र” तो खास कर विशेष को ही मानता “संग्रह" भी अर्थक्रिया के भाव और अभाव से द्रव्यभेद को मानता है तब दोनों में एकता की आपत्ति अनिवार्य हो जाती है"-इस आशंका का समाधान यह है कि "अति. शद्ध नैगमनय" के स्वीकृत द्रव्यभेद का संग्रह करने के लिए "संग्रह" भी कहीं कहीं अर्थक्रिया के भाव और अभाव से द्रव्यभेद नहीं मानता है। ऋजसूत्र तो केवल विशेष को ही मानता है, इसलिए ऋजुसूत्र के मत से सर्वत्र द्रव्यभेद है। दो नय के बीच इतना