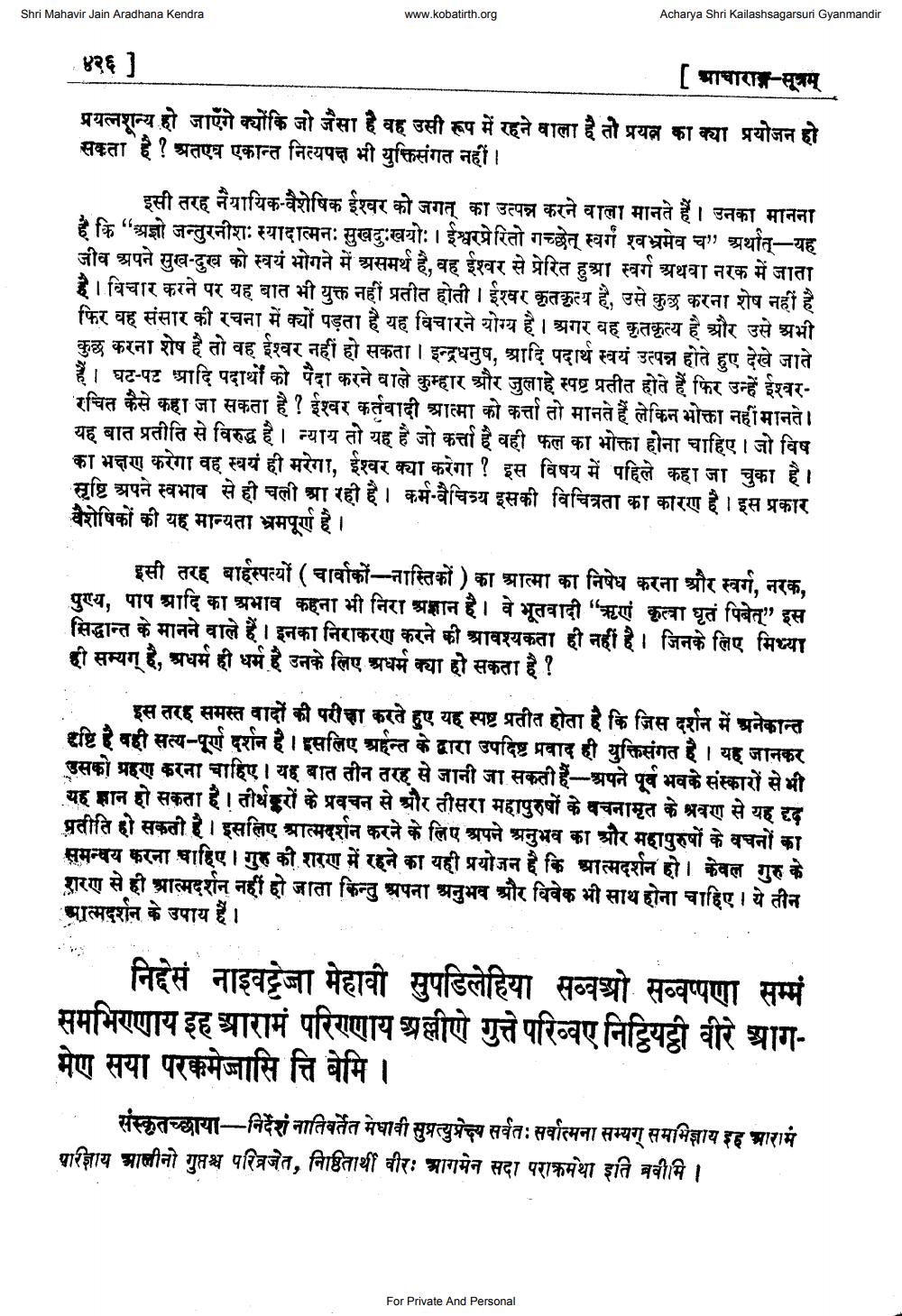________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
४२६ ]
[ आचाराङ्ग-सूत्रम्
प्रयत्नशून्य हो जाएंगे क्योंकि जो जैसा है वह उसी रूप में रहने वाला है तो प्रयत्न का क्या प्रयोजन हो सकता है ? as एकान्त नित्यपक्ष भी युक्तिसंगत नहीं ।
इसी तरह नैयायिक-वैशेषिक ईश्वर को जगत् का उत्पन्न करने वाला मानते हैं। उनका मानना है कि "अज्ञो जन्तुरनीशः स्यादात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं श्वभ्रमेव च" अर्थात् – यह जीव अपने सुख-दुख को स्वयं भोगने में असमर्थ है, वह ईश्वर से प्रेरित हुआ स्वर्ग अथवा नरक में जाता है । विचार करने पर यह बात भी युक्त नहीं प्रतीत होती । ईश्वर कृतकृत्य है, उसे कुछ करना शेष नहीं है। फिर वह संसार की रचना में क्यों पड़ता है यह विचारने योग्य है । अगर वह कृतकृत्य है और उसे अभी कुछ करना शेष है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता । इन्द्रधनुष, आदि पदार्थ स्वयं उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। घट-पट आदि पदार्थों को पैदा करने वाले कुम्हार और जुलाहे स्पष्ट प्रतीत होते हैं फिर उन्हें ईश्वर'रचित कैसे कहा जा सकता है ? ईश्वर कर्तवादी आत्मा को कर्त्ता तो मानते हैं लेकिन भोक्ता नहीं मानते । यह बात प्रतीति से विरुद्ध है । न्याय तो यह है जो कर्त्ता है वही फल का भोक्ता होना चाहिए। जो विष का भक्षण करेगा वह स्वयं ही मरेगा, ईश्वर क्या करेगा ? इस विषय में पहिले कहा जा चुका है । सृष्टि अपने स्वभाव से ही चली आ रही है। कर्म वैचित्र्य इसकी विचित्रता का कारण है। इस प्रकार वैशेषिकों की यह मान्यता भ्रमपूर्ण है ।
इसी तरह बार्हस्पत्यों (चार्वाकों - नास्तिकों ) का आत्मा का निषेध करना और स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप आदि का अभाव कहना भी निरा अज्ञान है। वे भूतवादी "ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्” इस सिद्धान्त के मानने वाले हैं। इनका निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनके लिए मिध्या ही सम्यग् है, अधर्म ही धर्म है उनके लिए अधर्म क्या हो सकता है ?
इस तरह समस्त वादों की परीक्षा करते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस दर्शन में अनेकान्त है वही सत्य-पूर्ण दर्शन है। इसलिए अर्हन्त के द्वारा उपदिष्ट प्रवाद ही युक्तिसंगत है । यह जानकर उसको ग्रहण करना चाहिए। यह बात तीन तरह से जानी जा सकती हैं - अपने पूर्व भवके संस्कारों से भी यह ज्ञान हो सकता है। तीर्थङ्कुरों के प्रवचन से और तीसरा महापुरुषों के वचनामृत के श्रवण से यह हद प्रतीति हो सकती है। इसलिए आत्मदर्शन करने के लिए अपने अनुभव का और महापुरुषों के वचनों का समन्वय करना चाहिए। गुरु की शरण में रहने का यही प्रयोजन है कि आत्मदर्शन हो । केवल गुरु के शरण से ही आत्मदर्शन नहीं हो जाता किन्तु अपना अनुभव और विवेक भी साथ होना चाहिए। ये तीन आत्मदर्शन के उपाय हैं।
निद्देसं नाइवट्टेज्जा मेहावी सुपडिलेहिया सव्वश्र सव्वप्पणा सम्म समभिण्णाय इह थारामं परिणाय अल्लीणे गुत्ते परिव्वए निट्टियट्ठी वीरे श्रागमेण सया परकमेज्जासि ति बेमि ।
संस्कृतच्छाया - निर्देशं नातिवर्तेत मेधावी सुप्रत्युप्रेक्ष्य सर्वतः सर्वात्मना सम्यग् समभिज्ञाय इह आराम परिज्ञाय तीनो गुप्तश्च परिव्रजेत, निष्ठितार्थी वीरः श्रागमेन सदा पराक्रमथा इति ब्रवीमि ।
For Private And Personal