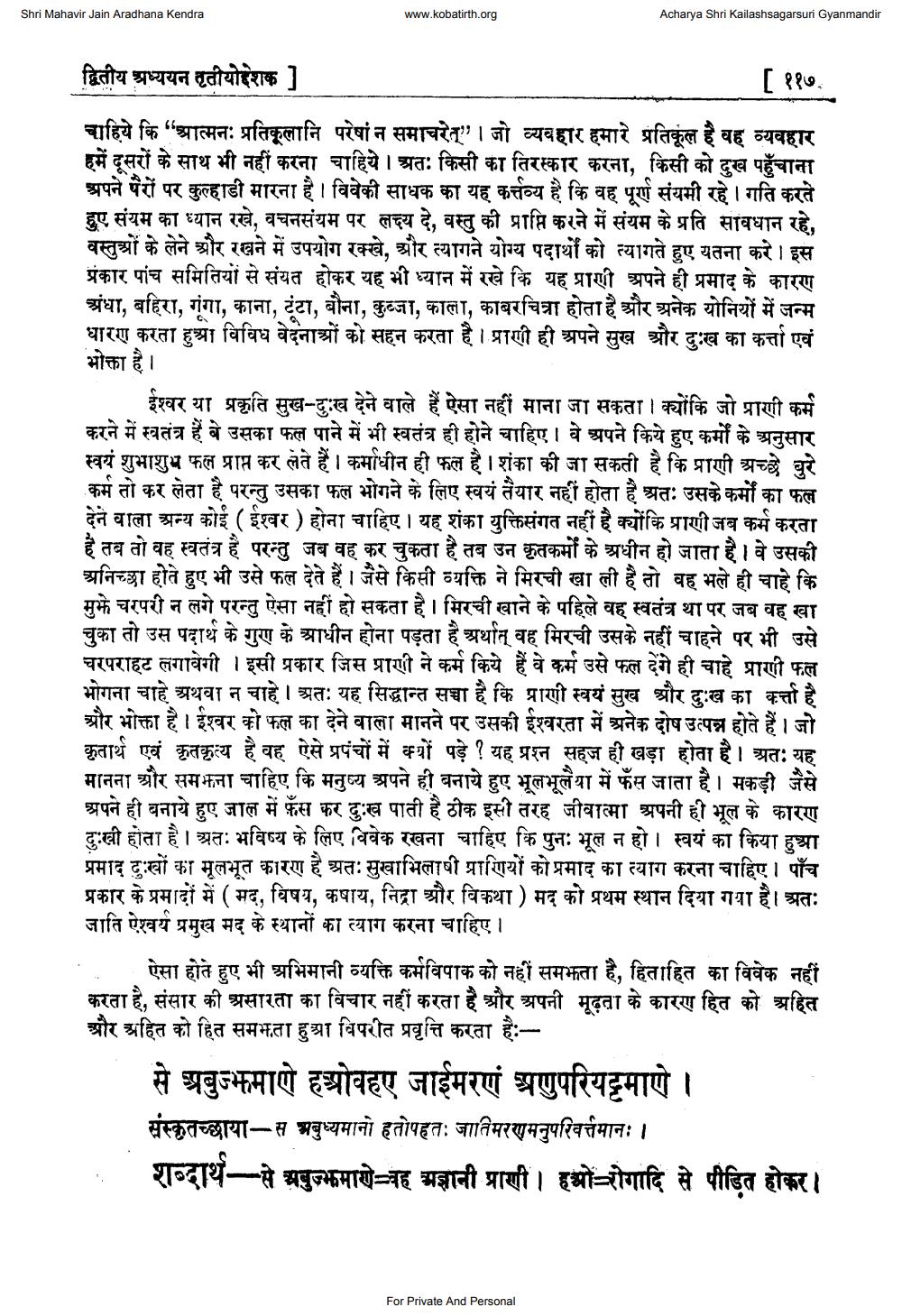________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
द्वितीय अध्ययन तृतीयोदेशक ]
[ ११७.
चाहिये कि "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्” । जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल है वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिये । अतः किसी का तिरस्कार करना, किसी को दुख पहुँचाना अपने पैरों पर कुल्हाडी मारना है । विवेकी साधक का यह कर्त्तव्य है कि वह पूर्ण संयमी रहे । गति करते हुए संयम का ध्यान रखे, वचनसंयम पर लक्ष्य दे, वस्तु की प्राप्ति करने में संयम के प्रति सावधान रहे, वस्तुओं के लेने और रखने में उपयोग रक्खे, और त्यागने योग्य पदार्थों को त्यागते हुए यतना करे। इस प्रकार पांच समितियों से संयत होकर यह भी ध्यान में रखे कि यह प्राणी अपने ही प्रमाद के कारण अंधा, बहिरा, गूंगा, काना, टूटा, बौना, कुब्जा, काला, काबर चित्रा होता है और अनेक योनियों में जन्म धारण करता हुआ विविध वेदनाओं को सहन करता है। प्राणी ही अपने सुख और दुःख का कर्त्ता एवं भोक्ता है।
ईश्वर या प्रकृति सुख-दुःख देने वाले हैं ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि जो प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं वे उसका फल पाने में भी स्वतंत्र ही होने चाहिए। वे अपने किये हुए कर्मों के अनुसार स्वयं शुभाशुभ फल प्राप्त कर लेते हैं। कर्माधीन ही फल है। शंका की जा सकती है कि प्राणी अच्छे बुरे कर्म तो कर लेता है परन्तु उसका फल भोगने के लिए स्वयं तैयार नहीं होता है अतः उसके कर्मों का फल देने वाला अन्य कोई (ईश्वर) होना चाहिए। यह शंका युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि प्राणी जब कर्म करता है तब तो वह स्वतंत्र है परन्तु जब वह कर चुकता है तब उन कृतकर्मों के अधीन हो जाता है। वे उसकी अनिच्छा होते हुए भी उसे फल देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मिरची खा ली है तो वह भले ही चाहे कि मुझे चरपरी न लगे परन्तु ऐसा नहीं हो सकता है। मिरची खाने के पहिले वह स्वतंत्र था पर जब वह खा चुका तो उस पदार्थ के गुण के आधीन होना पड़ता है अर्थात् वह मिरची उसके नहीं चाहने पर भी उसे चरपराहट लगावेगी । इसी प्रकार जिस प्रारणी ने कर्म किये हैं वे कर्म उसे फल देंगे ही चाहे प्राणी फल भोगना चाहे अथवा न चाहे । अतः यह सिद्धान्त सच्चा है कि प्राणी स्वयं सुख और दुःख का कर्त्ता है और भोक्ता है। ईश्वर को फल का देने वाला मानने पर उसकी ईश्वरता में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । जो कृतार्थ एवं कृतकृत्य है वह ऐसे प्रपंचों में क्यों पड़े ? यह प्रश्न सहज ही खड़ा होता है । अतः यह मानना और समझना चाहिए कि मनुष्य अपने ही बनाये हुए भूलभूलैया में फँस जाता है । मकड़ी जैसे अपने ही बनाये हुए जाल में फँस कर दुःख पाती है ठीक इसी तरह जीवात्मा अपनी ही भूल के कारण दुःख होता है । अतः भविष्य के लिए विवेक रखना चाहिए कि पुनः भूल न हो । स्वयं का किया हुआ प्रमाद दुःखों का मूलभूत कारण है अतः सुखाभिलाषी प्राणियों को प्रमाद का त्याग करना चाहिए। पाँच प्रकार के प्रमादों में (मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा ) मद को प्रथम स्थान दिया गया है। अतः जाति ऐश्वर्य प्रमुख मद के स्थानों का त्याग करना चाहिए ।
ऐसा होते हुए भी अभिमानी व्यक्ति कर्मविपाक को नहीं समझता है, हिताहित का विवेक नहीं करता है, संसार की असारता का विचार नहीं करता है और अपनी मूढ़ता के कारण हित को अहित औरत को हित सममता हुआ विपरीत प्रवृत्ति करता है:
से बुज्झमाणे होव जाईमरणं श्रणुपरियट्टमाये । संस्कृतच्छाया - स अबुध्यमानो हतोपहतः जातिमरणमनुपरिवर्त्तमानः ।
शब्दार्थ - से अबुज्झमाणे- वह अज्ञानी प्राणी । हम रोगादि से पीड़ित होकर ।
For Private And Personal