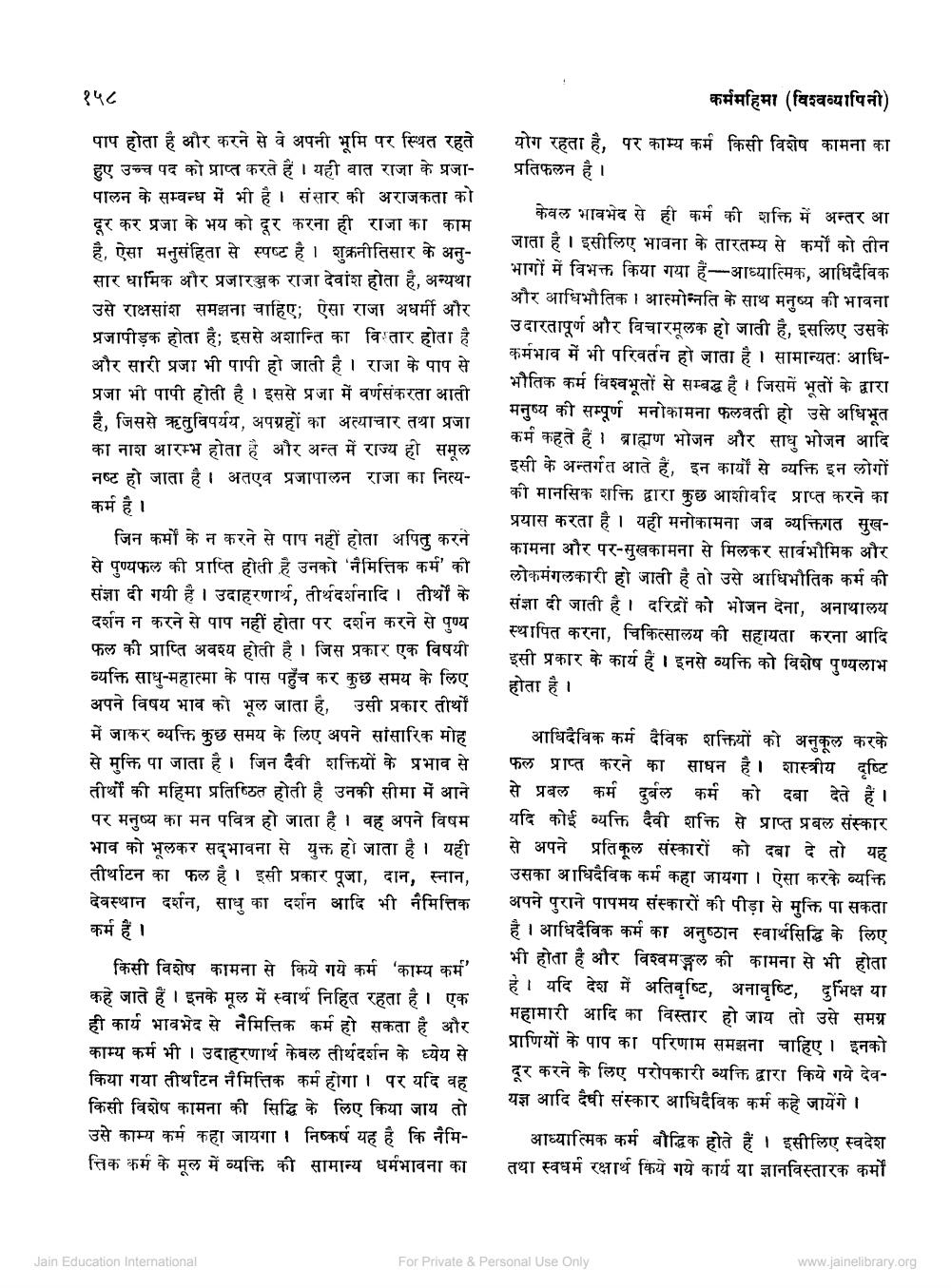________________
१५८
कर्ममहिमा (विश्वव्यापिनी)
योग रहता है, पर काम्य कर्म किसी विशेष कामना का प्रतिफलन है।
पाप होता है और करने से वे अपनी भूमि पर स्थित रहते हुए उच्च पद को प्राप्त करते हैं । यही बात राजा के प्रजा- पालन के सम्बन्ध में भी है। संसार की अराजकता को दूर कर प्रजा के भय को दूर करना ही राजा का काम है, ऐसा मनुसंहिता से स्पष्ट है । शुक्रनीतिसार के अनुसार धार्मिक और प्रजारञ्जक राजा देवांश होता है, अन्यथा उसे राक्षसांश समझना चाहिए; ऐसा राजा अधर्मी और प्रजापीड़क होता है; इससे अशान्ति का विस्तार होता है और सारी प्रजा भी पापी हो जाती है। राजा के पाप से प्रजा भी पापी होती है । इससे प्रजा में वर्णसंकरता आती है, जिससे ऋतुविपर्यय, अपग्रहों का अत्याचार तथा प्रजा का नाश आरम्भ होता है और अन्त में राज्य हो समूल नष्ट हो जाता है। अतएव प्रजापालन राजा का नित्यकर्म है।
जिन कर्मों के न करने से पाप नहीं होता अपितु करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है उनको 'नैमित्तिक कर्म' की संज्ञा दी गयी है। उदाहरणार्थ, तीर्थदर्शनादि । तीर्थों के दर्शन न करने से पाप नहीं होता पर दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार एक विषयी व्यक्ति साधु-महात्मा के पास पहुँच कर कुछ समय के लिए अपने विषय भाव को भूल जाता है, उसी प्रकार तीर्थों में जाकर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने सांसारिक मोह से मुक्ति पा जाता है। जिन दैवी शक्तियों के प्रभाव से तीर्थों की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने पर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। वह अपने विषम भाव को भूलकर सद्भावना से युक्त हो जाता है। यही तीर्थाटन का फल है। इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, देवस्थान दर्शन, साधु का दर्शन आदि भी नैमित्तिक कर्म है।
किसी विशेष कामना से किये गये कर्म 'काम्य कर्म' कहे जाते हैं । इनके मूल में स्वार्थ निहित रहता है। एक ही कार्य भावभेद से नैमित्तिक कर्म हो सकता है और काम्य कर्म भी । उदाहरणार्थ केवल तीर्थदर्शन के ध्येय से किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक कर्म होगा। पर यदि वह किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए किया जाय तो उसे काम्य कर्म कहा जायगा । निष्कर्ष यह है कि नैमित्तिक कर्म के मूल में व्यक्ति की सामान्य धर्मभावना का
केवल भावभेद से ही कर्म की शक्ति में अन्तर आ जाता है। इसीलिए भावना के तारतम्य से कर्मों को तीन भागों में विभक्त किया गया हैं-आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक । आत्मोन्नति के साथ मनुष्य की भावना उदारतापूर्ण और विचारमूलक हो जाती है, इसलिए उसके कर्मभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः आधिभौतिक कर्म विश्वभूतों से सम्बद्ध है । जिसमें भूतों के द्वारा मनुष्य की सम्पूर्ण मनोकामना फलवती हो उसे अधिभूत कर्म कहते हैं। ब्राह्मण भोजन और साधु भोजन आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं, इन कार्यों से व्यक्ति इन लोगों की मानसिक शक्ति द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही मनोकामना जब व्यक्तिगत सुखकामना और पर-सुखकामना से मिलकर सार्वभौमिक और लोकमंगलकारी हो जाती है तो उसे आधिभौतिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। दरिद्रों को भोजन देना, अनाथालय स्थापित करना, चिकित्सालय की सहायता करना आदि इसी प्रकार के कार्य हैं। इनसे व्यक्ति को विशेष पुण्यलाभ होता है।
आधिदैविक कर्म दैविक शक्तियों को अनुकूल करके फल प्राप्त करने का साधन है। शास्त्रीय दृष्टि से प्रबल कर्म दुर्बल कर्म को दबा देते हैं । यदि कोई व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रबल संस्कार से अपने प्रतिकूल संस्कारों को दबा दे तो यह उसका आधिदैविक कर्म कहा जायगा। ऐसा करके व्यक्ति अपने पुराने पापमय संस्कारों की पीड़ा से मुक्ति पा सकता है । आधिदैविक कर्म का अनुष्ठान स्वार्थसिद्धि के लिए भी होता है और विश्वमङ्गल की कामना से भी होता है। यदि देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष या महामारी आदि का विस्तार हो जाय तो उसे समग्र प्राणियों के पाप का परिणाम समझना चाहिए। इनको दूर करने के लिए परोपकारी व्यक्ति द्वारा किये गये देवयज्ञ आदि देषी संस्कार आधिदैविक कर्म कहे जायेंगे।
आध्यात्मिक कर्म बौद्धिक होते हैं । इसीलिए स्वदेश तथा स्वधर्म रक्षार्थ किये गये कार्य या ज्ञानविस्तारक कर्मों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org