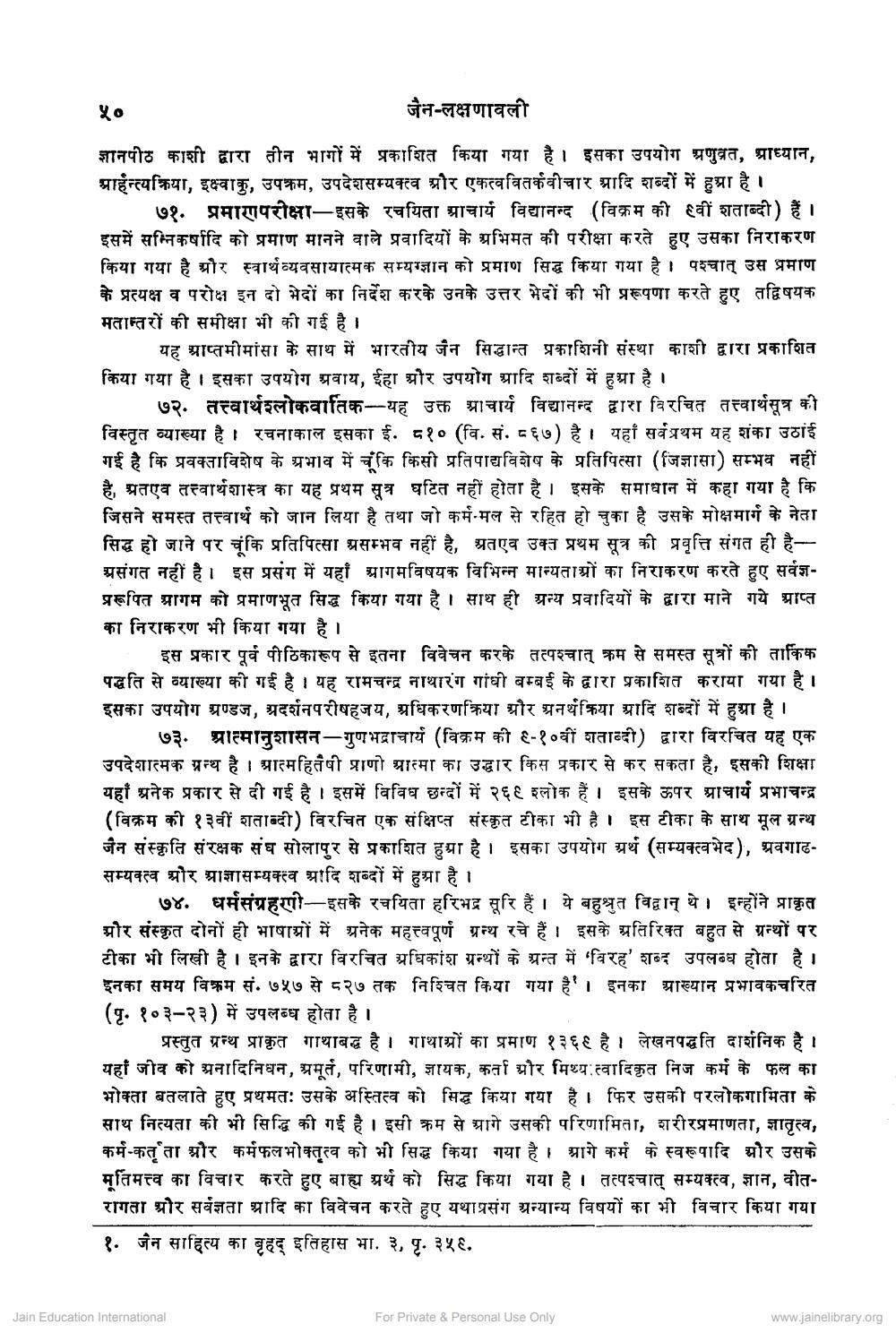________________
जैन-लक्षणावली
ज्ञानपीठ काशी द्वारा तीन भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग अणुव्रत, प्राध्यान, पार्हन्त्यक्रिया, इक्ष्वाकु, उपक्रम, उपदेशसम्यक्त्व और एकत्ववितर्कवीचार आदि शब्दों में हा है।
७१. प्रमारणपरीक्षा-इसके रचयिता प्राचार्य विद्यानन्द (विक्रम की हवीं शताब्दी) हैं। इसमें सम्निकर्षादि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियों के अभिमत की परीक्षा करते हुए उसका निराकरण
और स्वार्थव्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया गया है। पश्चात उस प्रमाण के प्रत्यक्ष व परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश करके उनके उत्तर भेदों की भी प्ररूपणा करते हुए तद्विषयक मतान्तरों की समीक्षा भी की गई है।
यह प्राप्तमीमांसा के साथ में भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग अवाय, ईहा और उपयोग आदि शब्दों में हरा है।
७२. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक-यह उक्त प्राचार्य विद्यानन्द द्वारा बिरचित तत्त्वार्थसूत्र की विस्तृत व्याख्या है। रचनाकाल इसका ई. ८१० (वि. सं. ८६७) है। यहाँ सर्वप्रथम यह शंका उठाई गई है कि प्रवक्ताविशेष के अभाव में चंकि किसी प्रतिपाद्यविशेष के प्रतिपित्सा (जिज्ञासा) सम्भव नहीं है, प्रतएव तत्त्वार्थशास्त्र का यह प्रथम सूत्र घटित नहीं होता है। इसके समाधान में कहा गया है कि जिसने समस्त तत्त्वार्थ को जान लिया है तथा जो कर्म-मल से रहित हो चुका है उसके मोक्षमार्ग के नेता सिद्ध हो जाने पर चंकि प्रतिपित्सा असम्भव नहीं है, अतएव उक्त प्रथम सत्र की प्रवृत्ति संगत ही हैअसंगत नहीं है। इस प्रसंग में यहाँ आगमविषयक विभिन्न मान्यताओं का निराकरण करते हुए सर्वज्ञप्ररूपित पागम को प्रमाणभूत सिद्ध किया गया है। साथ ही अन्य प्रवादियों के द्वारा माने गये प्राप्त का निराकरण भी किया गया है।
इस प्रकार पूर्व पीठिकारूप से इतना विवेचन करके तत्पश्चात् क्रम से समस्त सूत्रों की ताकिक पद्धति से व्याख्या की गई है। यह रामचन्द्र नाथारंग गांधी बम्बई के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसका उपयोग अण्डज, अदर्शनपरीषहजय, अधिकरणक्रिया और अनर्थक्रिया आदि शब्दों में हुआ है ।
७३. प्रात्मानुशासन-गुणभद्राचार्य (विक्रम की ९-१०वीं शताब्दी) द्वारा विरचित यह एक उपदेशात्मक ग्रन्थ है। आत्महितैषी प्राणो प्रात्मा का उद्धार किस प्रकार से कर सकता है, इसकी शिक्षा यहाँ अनेक प्रकार से दी गई है। इसमें विविध छन्दों में २६६ श्लोक हैं। इसके ऊपर प्राचार्य प्रभाचन्द्र (विक्रम की १३वीं शताब्दी) विरचित एक संक्षिप्त संस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ मूल ग्रन्थ जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित हया है। इसका उपयोग अर्थ (सम्यक्त्वभेद), अवगाढसम्यक्त्व और प्राज्ञासम्यक्त्व आदि शब्दों में हया है।।
७४. धर्मसंग्रहरणी-इसके रचयिता हरिभद्र सूरि हैं। ये बहुश्रुत विद्वान् थे। इन्होंने प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ग्रन्थों पर टीका भी लिखी है । इनके द्वारा विरचित अधिकांश ग्रन्थों के अन्त में 'विरह' शब्द उपलब्ध होता है। इनका समय विक्रम सं. ७५७ से ८२७ तक निश्चित किया गया है। इनका आख्यान प्रभावकचरित (पृ. १०३-२३) में उपलब्ध होता है।
प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत गाथाबद्ध है। गाथाओं का प्रमाण १३६६ है। लेखनपद्धति दार्शनिक है। यहाँ जीव को अनादिनिधन, अमूर्त, परिणामी, ज्ञायक, कर्ता और मिथ्य त्वादिकृत निज कर्म के फल का भोक्ता बतलाते हुए प्रथमतः उसके अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। फिर उसकी परलोकगामिता के साथ नित्यता की भी सिद्धि की गई है। इसी क्रम से आगे उसकी परिणामिता, शरीरप्रमाण कर्म-कर्तृता और कर्मफलभोक्तृत्व को भी सिद्ध किया गया है। आगे कर्म के स्वरूपादि और उसके मतिमत्त्व का विचार करते हुए बाह्य अर्थ को सिद्ध किया गया है। तत्पश्चात् सम्यक्त्व, ज्ञान, वीतरागता और सर्वज्ञता आदि का विवेचन करते हए यथाप्रसंग अन्यान्य विषयों का भी विचार किया गया १. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा. ३, पृ. ३५६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org