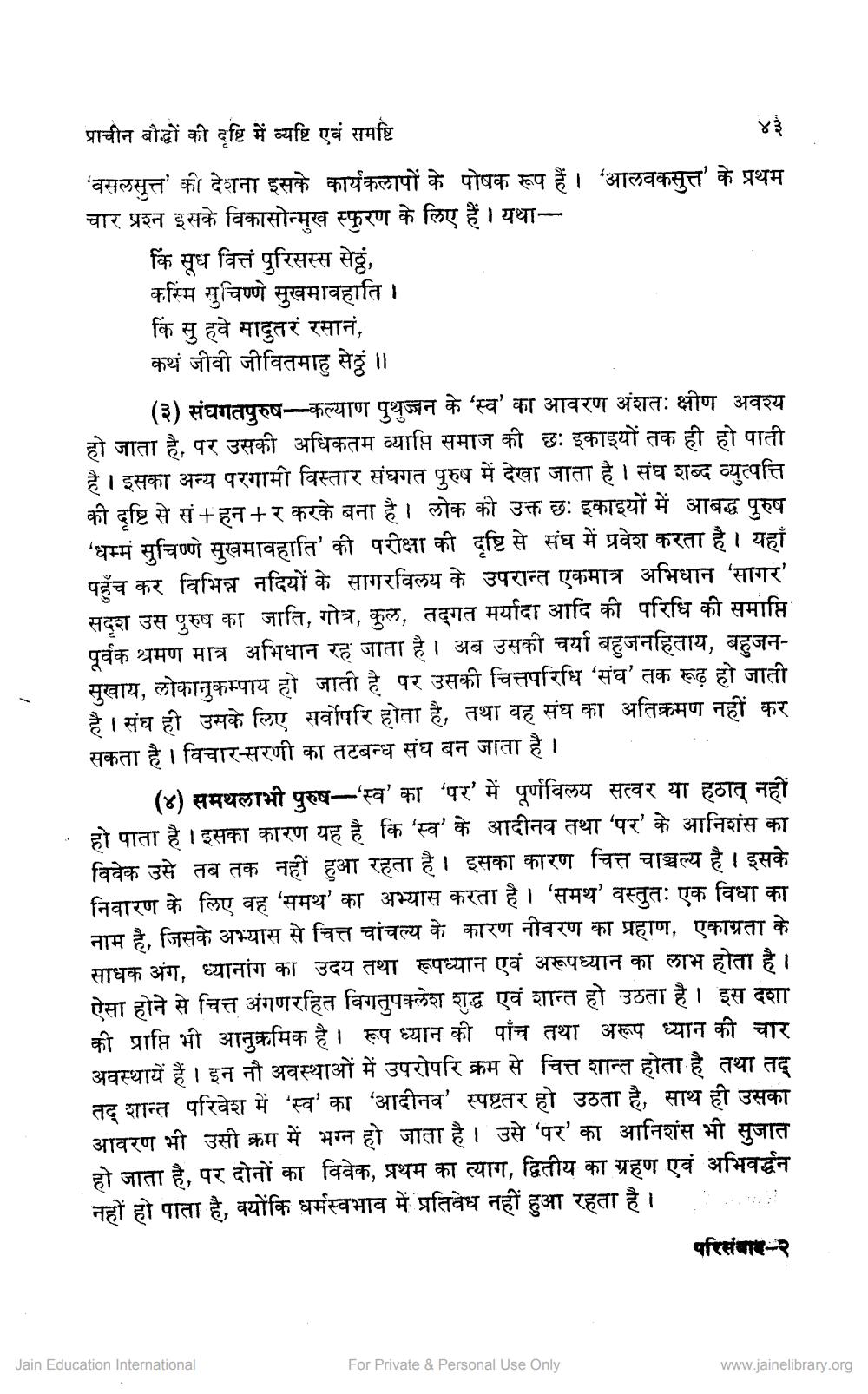________________
प्राचीन बौद्धों की दृष्टि में व्यष्टि एवं समष्टि
જરૂ
'वसलसुत्त' की देशना इसके कार्यकलापों के पोषक रूप हैं । 'आलवकसुत्त' के प्रथम चार प्रश्न इसके विकासोन्मुख स्फुरण के लिए हैं। यथा
किं सूध वित्तं पुरिसस्स सेठ्ठे, कस्मि सुचिणे सुखमावहाति । किं सु हवे मादुतरं रसानं,
कथं जीवी जीवितमाहु सेठ्ठे ॥
(३) संघगतपुरुष- - कल्याण पुथुज्जन के 'स्व' का आवरण अंशतः क्षीण अवश्य हो जाता है, पर उसकी अधिकतम व्याप्ति समाज की छः इकाइयों तक ही हो पाती है । इसका अन्य परगामी विस्तार संघगत पुरुष में देखा जाता है। संघ शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सं+ न + र करके बना है। लोक की उक्त छः इकाइयों में आबद्ध पुरुष 'धम्मं सुचिणे सुखमावहाति' की परीक्षा की दृष्टि से संघ में प्रवेश करता है । यहाँ पहुँच कर विभिन्न नदियों के सागरविलय के उपरान्त एकमात्र अभिधान 'सागर' सदृश उस पुरुष का जाति, गोत्र, कुल, तद्गत मर्यादा आदि की परिधि की समाप्ति पूर्वक श्रमण मात्र अभिधान रह जाता है। अब उसकी चर्या बहुजनहिताय, बहुजन - सुखाय, लोकानुकम्पाय हो जाती है पर उसकी चित्तपरिधि 'संघ' तक रूढ़ हो जाती है | संघ ही उसके लिए सर्वोपरि होता है, तथा वह संघ का अतिक्रमण नहीं कर सकता है । विचार सरणी का तटबन्ध संघ बन जाता है ।
(४) समथलाभी पुरुष - 'स्व' का 'पर' में पूर्णविलय सत्वर या हठात् नहीं हो पाता है । इसका कारण यह है कि 'स्व' के आदीनव तथा 'पर' के आनिशंस का विवेक उसे तब तक नहीं हुआ रहता है। इसका कारण चित्त चाञ्चल्य है । इसके निवारण के लिए वह 'समर्थ' का अभ्यास करता है । 'समर्थ' वस्तुतः एक विधा का नाम है, जिसके अभ्यास से चित्त चांचल्य के कारण नीवरण का प्रहाण, एकाग्रता के साधक अंग, ध्यानांग का उदय तथा रूपध्यान एवं अरूपध्यान का लाभ होता है । ऐसा होने से चित्त अंगणरहित विगतुपक्लेश शुद्ध एवं शान्त हो उठता है । इस दशा की प्राप्ति भी आनुक्रमिक है । रूप ध्यान की पाँच तथा अरूप ध्यान की चार अवस्थायें हैं । इन नौ अवस्थाओं में उपरोपरि क्रम से चित्त शान्त होता है तथा तद् तद् शान्त परिवेश में 'स्व' का 'आदीनव' स्पष्टतर हो उठता है, साथ ही उसका आवरण भी उसी क्रम में भग्न हो जाता है। उसे 'पर' का आनिशंस भी सुजात हो जाता है, पर दोनों का विवेक, प्रथम का त्याग, द्वितीय का ग्रहण एवं अभिवर्द्धन नहीं हो पाता है, क्योंकि धर्मस्वभाव में प्रतिवेध नहीं हुआ रहता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
परिसंवाद-२
www.jainelibrary.org