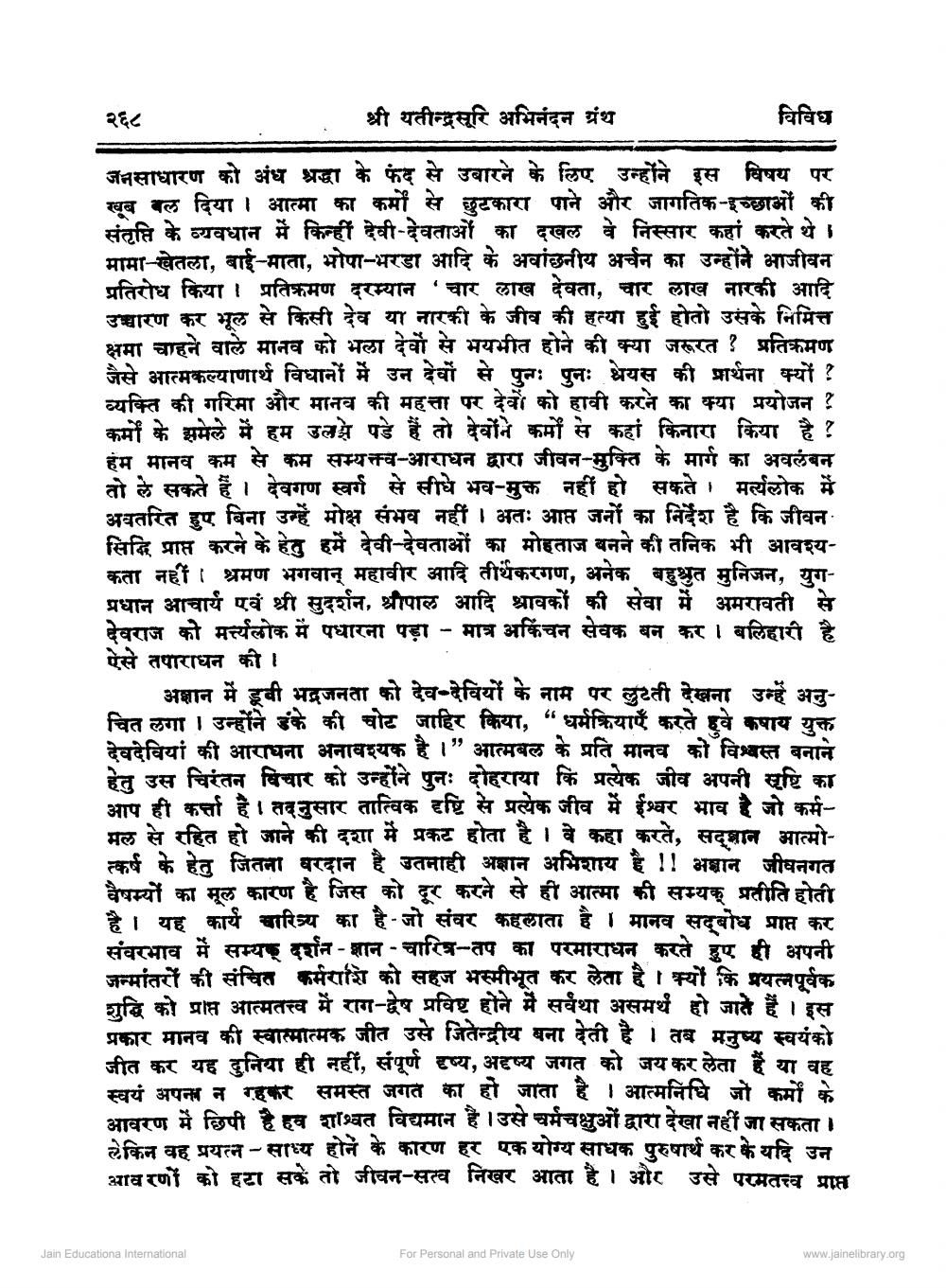________________
२६८
श्री यतीन्द्रसूरि अभिनंदन ग्रंथ
विविध
जनसाधारण को अंध श्रद्धा के फंद से उबारने के लिए उन्होंने इस विषय पर खब बल दिया। आत्मा का कर्मों से छुटकारा पाने और जागतिक-इच्छाओं की संतृप्ति के व्यवधान में किन्हीं देवी-देवताओं का दखल वे निस्सार कहां करते थे । मामा-खेतला, बाई-माता, भोपा-भरडा आदि के अवांछनीय अर्चन का उन्होंने आजीवन प्रतिरोध किया। प्रतिक्रमण दरम्यान 'चार लाख देवता, चार लाख नारकी आदि उच्चारण कर भूल से किसी देव या नारकी के जीव की हत्या हुई होतो उसके निमित्त क्षमा चाहने वाले मानव को भला देवों से भयभीत होने की क्या जरूरत ? प्रतिक्रमण जैसे आत्मकल्याणार्थ विधानों में उन देवों से पुनः पुनः श्रेयस की प्रार्थना क्यों ? व्यक्ति की गरिमा और मानव की महत्ता पर देवो को हावी करने का क्या प्रयोजन ? कर्मों के झमेले में हम उलझे पडे हैं तो देवोंने कमों से कहां किनारा किया है ? हम मानव कम से कम सम्यक्त्व-आराधन द्वारा जीवन-मुक्ति के मार्ग का अवलंबन तो ले सकते हैं। देवगण स्वर्ग से सीधे भव-मुक्त नहीं हो सकते । मर्त्यलोक में अवतरित हुए बिना उन्हें मोक्ष संभव नहीं । अतः आप्त जनों का निर्देश है कि जीवन सिद्धि प्राप्त करने के हेतु हमें देवी-देवताओं का मोहताज बनने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। श्रमण भगवान् महावीर आदि तीर्थकरगण, अनेक बहुश्रुत मुनिजन, युगप्रधान आचार्य एवं श्री सुदर्शन, श्रीपाल आदि श्रावकों की सेवा में अमरावती से देवराज को मर्त्यलोक में पधारना पड़ा - मात्र अकिंचन सेवक बन कर । बलिहारी है ऐसे तपाराधन की।
अज्ञान में डूबी भद्रजनता को देव-देवियों के नाम पर लुटती देखना उन्हें अनुचित लगा । उन्होंने डंके की चोट जाहिर किया, “धर्मक्रियाएँ करते हुवे कषाय युक्त देवदेवियां की आराधना अनावश्यक है ।" आत्मबल के प्रति मानव को विश्वस्त बनाने हेतु उस चिरंतन विचार को उन्होंने पुनः दोहराया कि प्रत्येक जीव अपनी सृष्टि का आप ही कर्ता है । तदनुसार तात्विक दृष्टि से प्रत्येक जीव में ईश्वर भाव है जो कर्ममल से रहित हो जाने की दशा में प्रकट होता है । वे कहा करते, सदनान आत्मोस्कर्ष के हेतु जितना वरदान है उतनाही अज्ञान अभिशाय है !! अचान जीवनगत वैषम्यों का मूल कारण है जिस को दूर करने से ही आत्मा की सम्यक् प्रतीति होती है। यह कार्य चारित्र्य का है - जो संवर कहलाता है । मानव सद्बोध प्राप्त कर संवरभाव में सम्यक् दर्शन - शान - चारित्र-तप का परमाराधन करते हुए ही अपनी जन्मांतरों की संचित कर्मराशि को सहज भस्मीभूत कर लेता है। क्यों कि प्रयत्नपूर्वक शुद्धि को प्राप्त आत्मतत्त्व में राग-द्वेष प्रविष्ट होने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव की स्वास्मात्मक जीत उसे जितेन्द्रीय बना देती है । तब मनुष्य स्वयंको जीत कर यह दुनिया ही नहीं, संपूर्ण दृष्य, अदृष्य जगत को जय कर लेता हैं या वह स्वयं अपना न रहकर समस्त जगत का हो जाता है । आत्मनिधि जो कर्मों के आवरण में छिपी है हव शाश्वत विद्यमान है । उसे चर्मचक्षुओं द्वारा देखा नहीं जा सकता। लेकिन वह प्रयत्न - साध्य होने के कारण हर एक योग्य साधक पुरुषार्थ कर के यदि उन आवरणों को हटा सके तो जीवन-सत्व निखर आता है । और उसे परमतत्त्व प्राप्त
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org