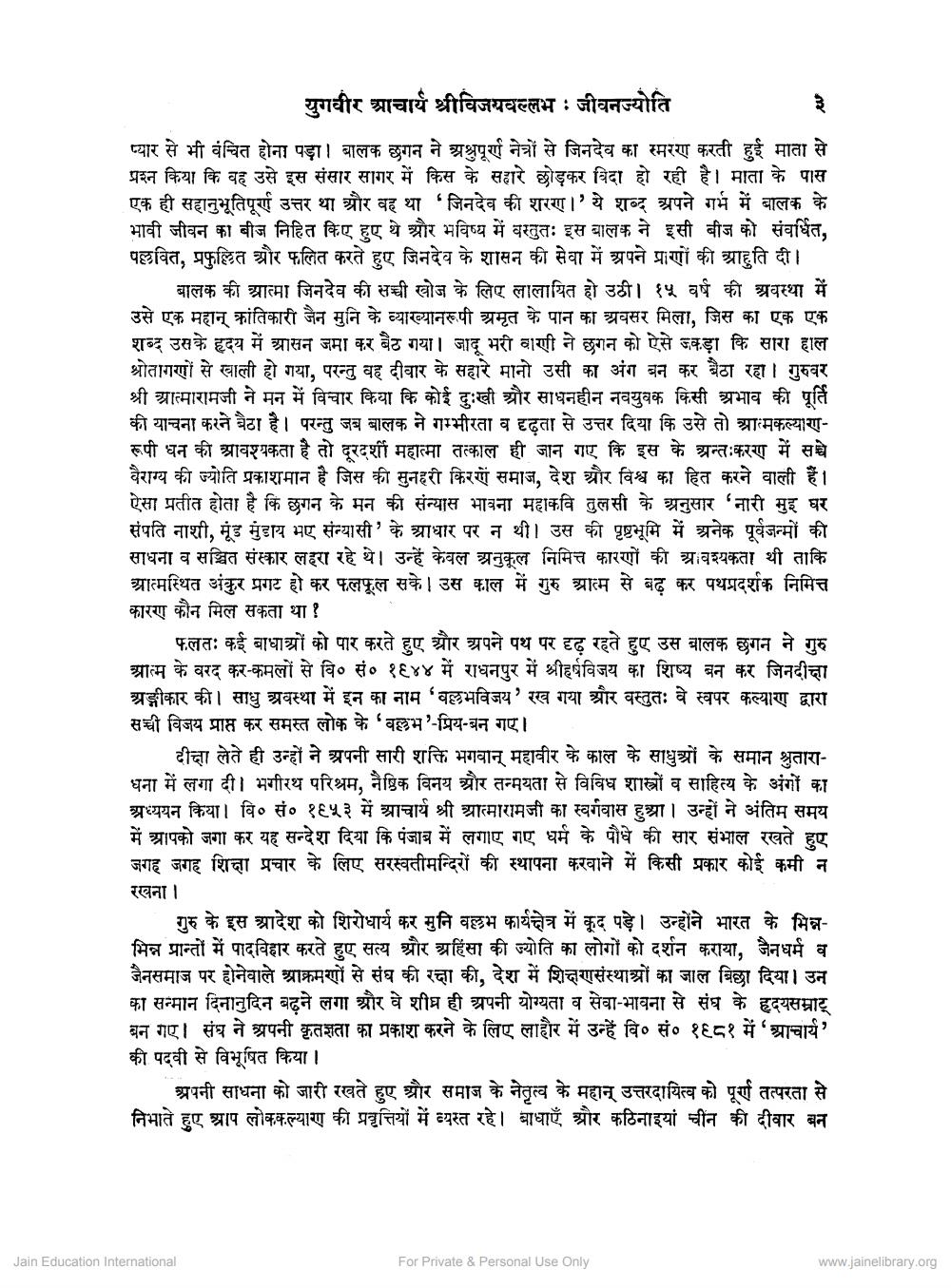________________
३
युगवीर आचार्य श्रीविजयवल्लभ : जीवनज्योति
प्यार से भी वंचित होना पड़ा। बालक छगन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से जिनदेव का स्मरण करती हुई माता से प्रश्न किया कि वह उसे इस संसार सागर में किस के सहारे छोड़कर विदा हो रही है। माता के पास एक ही सहानुभूतिपूर्ण उत्तर था और वह था 'जिनदेव की शरण ।' ये शब्द अपने गर्भ में बालक के भावी जीवन का बीज निहित किए हुए थे और भविष्य में वस्तुतः इस बालक ने इसी बीज को संवर्धित, पल्लवित, प्रफुल्लित और फलित करते हुए जिनदेव के शासन की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।
बालक की आत्मा जिनदेव की सच्ची खोज के लिए लालायित हो उठी । १५ वर्ष की अवस्था में उसे एक महान् क्रांतिकारी जैन मुनि के व्याख्यानरूपी अमृत के पान का अवसर मिला, जिस का एक एक शब्द उसके हृदय में श्रासन जमा कर बैठ गया । जादू भरी वाणी ने छगन को ऐसे जकड़ा कि सारा हाल श्रोतागणों से खाली हो गया, परन्तु वह दीवार के सहारे मानो उसी का अंग बन कर बैठा रहा । गुरुवर श्री आत्मारामजी ने मन में विचार किया कि कोई दुःखी और साधनहीन नवयुवक किसी भाव की पूर्ति की याचना करने बैठा है । परन्तु जब बालक ने गम्भीरता व दृढ़ता से उत्तर दिया कि उसे तो आत्मकल्याणरूपी धन की आवश्यकता है तो दूरदर्शी महात्मा तत्काल ही जान गए कि इस के अन्तःकरण में सच्चे वैराग्य की ज्योति प्रकाशमान है जिस की सुनहरी किरणें समाज, देश और विश्व का हित करने वाली हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि छगन के मन की संन्यास भावना महाकवि तुलसी के अनुसार 'नारी मुइ घर संपति नाशी, मूंड मुंडाय भए संन्यासी' के आधार पर न थी । उस की पृष्ठभूमि में अनेक पूर्वजन्मों की साधना व सञ्चित संस्कार लहरा रहे थे। उन्हें केवल अनुकूल निमित्त कारणों की आवश्यकता थी ताकि आत्मस्थित अंकुर प्रगट हो कर फलफूल सके। उस काल में गुरु आत्म से बढ़ कर पथप्रदर्शक निमित्त कारण कौन मिल सकता था ?
फलतः कई बाधाओं को पार करते हुए और अपने पथ पर दृढ़ रहते हुए उस बालक छगन ने गुरु आत्म के वरद कर-कमलों से वि० सं० १६४४ में राधनपुर में श्रीहर्षविजय का शिष्य बन कर जिनदीक्षा अङ्गीकार की । साधु अवस्था में इन का नाम 'वल्लभविजय' रख गया और वस्तुतः वे स्वपर कल्याण द्वारा सच्ची विजय प्राप्त कर समस्त लोक के 'वल्लभ' प्रिय बन गए ।
दीक्षा लेते ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति भगवान् महावीर के काल के साधुओं के समान श्रुताराधना में लगा दी। भगीरथ परिश्रम, नैष्ठिक विनय और तन्मयता से विविध शास्त्रों व साहित्य के अंगों का अध्ययन किया। वि० सं० १९५३ में श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी का स्वर्गवास हुआ। उन्हों ने अंतिम समय में आपको जगा कर यह सन्देश दिया कि पंजाब में लगाए गए धर्म के पौधे की सार संभाल रखते हुए जगह जगह शिक्षा प्रचार के लिए सरस्वतीमन्दिरों की स्थापना करवाने में किसी प्रकार कोई कमी न
रखना ।
गुरु के इस आदेश को शिरोधार्य कर मुनि वल्लभ कार्यक्षेत्र में कूद । उन्होंने भारत के भिन्नभिन्न प्रान्तों में पादविहार करते हुए सत्य और अहिंसा की ज्योति का लोगों को दर्शन कराया, जैनधर्म व जैन समाज पर होनेवाले श्राक्रमणों से संघ की रक्षा की, देश में शिक्षणसंस्थानों का जाल बिछा दिया। उन का सन्मान दिनानुदिन बढ़ने लगा और वे शीघ्र ही अपनी योग्यता व सेवा भावना से संघ के हृदयसम्राट् बन गए। संघ ने अपनी कृतज्ञता का प्रकाश करने के लिए लाहौर में उन्हें वि० सं० १६८१ में ' श्राचार्य ' की पदवी से विभूषित किया ।
अपनी साधना को जारी रखते हुए और समाज के नेतृत्व के महान् उत्तरदायित्व को पूर्ण तत्परता से निभाते हुए श्राप लोककल्याण की प्रवृत्तियों में व्यस्त रहे । बाधाएँ और कठिनाइयां चीन की दीवार बन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org