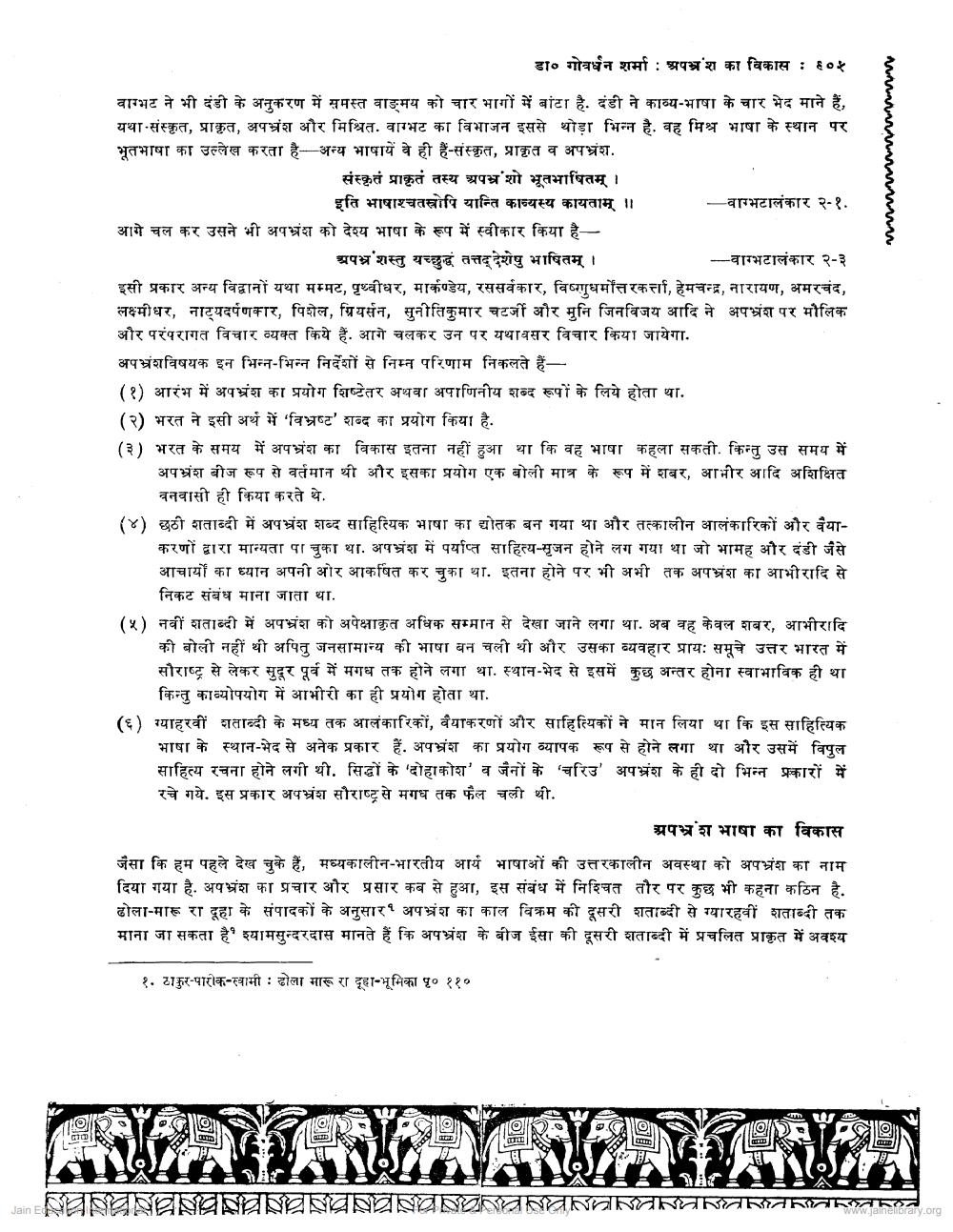________________
डा. गोवर्धन शर्मा : अपभ्रश का विकास : १०५
वाग्भट ने भी दंडी के अनुकरण में समस्त वाङ्मय को चार भागों में बांटा है. दंडी ने काव्य-भाषा के चार भेद माने हैं, यथा-संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्रित. वाग्भट का विभाजन इससे थोड़ा भिन्न है. वह मिश्र भाषा के स्थान पर भूतभाषा का उल्लेख करता है—अन्य भाषायें वे ही हैं-संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश.
संस्कृतं प्राकृतं तस्य अपभ्रंशो भूतभाषितम् । इति भाषाश्चतस्रोपि यान्ति काव्यस्य कायताम् ।।
-वाग्भटालंकार २-१. आगे चल कर उसने भी अपभ्रंश को देश्य भाषा के रूप में स्वीकार किया हैअपभ्रशस्तु यच्छुद्धं तत्तद्देशेषु भाषितम् ।
-वाग्भटालंकार २-३ इसी प्रकार अन्य विद्वानों यथा मम्मट, पृथ्वीधर, मार्कण्डेय, रससर्वकार, विष्णुधर्मोत्तरकर्त्ता, हेमचन्द्र, नारायण, अमरचंद, लक्ष्मीधर, नाट्यदर्पणकार, पिशेल, ग्रियर्सन, सुनीतिकुमार चटर्जी और मुनि जिनविजय आदि ने अपभ्रंश पर मौलिक और परंपरागत विचार व्यक्त किये हैं. आगे चलकर उन पर यथावसर विचार किया जायेगा. अपभ्रंशविषयक इन भिन्न-भिन्न निर्देशों से निम्न परिणाम निकलते हैं(१) आरंभ में अपभ्रंश का प्रयोग शिष्टेतर अथवा अपाणिनीय शब्द रूपों के लिये होता था. (२) भरत ने इसी अर्थ में 'विभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया है. (३) भरत के समय में अपभ्रंश का विकास इतना नहीं हुआ था कि वह भाषा कहला सकती. किन्तु उस समय में
अपभ्रंश बीज रूप से वर्तमान थी और इसका प्रयोग एक बोली मात्र के रूप में शबर, आभीर आदि अशिक्षित वनवासी ही किया करते थे. छठी शताब्दी में अपभ्रंश शब्द साहित्यिक भाषा का द्योतक बन गया था और तत्कालीन आलंकारिकों और वैयाकरणों द्वारा मान्यता पा चुका था. अपभ्रंश में पर्याप्त साहित्य-सृजन होने लग गया था जो भामह और दंडी जैसे आचार्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुका था. इतना होने पर भी अभी तक अपभ्रंश का आभीरादि से
निकट संबंध माना जाता था. (५) नवीं शताब्दी में अपभ्रंश को अपेक्षाकृत अधिक सम्मान से देखा जाने लगा था. अब वह केवल शबर, आभीरादि
की बोली नहीं थी अपितु जनसामान्य की भाषा बन चली थी और उसका व्यवहार प्रायः समूचे उत्तर भारत में सौराष्ट्र से लेकर सुदूर पूर्व में मगध तक होने लगा था. स्थान-भेद से इसमें कुछ अन्तर होना स्वाभाविक ही था
किन्तु काव्योपयोग में आभीरी का ही प्रयोग होता था. (६) ग्याहरवीं शताब्दी के मध्य तक आलंकारिकों, वैयाकरणों और साहित्यिकों ने मान लिया था कि इस साहित्यिक
भाषा के स्थान-भेद से अनेक प्रकार हैं. अपभ्रंश का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था और उसमें विपुल साहित्य रचना होने लगी थी. सिद्धों के 'दोहाकोश' व जैनों के 'चरिउ' अपभ्रंश के ही दो भिन्न प्रकारों में रचे गये. इस प्रकार अपभ्रंश सौराष्ट्र से मगध तक फैल चली थी.
अपभ्रंश भाषा का विकास जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मध्यकालीन-भारतीय आर्य भाषाओं की उत्तरकालीन अवस्था को अपभ्रंश का नाम दिया गया है. अपभ्रंश का प्रचार और प्रसार कब से हुआ, इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना कठिन है. ढोला-मारू रा दूहा के संपादकों के अनुसार अपभ्रंश का काल विक्रम की दूसरी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जा सकता है। श्यामसुन्दरदास मानते हैं कि अपभ्रंश के बीज ईसा की दूसरी शताब्दी में प्रचलित प्राकृत में अवश्य
१. ठाकुर-पारीक-स्वामी : ढोला मारू रा हा भूमिका पृ० ११०
SAMRAOMETal
ATML
A
Jan FORENENANabebidanandana Dhahardhiarinthyhod.org