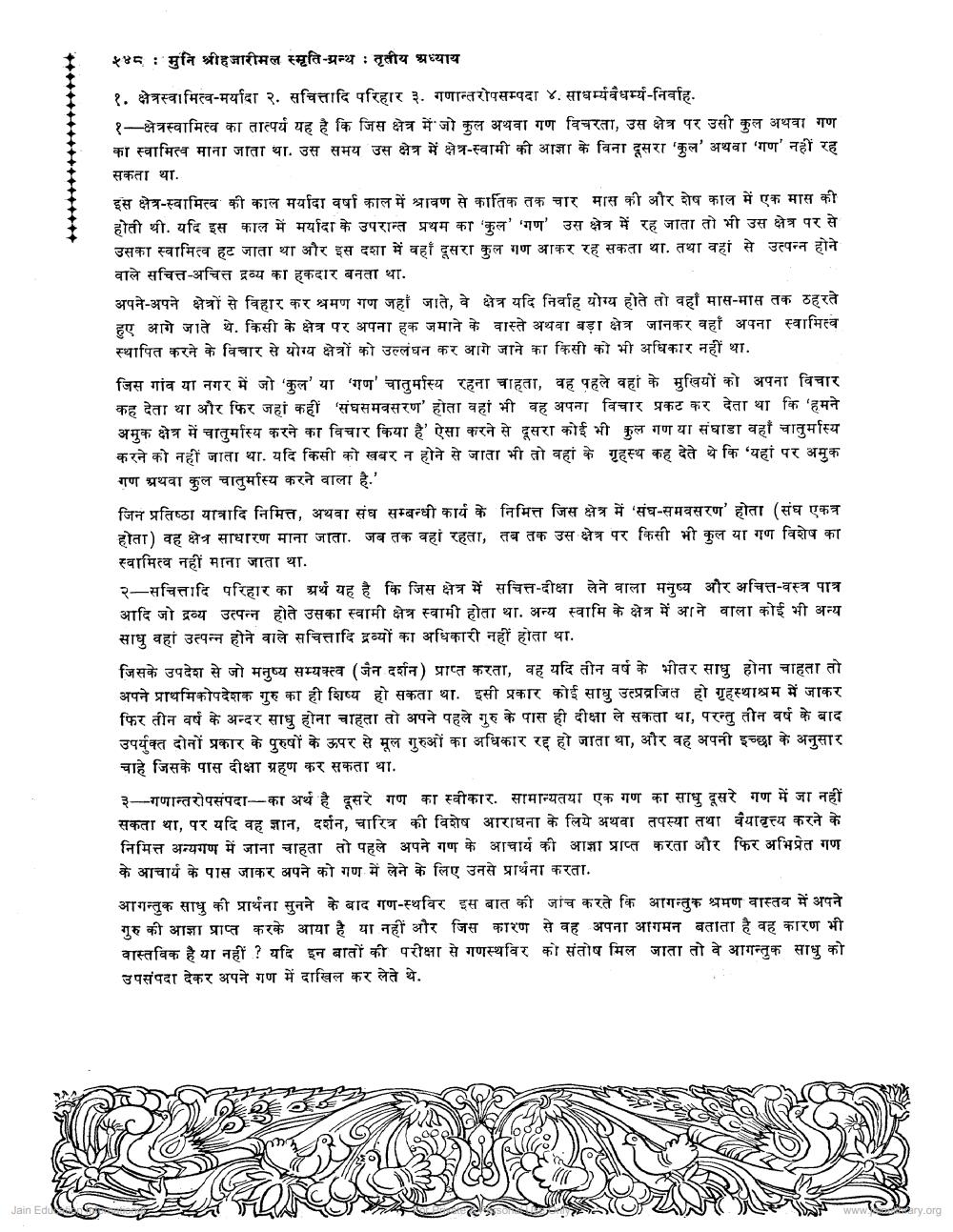________________
५४८ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : तृतीय अध्याय १. क्षेत्रस्वामित्व-मर्यादा २. सचित्तादि परिहार ३. गणान्तरोपसम्पदा ४. साधर्म्यवैधर्म्य-निर्वाह. १-क्षेत्रस्वामित्व का तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र में जो कुल अथवा गण विचरता, उस क्षेत्र पर उसी कुल अथवा गण का स्वामित्व माना जाता था. उस समय उस क्षेत्र में क्षेत्र-स्वामी की आज्ञा के विना दूसरा 'कुल' अथवा 'गण' नहीं रह सकता था. इस क्षेत्र-स्वामित्व की काल मर्यादा वर्षा काल में श्रावण से कार्तिक तक चार मास की और शेष काल में एक मास की होती थी. यदि इस काल में मर्यादा के उपरान्त प्रथम का 'कुल' 'गण' उस क्षेत्र में रह जाता तो भी उस क्षेत्र पर से उसका स्वामित्व हट जाता था और इस दशा में वहाँ दूसरा कुल गण आकर रह सकता था. तथा वहां से उत्पन्न होने वाले सचित्त-अचित्त द्रव्य का हकदार बनता था. अपने-अपने क्षेत्रों से विहार कर श्रमण गण जहाँ जाते, वे क्षेत्र यदि निर्वाह योग्य होते तो वहाँ मास-मास तक ठहरते हुए आगे जाते थे. किसी के क्षेत्र पर अपना हक जमाने के वास्ते अथवा बड़ा क्षेत्र जानकर वहाँ अपना स्वामित्व स्थापित करने के विचार से योग्य क्षेत्रों को उल्लंघन कर आगे जाने का किसी को भी अधिकार नहीं था. जिस गांव या नगर में जो 'कुल' या 'गण' चातुर्मास्य रहना चाहता, वह पहले वहां के मुखियों को अपना विचार कह देता था और फिर जहां कहीं 'संघसमवसरण' होता वहां भी वह अपना विचार प्रकट कर देता था कि 'हमने अमुक क्षेत्र में चातुर्मास्य करने का विचार किया है' ऐसा करने से दूसरा कोई भी कुल गण या संघाडा वहाँ चातुर्मास्य करने को नहीं जाता था. यदि किसी को खबर न होने से जाता भी तो वहां के गृहस्थ कह देते थे कि 'यहां पर अमुक गण अथवा कुल चातुर्मास्य करने वाला है.' जिन प्रतिष्ठा यात्रादि निमित्त, अथवा संघ सम्बन्धी कार्य के निमित्त जिस क्षेत्र में 'संघ-समवसरण' होता (संघ एकत्र होता) वह क्षेत्र साधारण माना जाता. जब तक वहां रहता, तब तक उस क्षेत्र पर किसी भी कुल या गण विशेष का स्वामित्व नहीं माना जाता था. २–सचित्तादि परिहार का अर्थ यह है कि जिस क्षेत्र में सचित्त-दीक्षा लेने वाला मनुष्य और अचित्त-वस्त्र पात्र आदि जो द्रव्य उत्पन्न होते उसका स्वामी क्षेत्र स्वामी होता था. अन्य स्वामि के क्षेत्र में आने वाला कोई भी अन्य साधु वहां उत्पन्न होने वाले सचित्तादि द्रव्यों का अधिकारी नहीं होता था. जिसके उपदेश से जो मनुष्य सम्यक्त्व (जैन दर्शन) प्राप्त करता, वह यदि तीन वर्ष के भीतर साधु होना चाहता तो अपने प्राथमिकोपदेशक गुरु का ही शिष्य हो सकता था. इसी प्रकार कोई साधु उत्प्रवजित हो गृहस्थाश्रम में जाकर फिर तीन वर्ष के अन्दर साधु होना चाहता तो अपने पहले गुरु के पास ही दीक्षा ले सकता था, परन्तु तीन वर्ष के बाद उपर्युक्त दोनों प्रकार के पुरुषों के ऊपर से मूल गुरुओं का अधिकार रद्द हो जाता था, और वह अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिसके पास दीक्षा ग्रहण कर सकता था. ३-गणान्तरोपसंपदा-का अर्थ है दूसरे गण का स्वीकार. सामान्यतया एक गण का साधु दूसरे गण में जा नहीं सकता था, पर यदि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र की विशेष आराधना के लिये अथवा तपस्या तथा वैयावृत्त्य करने के निमित्त अन्यगण में जाना चाहता तो पहले अपने गण के आचार्य की आज्ञा प्राप्त करता और फिर अभिप्रेत गण के आचार्य के पास जाकर अपने को गण में लेने के लिए उनसे प्रार्थना करता.
आगन्तुक साधु की प्रार्थना सुनने के बाद गण-स्थविर इस बात की जांच करते कि आगन्तुक श्रमण वास्तव में अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके आया है या नहीं और जिस कारण से वह अपना आगमन बताता है वह कारण भी वास्तविक है या नहीं ? यदि इन बातों की परीक्षा से गणस्थविर को संतोष मिल जाता तो वे आगन्तुक साधु को उपसंपदा देकर अपने गण में दाखिल कर लेते थे.
S
Jain E
dasary.org