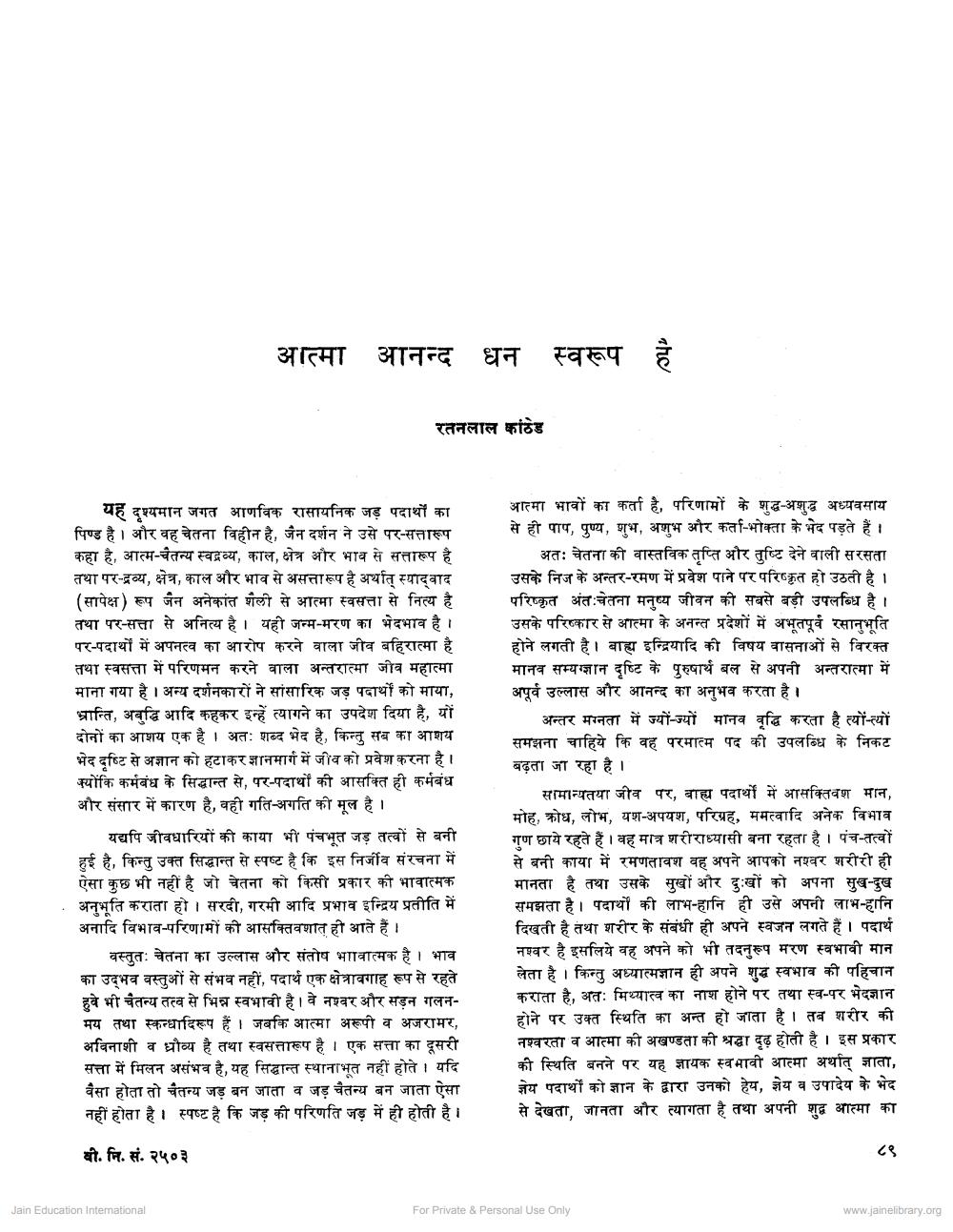________________
आत्मा आनन्द धन स्वरूप है
रतनलाल कांठेड
यह दृश्यमान जगत आणविक रासायनिक जड़ पदार्थों का पिण्ड है। और वह चेतना विहीन है, जैन दर्शन ने उसे पर-सत्तारूप कहा है, आत्म-चैतन्य स्वद्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव से सत्तारूप है तथा पर-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से असत्तारूप है अर्थात् स्याद्वाद (सापेक्ष) रूप जैन अनेकांत शैली से आत्मा स्वसत्ता से नित्य है तथा पर-सत्ता से अनित्य है। यही जन्म-मरण का भेदभाव है। पर-पदार्थों में अपनत्व का आरोप करने वाला जीव बहिरात्मा है तथा स्वसत्ता में परिणमन करने वाला अन्तरात्मा जीव महात्मा माना गया है। अन्य दर्शनकारों ने सांसारिक जड़ पदार्थों को माया, भ्रान्ति, अबुद्धि आदि कहकर इन्हें त्यागने का उपदेश दिया है, यों दोनों का आशय एक है । अतः शब्द भेद है, किन्तु सब का आशय भेद दृष्टि से अज्ञान को हटाकर ज्ञानमार्ग में जीव को प्रवेश करना है। क्योंकि कर्मबंध के सिद्धान्त से, पर-पदार्थों की आसक्ति ही कर्मबंध और संसार में कारण है, वही गति-अगति की मूल है।
यद्यपि जीवधारियों की काया भी पंचभूत जड़ तत्वों से बनी हुई है, किन्तु उक्त सिद्धान्त से स्पष्ट है कि इस निर्जीव संरचना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेतना को किसी प्रकार की भावात्मक अनुभूति कराता हो। सरदी, गरमी आदि प्रभाव इन्द्रिय प्रतीति में अनादि विभाव-परिणामों की आसक्तिवशात ही आते हैं।
वस्तुतः चेतना का उल्लास और संतोष भावात्मक है। भाव का उद्भव वस्तुओं से संभव नहीं, पदार्थ एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हुवे भी चैतन्य तत्व से भिन्न स्वभावी है। वे नश्वर और सड़न गलनमय तथा स्कन्धादिरूप हैं। जबकि आत्मा अरूपी व अजरामर, अविनाशी व ध्रौव्य है तथा स्वसत्तारूप है । एक सत्ता का दूसरी सत्ता में मिलन असंभव है, यह सिद्धान्त स्थानाभूत नहीं होते। यदि वैसा होता तो चैतन्य जड़ बन जाता व जड़ चैतन्य बन जाता ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट है कि जड़ की परिणति जड़ में ही होती है।
आत्मा भावों का कर्ता है, परिणामों के शुद्ध-अशुद्ध अध्यवसाय से ही पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ और कर्ता-भोक्ता के भेद पड़ते हैं। ___ अतः चेतना की वास्तविक तृप्ति और तुष्टि देने वाली सरसता उसके निज के अन्तर-रमण में प्रवेश पाने पर परिष्कृत हो उठती है । परिष्कृत अंतःचेतना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके परिकार से आत्मा के अनन्त प्रदेशों में अभूतपूर्व रसानुभूति होने लगती है। बाह्य इन्द्रियादि की विषय वासनाओं से विरक्त मानव सम्यग्ज्ञान दृष्टि के पुरुषार्थ बल से अपनी अन्तरात्मा में अपूर्व उल्लास और आनन्द का अनुभव करता है। ___अन्तर मग्नता में ज्यों-ज्यों मानव वृद्धि करता है त्यों-त्यों समझना चाहिये कि वह परमात्म पद की उपलब्धि के निकट बढ़ता जा रहा है।
सामान्यतया जीव पर, बाह्य पदार्थों में आसक्तिवश मान, मोह, क्रोध, लोभ, यश-अपयश, परिग्रह, ममत्वादि अनेक विभाव गुण छाये रहते हैं । वह मात्र शरीराध्यासी बना रहता है । पंच-तत्वों से बनी काया में रमणतावश वह अपने आपको नश्वर शरीरी ही मानता है तथा उसके सुखों और दुःखों को अपना सुख-दुख समझता है। पदार्थों की लाभ-हानि ही उसे अपनी लाभ-हानि दिखती है तथा शरीर के संबंधी ही अपने स्वजन लगते हैं। पदार्थ नश्वर है इसलिये वह अपने को भी तदनुरूप मरण स्वभावी मान लेता है । किन्तु अध्यात्मज्ञान ही अपने शुद्ध स्वभाव की पहिचान कराता है, अतः मिथ्यात्व का नाश होने पर तथा स्व-पर भेदज्ञान होने पर उक्त स्थिति का अन्त हो जाता है। तब शरीर की नश्वरता व आत्मा की अखण्डता की श्रद्धा दृढ़ होती है। इस प्रकार की स्थिति बनने पर यह ज्ञायक स्वभावी आत्मा अर्थात् ज्ञाता, ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान के द्वारा उनको हेय, ज्ञेय व उपादेय के भेद से देखता, जानता और त्यागता है तथा अपनी शुद्ध आत्मा का
बी.नि. सं. २५०३
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org