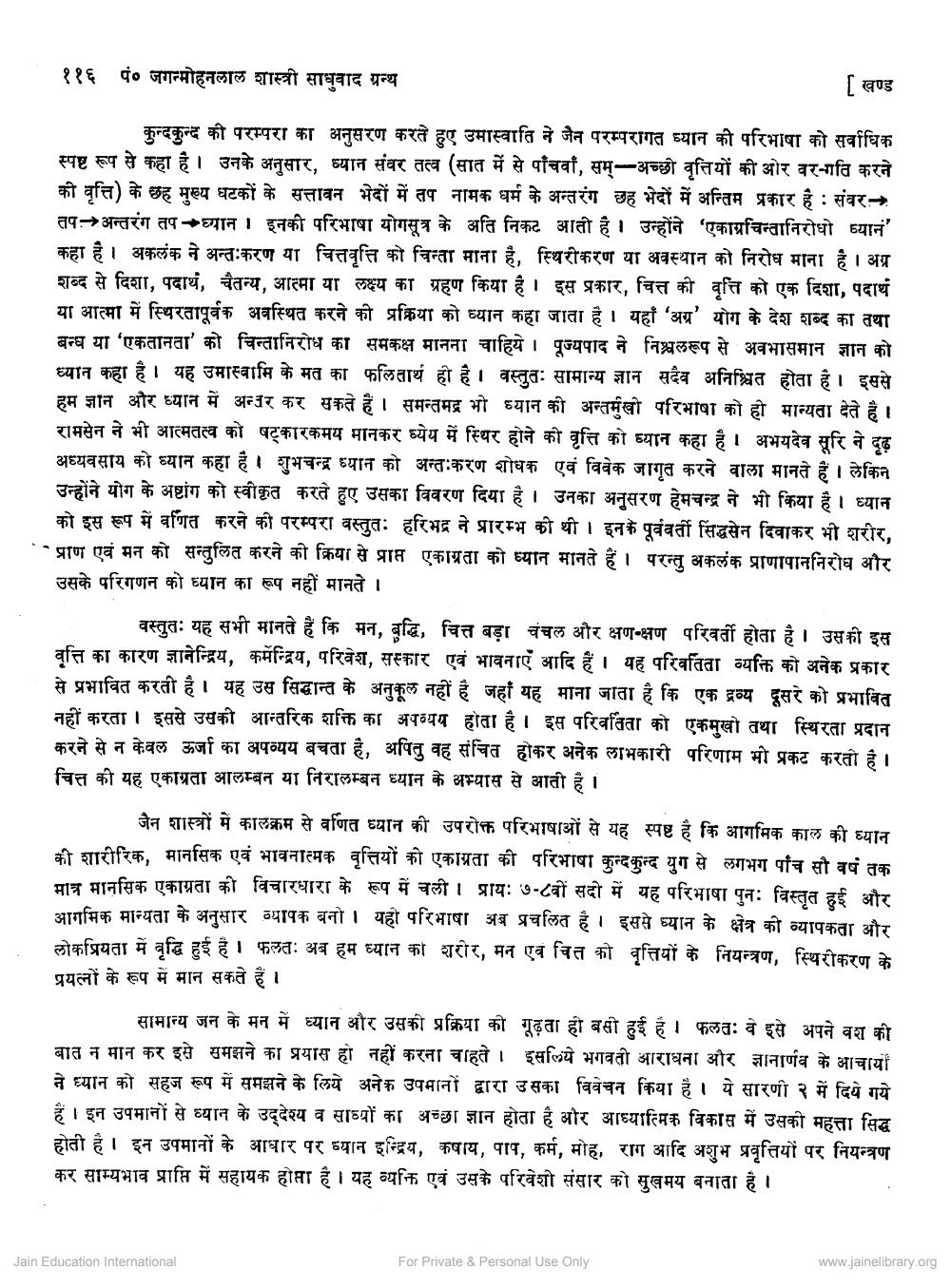________________
११६
पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य
[ खण्ड
कुन्दकुन्द की परम्परा का स्पष्ट रूप से कहा है । उनके अनुसार,
,
अनुसरण करते हुए उमास्वाति ने जैन परम्परागत ध्यान की परिभाषा को सर्वाधिक ध्यान संवर तत्व (सात में से पाँचवीं, सम्-अच्छी वृत्तियों की ओर वर गति करने की वृत्ति) के छह मुख्य घटकों के सत्तावन भेदों में तप नामक धर्म के अन्तरंग छह भेदों में अन्तिम प्रकार है : संवर तप अन्तरंग तप ध्यान इनकी परिभाषा योगसूत्र के अति निकट आती है। उन्होंने 'एकाग्रचिन्वानिरोधो ध्यानं' कहा है। अकलंक ने अन्तःकरण या चित्तवृत्ति को विन्ता माना है, स्थिरीकरण या अवस्थान को निरोध माना है। अप्र शब्द से दिशा, पदार्थ, चैतन्य, आत्मा या लक्ष्य का ग्रहण किया है। इस प्रकार, चित्त की वृत्ति को एक दिशा, पदार्थ या आत्मा में स्थिरतापूर्वक अवस्थित करने की प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है। यहाँ 'अग्र' योग के देश शब्द का तथा बन्ध या 'एकतानता' को चिन्तानिरोध का समकक्ष मानना चाहिये । पूज्यपाद ने निश्चलरूप से अवभासमान ज्ञान को ध्यान कहा है । यह उमास्वामि के मत का फलितार्थ ही है । वस्तुतः सामान्य ज्ञान सदैव अनिश्चित होता है। इससे हम ज्ञान और ध्यान में अडर कर सकते है। समन्तभद्र भी ध्यान की अन्तर्मुखो परिभाषा को ही मान्यता देते हैं। रामसेन ने भी आत्मतत्व को षट्कारकमय मानकर ध्येय में स्थिर होने की वृत्ति को ध्यान कहा है । अभयदेव सूरि ने दृढ़ अध्यवसाय को ध्यान कहा है। शुभचन्द्र ध्यान को अन्तःकरण शोधक एवं विवेक जागृत करने वाला मानते हैं लेकिन उन्होंने योग के अष्टांग को स्वीकृत करते हुए उसका विवरण दिया है। उनका अनुसरण हेमचन्द्र ने भी किया है। ध्यान को इस रूप में वर्णित करने की परम्परा वस्तुतः हरिभद्र ने प्रारम्भ की थी। इनके पूर्ववर्ती सिद्धसेन दिवाकर भी शरीर, प्राण एवं मन को सन्तुलित करने की क्रिया से प्राप्त एकाग्रता को ध्यान मानते हैं। परन्तु अकलंक प्राणापाननिरोध और उसके परिगणन को ध्यान का रूप नहीं मानते ।
।
वस्तुतः यह सभी मानते हैं कि मन, बुद्धि, पित्त बड़ा चंचल और क्षण-क्षण परिवर्ती होता है। उसकी इस वृत्ति का कारण ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, परिवेश, सस्कार एवं भावनाएं आदि हैं। यह परिवर्तिता व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। यह उस सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है जहाँ यह माना जाता है कि एक द्रव्य दूसरे को प्रभावित एकमुखो तथा स्थिरता प्रदान परिणाम भी प्रकट करती है।
नहीं करता। इससे उसकी आन्तरिक शक्ति का अपव्यय होता है। इस परिवर्तिता को करने से न केवल ऊर्जा का अपव्यय बचता है, अपितु वह संचित होकर अनेक लाभकारी चित्त की यह एकाग्रता आलम्बन या निरालम्बन ध्यान के अभ्यास से आती है ।
जैन शास्त्रों में कालक्रम से वर्णित ध्यान की उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आगमिक काल की ध्यान की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक वृत्तियों को एकाग्रता की परिभाषा कुन्दकुन्द युग से लगभग पाँच सौ वर्ष तक मात्र मानसिक एकाग्रता की विचारधारा के रूप में चली । प्रायः ७-८वीं सदी में यह परिभाषा पुनः विस्तृत हुई और आगमिक मान्यता के अनुसार व्यापक बनो। यो परिभाषा अब प्रचलित है। इससे ध्यान के क्षेत्र को व्यापकता और लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। फलतः अब हम ध्यान का शरीर, मन एवं वित्तको वृत्तियों के नियन्त्रण, स्थिरीकरण के प्रयत्नों के रूप में मान सकते हैं ।
सामान्य जन के मन में ध्यान और उसकी प्रक्रिया को नहीं करना चाहते।
गूढ़ता ही बसी हुई है । फलतः वे इसे अपने वश की बात न मान कर इसे समझने का प्रयास हो इसलिये भगवती आराधना और ज्ञानार्णव के आचार्यां ने ध्यान को सहज रूप में समझने के लिये अनेक उपमानों द्वारा उसका विवेचन किया है । ये सारणी २ में दिये गये हैं। इन उपमानों से ध्यान के उद्देश्य व साध्यों का अच्छा ज्ञान होता है और आध्यात्मिक विकास में उसकी महत्ता सिद्ध होती है । इन उपमानों के आधार पर ध्यान इन्द्रिय, कषाय, पाप, कर्म, मोह, राग आदि अशुभ प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण कर साम्यभाव प्राप्ति में सहायक होता है । यह व्यक्ति एवं उसके परिवेशी संसार को सुखमय बनाता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org