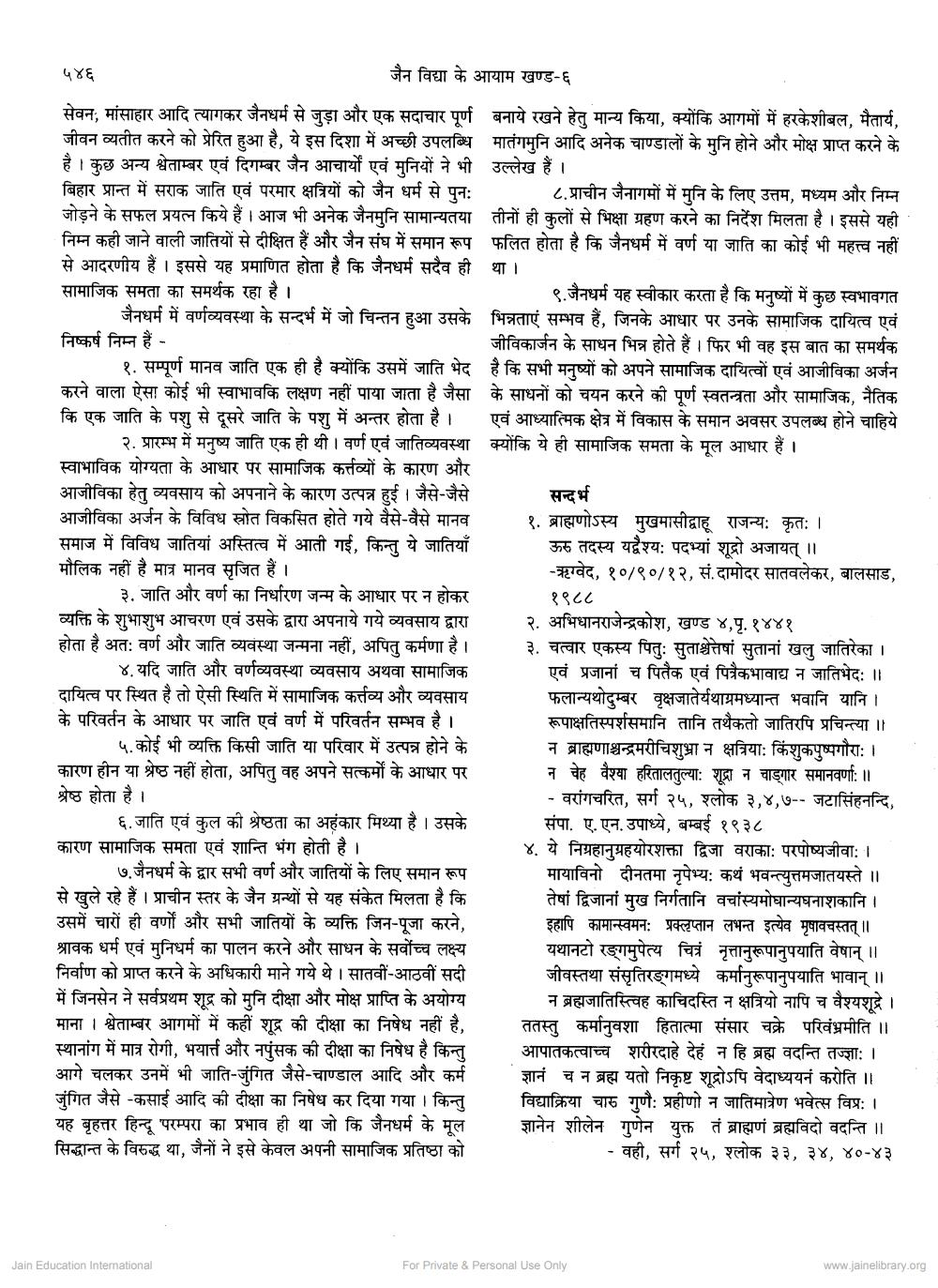________________
५४६
1
सेवन, मांसाहार आदि त्यागकर जैनधर्म से जुड़ा और एक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने को प्रेरित हुआ है, ये इस दिशा में अच्छी उपलब्धि है कुछ अन्य श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जैन आचार्यों एवं मुनियों ने भी बिहार प्रान्त में सराक जाति एवं परमार क्षत्रियों को जैन धर्म से पुनः जोड़ने के सफल प्रयत्न किये हैं। आज भी अनेक जैनमुनि सामान्यतया निम्न कही जाने वाली जातियों से दीक्षित हैं और जैन संघ में समान रूप से आदरणीय हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैनधर्म सदैव ही सामाजिक समता का समर्थक रहा है।
जैन विद्या के आयाम खण्ड ६
१. सम्पूर्ण मानव जाति एक ही है क्योंकि उसमें जाति भेद करने वाला ऐसा कोई भी स्वाभावकि लक्षण नहीं पाया जाता है जैसा कि एक जाति के पशु से दूसरे जाति के पशु में अन्तर होता है।
२. प्रारम्भ में मनुष्य जाति एक ही थी। वर्ण एवं जातिव्यवस्था स्वाभाविक योग्यता के आधार पर सामाजिक कर्त्तव्यों के कारण और आजीविका हेतु व्यवसाय को अपनाने के कारण उत्पन्न हुई। जैसे-जैसे आजीविका अर्जन के विविध स्रोत विकसित होते गये वैसे-वैसे मानव समाज में विविध जातियां अस्तित्व में आती गई, किन्तु ये जातियाँ मौलिक नहीं है मात्र मानव सृजित हैं।
३. जाति और वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर व्यक्ति के शुभाशुभ आचरण एवं उसके द्वारा अपनाये गये व्यवसाय द्वारा होता है अत: वर्ण और जाति व्यवस्था जन्मना नहीं, अपितु कर्मणा है । ४ यदि जाति और वर्णव्यवस्था व्यवसाय अथवा सामाजिक दायित्व पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक कर्तव्य और व्यवसाय के परिवर्तन के आधार पर जाति एवं वर्ण में परिवर्तन सम्भव है।
९. जैनधर्म यह स्वीकार करता है कि मनुष्यों में कुछ स्वभावगत जैनधर्म में वर्णव्यवस्था के सन्दर्भ में जो चिन्तन हुआ उसके भिन्नताएं सम्भव हैं, जिनके आधार पर उनके सामाजिक दायित्व एवं निष्कर्ष निम्न है - जीविकार्जन के साधन भिन्न होते है फिर भी वह इस बात का समर्थक है कि सभी मनुष्यों को अपने सामाजिक दायित्वों एवं आजीविका अर्जन के साधनों को चयन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिये क्योंकि ये ही सामाजिक समता के मूल आधार हैं।
५. कोई भी व्यक्ति किसी जाति या परिवार में उत्पन्न होने के कारण होन या श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु वह अपने सत्कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ होता है ।
६. जाति एवं कुल की श्रेष्ठता का अहंकार मिथ्या है। उसके कारण सामाजिक समता एवं शान्ति भंग होती है।
७. जैनधर्म के द्वार सभी वर्ण और जातियों के लिए समान रूप से खुले रहे हैं। प्राचीन स्तर के जैन ग्रन्थों से यह संकेत मिलता है कि उसमें चारों ही वर्णों और सभी जातियों के व्यक्ति जिन-पूजा करने,
श्रावक धर्म एवं मुनिधर्म का पालन करने और साधन के सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करने के अधिकारी माने गये थे। सातवीं-आठवीं सदी में जिनसेन ने सर्वप्रथम शूद्र को मुनि दीक्षा और मोक्ष प्राप्ति के अयोग्य माना । श्वेताम्बर आगमों में कहीं शूद्र की दीक्षा का निषेध नहीं है, स्थानांग में मात्र रोगी, भयार्त और नपुंसक की दीक्षा का निषेध है किन्तु आगे चलकर उनमें भी जाति- जुंगित जैसे - चाण्डाल आदि और कर्म जुंगित जैसे - कसाई आदि की दीक्षा का निषेध कर दिया गया । किन्तु यह बृहत्तर हिन्दू परम्परा का प्रभाव ही या जो कि जैनधर्म के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध था, जैनों ने इसे केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को
Jain Education International
बनाये रखने हेतु मान्य किया, क्योंकि आगमों में हरकेशीबल, मैतार्य, मातंगमुनि आदि अनेक चाण्डालों के मुनि होने और मोक्ष प्राप्त करने के उल्लेख हैं ।
८. प्राचीन जैनागमों में मुनि के लिए उत्तम, मध्यम और निम्न तीनों ही कुलों से भिक्षा ग्रहण करने का निर्देश मिलता है। इससे यही फलित होता है कि जैनधर्म में वर्ण या जाति का कोई भी महत्त्व नहीं था ।
सन्दर्भ
१. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत् ॥
- ऋग्वेद, १०/९०/१२. सं. दामोदर सातवलेकर, बालसाड, १९८८
२. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, पृ. १४४१
३. चत्वार एकस्य पितुः सुताश्चेत्तेषां सुतानां खलु जातिरेका । एवं प्रजानां च पितैक एवं पित्रैकभावाद्य न जातिभेदः ॥ फलान्यथोदुम्बर वृक्षजातेर्यथाग्रमध्यान्त भवानि यानि । रूपाक्षतिस्पर्शसमानि तानि तथैकतो जातिरपि प्रचिन्त्या ॥ न ब्राह्मणाचन्द्रमरीचिशुभ्रा न क्षत्रियाः किंशुकपुष्पगौराः । न चेह वैश्वा हरितालतुल्याः शूद्रा न चाहतार समानवर्णाः ॥ - वरांगचरित, सर्ग २५ श्लोक ३, ४, ७ जटासिंहनन्दि संपा. ए. एन. उपाध्ये, बम्बई १९३८
४. ये निग्रहानुग्रहयोरशक्ता द्विजा वराकाः परपोष्यजीवाः । मायाविनो दीनतमा नृपेभ्यः कथं भवन्त्युत्तमजातयस्ते ॥ तेषां द्विजानां मुख निर्गतानि वचांस्यमोघान्यघनाशकानि । इहापि कामान्स्वमनः प्रक्लृप्तान लभन्त इत्येव मृषावचस्तत् ॥ यथानटोरागमुपेत्य चित्रं नृत्तानुरूपानुपयाति वेषान् ॥ जीवस्तथा संसृतिरङ्गमध्ये कर्मानुरूपानुपयाति भावान् ॥ न ब्रह्मजातिस्त्विह काचिदस्ति न क्षत्रियो नापि च वैश्यशूद्रे । ततस्तु कर्मानुवशा हितात्मा संसार चक्रे परिवंभ्रमीति ।। आपातकत्वाच्च शरीरदाहे देहं न हि ब्रह्म वदन्ति तज्ज्ञाः । ज्ञानं च न ब्रह्म यतो निकृष्ट शूद्रोऽपि वेदाध्ययनं करोति ।। विद्याक्रिया चारू गुणैः प्रहीणो न जातिमात्रेण भवेत्स विप्रः । ज्ञानेन शीलेन गुणेन युक्त तं ब्राह्मणं ब्रह्मविदो वदन्ति ॥ यही सर्ग २५ श्लोक ३३, ३४, ४०-४३
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.