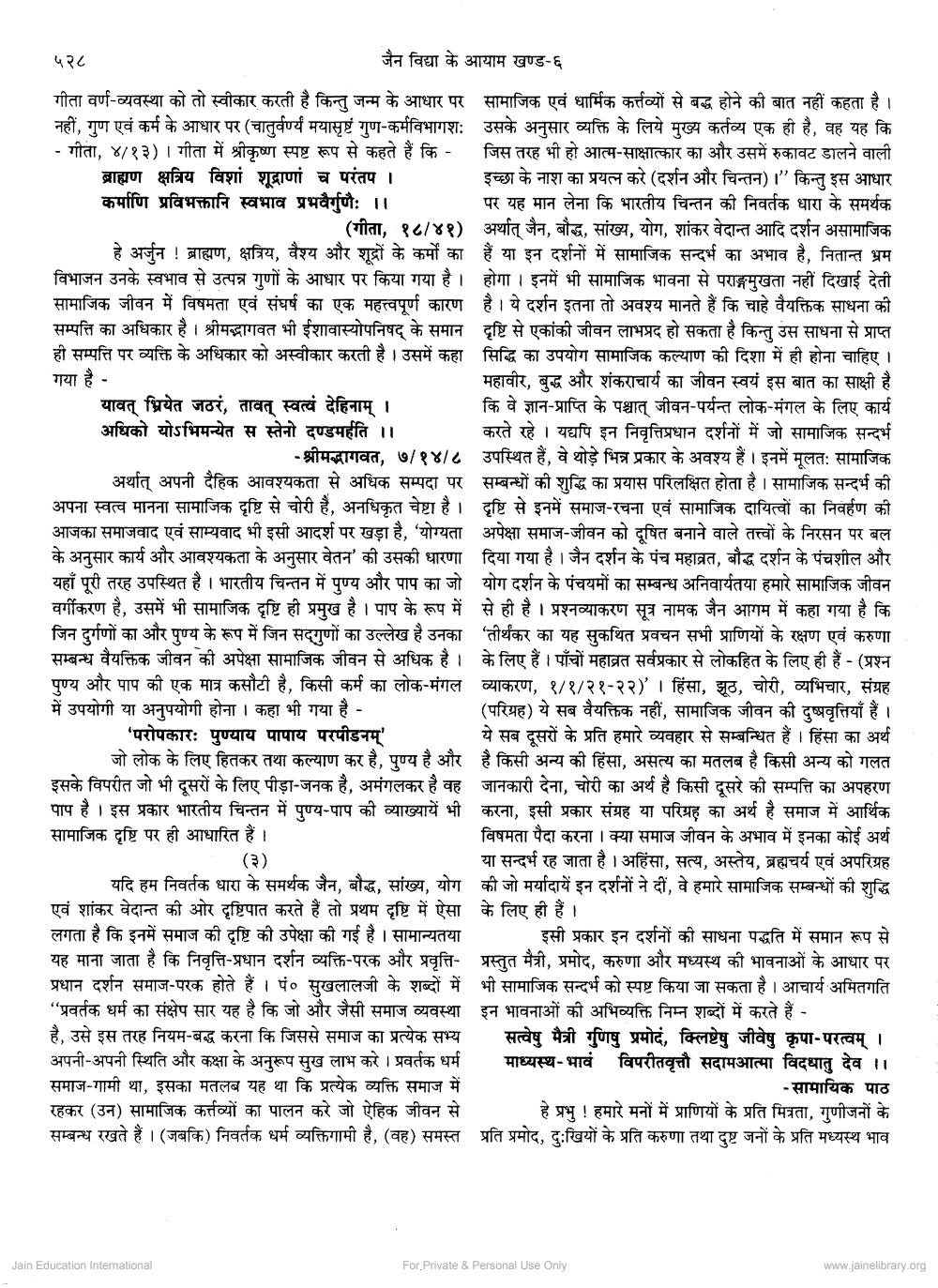________________
५२८
जैन विद्या के आयाम खण्ड-६
गीता वर्ण-व्यवस्था को तो स्वीकार करती है किन्तु जन्म के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों से बद्ध होने की बात नहीं कहता है । नहीं, गुण एवं कर्म के आधार पर (चातुर्वयं मयासष्टं गुण-कर्मविभागशः उसके अनुसार व्यक्ति के लिये मुख्य कर्तव्य एक ही है, वह यह कि - गीता, ४/१३) । गीता में श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि - जिस तरह भी हो आत्म-साक्षात्कार का और उसमें रुकावट डालने वाली
ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परंतप । इच्छा के नाश का प्रयत्न करे (दर्शन और चिन्तन)।" किन्तु इस आधार कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः ।।
पर यह मान लेना कि भारतीय चिन्तन की निवर्तक धारा के समर्थक
(गीता, १८/४१) अर्थात् जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, शांकर वेदान्त आदि दर्शन असामाजिक हे अर्जुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का हैं या इन दर्शनों में सामाजिक सन्दर्भ का अभाव है, नितान्त भ्रम विभाजन उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर किया गया है। होगा । इनमें भी सामाजिक भावना से पराङ्गमुखता नहीं दिखाई देती सामाजिक जीवन में विषमता एवं संघर्ष का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। ये दर्शन इतना तो अवश्य मानते हैं कि चाहे वैयक्तिक साधना की सम्पत्ति का अधिकार है । श्रीमद्भागवत भी ईशावास्योपनिषद् के समान दृष्टि से एकांकी जीवन लाभप्रद हो सकता है किन्तु उस साधना से प्राप्त ही सम्पत्ति पर व्यक्ति के अधिकार को अस्वीकार करती है। उसमें कहा सिद्धि का उपयोग सामाजिक कल्याण की दिशा में ही होना चाहिए। गया है -
महावीर, बुद्ध और शंकराचार्य का जीवन स्वयं इस बात का साक्षी है यावत् भ्रियेत जठरं, तावत् स्वत्वं देहिनाम् । कि वे ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् जीवन-पर्यन्त लोक-मंगल के लिए कार्य अधिको योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ।। करते रहे । यद्यपि इन निवृत्तिप्रधान दर्शनों में जो सामाजिक सन्दर्भ
-श्रीमद्भागवत, ७/१४/८ उपस्थित हैं, वे थोड़े भिन्न प्रकार के अवश्य हैं। इनमें मूलत: सामाजिक अर्थात् अपनी दैहिक आवश्यकता से अधिक सम्पदा पर सम्बन्धों की शुद्धि का प्रयास परिलक्षित होता है । सामाजिक सन्दर्भ की अपना स्वत्व मानना सामाजिक दृष्टि से चोरी है, अनधिकृत चेष्टा है। दृष्टि से इनमें समाज-रचना एवं सामाजिक दायित्वों का निवर्हण की आजका समाजवाद एवं साम्यवाद भी इसी आदर्श पर खड़ा है, 'योग्यता अपेक्षा समाज-जीवन को दूषित बनाने वाले तत्त्वों के निरसन पर बल के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन' की उसकी धारणा दिया गया है । जैन दर्शन के पंच महाव्रत, बौद्ध दर्शन के पंचशील और यहाँ पूरी तरह उपस्थित है । भारतीय चिन्तन में पुण्य और पाप का जो योग दर्शन के पंचयमों का सम्बन्ध अनिवार्यतया हमारे सामाजिक जीवन वर्गीकरण है, उसमें भी सामाजिक दृष्टि ही प्रमुख है । पाप के रूप में से ही है । प्रश्नव्याकरण सूत्र नामक जैन आगम में कहा गया है कि जिन दुर्गणों का और पुण्य के रूप में जिन सद्गुणों का उल्लेख है उनका 'तीर्थंकर का यह सुकथित प्रवचन सभी प्राणियों के रक्षण एवं करुणा सम्बन्ध वैयक्तिक जीवन की अपेक्षा सामाजिक जीवन से अधिक है। के लिए हैं । पाँचों महाव्रत सर्वप्रकार से लोकहित के लिए ही हैं - (प्रश्न पुण्य और पाप की एक मात्र कसौटी है, किसी कर्म का लोक-मंगल व्याकरण, १/१/२१-२२) । हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, संग्रह में उपयोगी या अनुपयोगी होना । कहा भी गया है -
(परिग्रह) ये सब वैयक्तिक नहीं, सामाजिक जीवन की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्'
ये सब दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से सम्बन्धित हैं । हिंसा का अर्थ ___ जो लोक के लिए हितकर तथा कल्याण कर है, पुण्य है और है किसी अन्य की हिंसा, असत्य का मतलब है किसी अन्य को गलत इसके विपरीत जो भी दूसरों के लिए पीड़ा-जनक है, अमंगलकर है वह जानकारी देना, चोरी का अर्थ है किसी दूसरे की सम्पत्ति का अपहरण पाप है । इस प्रकार भारतीय चिन्तन में पुण्य-पाप की व्याख्यायें भी करना, इसी प्रकार संग्रह या परिग्रह का अर्थ है समाज में आर्थिक सामाजिक दृष्टि पर ही आधारित हैं।
विषमता पैदा करना । क्या समाज जीवन के अभाव में इनका कोई अर्थ (३)
या सन्दर्भ रह जाता है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह यदि हम निवर्तक धारा के समर्थक जैन, बौद्ध, सांख्य, योग की जो मर्यादायें इन दर्शनों ने दीं, वे हमारे सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि एवं शांकर वेदान्त की ओर दृष्टिपात करते हैं तो प्रथम दृष्टि में ऐसा के लिए ही हैं। लगता है कि इनमें समाज की दृष्टि की उपेक्षा की गई है । सामान्यतया इसी प्रकार इन दर्शनों की साधना पद्धति में समान रूप से यह माना जाता है कि निवृत्ति-प्रधान दर्शन व्यक्ति-परक और प्रवृत्ति- प्रस्तुत मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ की भावनाओं के आधार पर प्रधान दर्शन समाज-परक होते हैं । पं० सुखलालजी के शब्दों में भी सामाजिक सन्दर्भ को स्पष्ट किया जा सकता है । आचार्य अमितगति "प्रवर्तक धर्म का संक्षेप सार यह है कि जो और जैसी समाज व्यवस्था इन भावनाओं की अभिव्यक्ति निम्न शब्दों में करते हैं - है, उसे इस तरह नियम-बद्ध करना कि जिससे समाज का प्रत्येक सभ्य सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा-परत्वम् । अपनी-अपनी स्थिति और कक्षा के अनुरूप सुख लाभ करे । प्रवर्तक धर्म माध्यस्थ-भावं विपरीतवृत्तौ सदामआत्मा विदधातु देव ।। समाज-गामी था, इसका मतलब यह था कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में
-सामायिक पाठ रहकर (उन) सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे जो ऐहिक जीवन से
हे प्रभु ! हमारे मनों में प्राणियों के प्रति मित्रता, गुणीजनों के सम्बन्ध रखते हैं । (जबकि) निवर्तक धर्म व्यक्तिगामी है, (वह) समस्त प्रति प्रमोद, दुःखियों के प्रति करुणा तथा दुष्ट जनों के प्रति मध्यस्थ भाव
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org