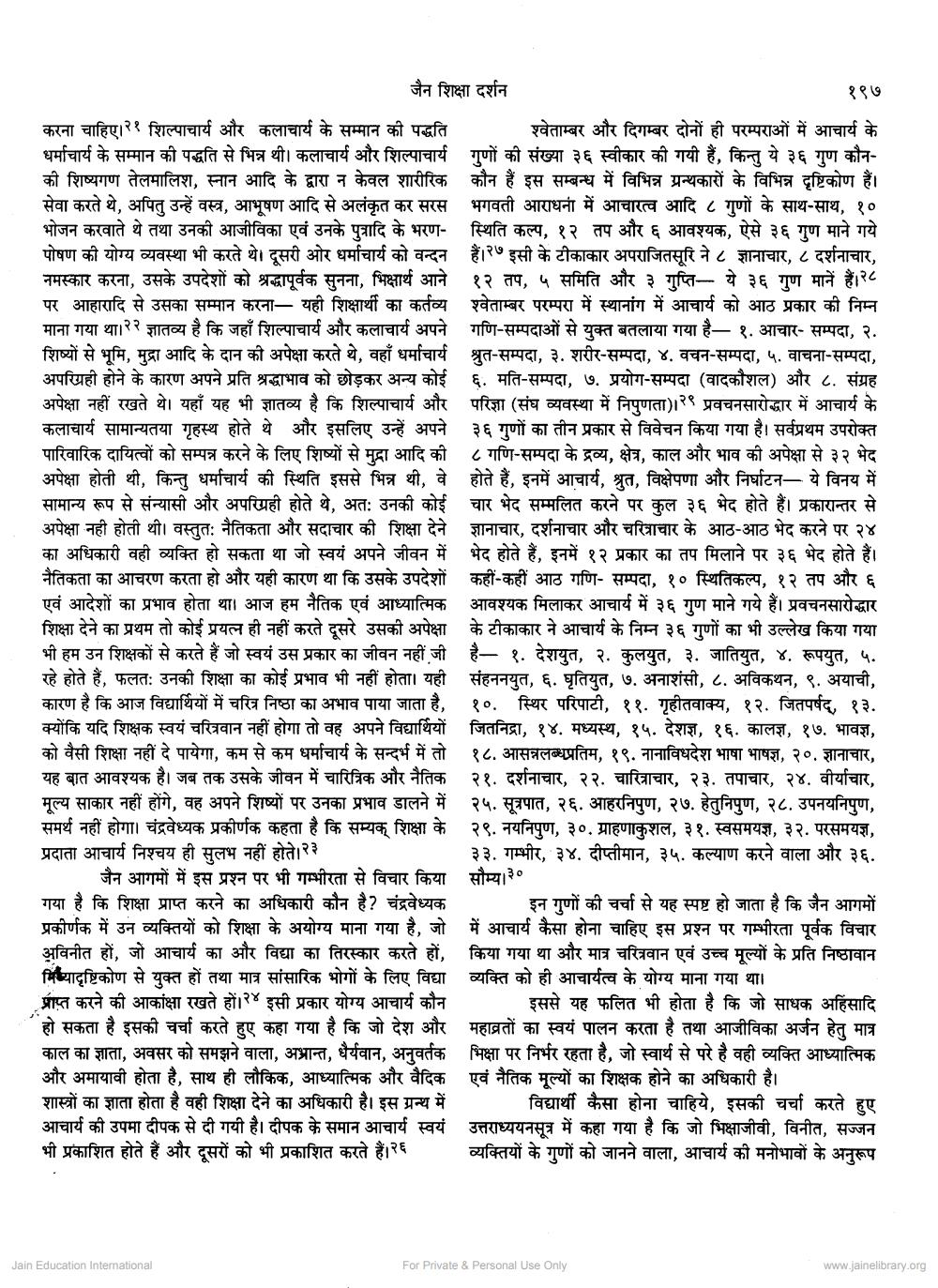________________
करना चाहिए । २१ शिल्पाचार्य और कलाचार्य के सम्मान की पद्धति धर्माचार्य के सम्मान की पद्धति से भिन्न थी। कलाचार्य और शिल्पाचार्य की शिष्यगण तेलमालिश, स्नान आदि के द्वारा न केवल शारीरिक सेवा करते थे, अपितु उन्हें वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत कर सरस भोजन करवाते थे तथा उनकी आजीविका एवं उनके पुत्रादि के भरणपोषण की योग्य व्यवस्था भी करते थे। दूसरी ओर धर्माचार्य को वन्दन नमस्कार करना, उसके उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुनना, भिक्षार्थ आने पर आहारादि से उसका सम्मान करना यही शिक्षार्थी का कर्तव्य माना गया था।२२ ज्ञातव्य है कि जहाँ शिल्पाचार्य और कलाचार्य अपने शिष्यों से भूमि, मुद्रा आदि के दान की अपेक्षा करते थे, वहाँ धर्माचार्य अपरिग्रही होने के कारण अपने प्रति श्रद्धाभाव को छोड़कर अन्य कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि शिल्पाचार्य और कलाचार्य सामान्यतया गृहस्थ होते थे और इसलिए उन्हें अपने पारिवारिक दायित्वों को सम्पन्न करने के लिए शिष्यों से मुद्रा आदि की अपेक्षा होती थी, किन्तु धर्माचार्य की स्थिति इससे भिन्न थी, वे सामान्य रूप से संन्यासी और अपरिग्रही होते थे, अतः उनकी कोई अपेक्षा नही होती थी। वस्तुतः नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देने का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता था जो स्वयं अपने जीवन में नैतिकता का आचरण करता हो और यही कारण था कि उसके उपदेशों एवं आदेशों का प्रभाव होता था। आज हम नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रथम तो कोई प्रयत्न ही नहीं करते दूसरे उसकी अपेक्षा भी हम उन शिक्षकों से करते हैं जो स्वयं उस प्रकार का जीवन नहीं जी रहे होते हैं, फलतः उनको शिक्षा का कोई प्रभाव भी नहीं होता। यही कारण है कि आज विद्यार्थियों में चरित्र निष्ठा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं चरित्रवान नहीं होगा तो वह अपने विद्यार्थियों को वैसी शिक्षा नहीं दे पायेगा, कम से कम धर्माचार्य के सन्दर्भ में तो यह बात आवश्यक है। जब तक उसके जीवन में चारित्रिक और नैतिक मूल्य साकार नहीं होंगे, वह अपने शिष्यों पर उनका प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होगा। चंद्रवेध्यक प्रकीर्णक कहता है कि सम्यक शिक्षा के प्रदाता आचार्य निश्चय ही सुलभ नहीं होते। २३
जैन आगमों में इस प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार किया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी कौन है ? चंद्रवेध्यक प्रकीर्णक में उन व्यक्तियों को शिक्षा के अयोग्य माना गया है, जो अविनीत हों, जो आचार्य का और विद्या का तिरस्कार करते हों मिध्यादृष्टिकोण से युक्त हों तथा मात्र सांसारिक भोगों के लिए विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हों। २४ इसी प्रकार योग्य आचार्य कौन हो सकता है इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि जो देश और काल का ज्ञाता, अवसर को समझने वाला, अभ्रान्त, धैर्यवान, अनुवर्तक और अमायावी होता है, साथ ही लौकिक, आध्यात्मिक और वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता होता है वही शिक्षा देने का अधिकारी है। इस ग्रन्थ में आचार्य की उपमा दीपक से दी गयी है। दीपक के समान आचार्य स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। २६
Jain Education International
जैन शिक्षा दर्शन
-
१९७
श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में आचार्य के गुणों की संख्या ३६ स्वीकार की गयी हैं, किन्तु ये ३६ गुण कौनकौन हैं इस सम्बन्ध में विभिन्न ग्रन्थकारों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। भगवती आराधना में आचारत्व आदि ८ गुणों के साथ-साथ, १० स्थिति कल्प, १२ तप और ६ आवश्यक ऐसे ३६ गुण माने गये हैं। २७ इसी के टीकाकार अपराजितसूरि ने ८ ज्ञानाचार, ८ दर्शनाचार, १२ तप, ५ समिति और ३ गुप्ति- ये ३६ गुण मानें हैं। २८ श्वेताम्बर परम्परा में स्थानांग में आचार्य को आठ प्रकार की निम्न गणि-सम्पदाओं से युक्त बतलाया गया है — १. आचार - सम्पदा, २. श्रुत-सम्पदा, ३. शरीर-सम्पदा, ४ वचन सम्पदा, ५. वाचना- सम्पदा, ६ मति सम्पदा, ७ प्रयोग सम्पदा (वादकौशल) और ८. संग्रह परिज्ञा (संघ व्यवस्था में निपुणता ) | २९ प्रवचनसारोद्धार में आचार्य के ३६ गुणों का तीन प्रकार से विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम उपरोक्त ८ गणि-सम्पदा के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से ३२ भेद होते हैं, इनमें आचार्य, श्रुत, विक्षेपणा और निर्धाटन — ये विनय में चार भेद सम्मलित करने पर कुल ३६ भेद होते हैं। प्रकारान्तर से ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चरित्राचार के आठ-आठ भेद करने पर २४ भेद होते हैं, इनमें १२ प्रकार का तप मिलाने पर ३६ भेद होते हैं। कहीं-कहीं आठ गणि- सम्पदा, १० स्थितिकल्प, १२ तप और ६ आवश्यक मिलाकर आचार्य में ३६ गुण माने गये हैं। प्रवचनसारोद्धार के टीकाकार ने आचार्य के निम्न ३६ गुणों का भी उल्लेख किया गया है- १. देशयुत, २. कुलयुत, ३ जातियुत, ४ रूपयुत, ५. संहननयुत, ६. घृतियुत, ७ अनाशंसी, ८. अविकथन, ९. अयाची, १०. स्थिर परिपाटी, ११. गृहीतवाक्य, १२. जितपर्षद्, १३. जितनिद्रा, १४ मध्यस्थ, १५. देशश, १६. कालश, १७. भावश १८. आसन्नलब्धप्रतिम, १९. नानाविधदेश भाषा भाषज्ञ, २०. ज्ञानाचार, २१. दर्शनाचार, २२. चारित्राचार, २३. तपाचार, २४ वीर्याचार, २५. सूत्रपात, २६. आहरनिपुण, २७. हेतुनिपुण, २८. उपनयनिपुण, २९. नयनिपुण, ३०. ग्राहणाकुशल, ३१. स्वसमयश, ३२. परसमयज्ञ, ३३. गम्भीर, ३४. दीप्तीमान, ३५. कल्याण करने वाला और ३६. सौम्य । ३०
इन गुणों की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन आगमों में आचार्य कैसा होना चाहिए इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया था और मात्र चरित्रवान एवं उच्च मूल्यों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति को ही आचार्यत्व के योग्य माना गया था।
इससे यह फलित भी होता है कि जो साधक अहिंसादि महाव्रतों का स्वयं पालन करता है तथा आजीविका अर्जन हेतु मात्र भिक्षा पर निर्भर रहता है, जो स्वार्थ से परे है वही व्यक्ति आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का शिक्षक होने का अधिकारी है।
विद्यार्थी कैसा होना चाहिये, इसकी चर्चा करते हुए उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जो भिक्षाजीवी, विनीत, सज्जन व्यक्तियों के गुणों को जानने वाला, आचार्य की मनोभावों के अनुरूप
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.