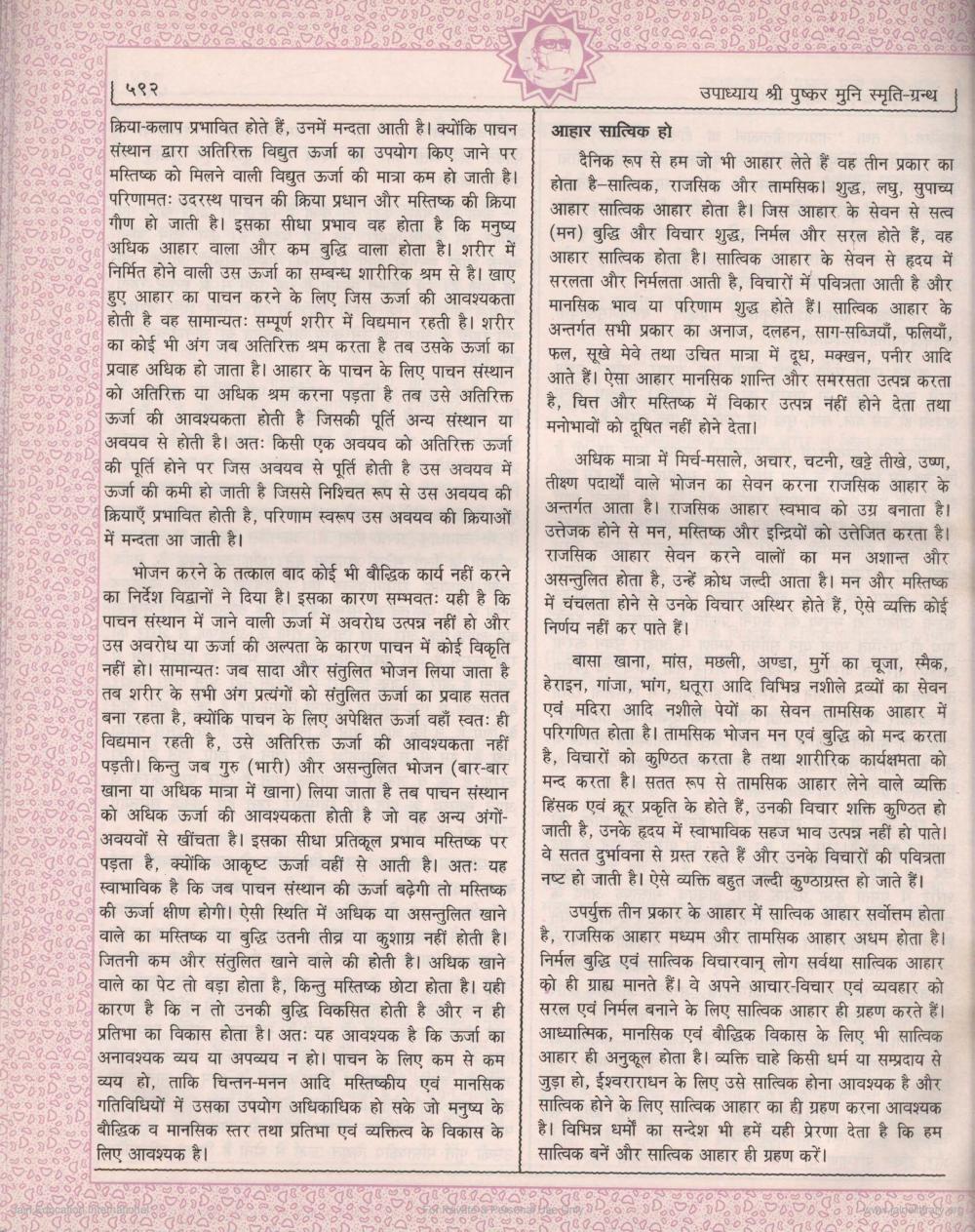________________
B
FOR
५९२
क्रिया-कलाप प्रभावित होते हैं, उनमें मन्दता आती है। क्योंकि पाचन संस्थान द्वारा अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा का उपयोग किए जाने पर मस्तिष्क को मिलने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। | परिणामतः उदरस्थ पाचन की क्रिया प्रधान और मस्तिष्क की क्रिया गीण हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि मनुष्य अधिक आहार वाला और कम बुद्धि वाला होता है शरीर में निर्मित होने वाली उस ऊर्जा का सम्बन्ध शारीरिक श्रम से है। खाए हुए आहार का पाचन करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह सामान्यतः सम्पूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है। शरीर का कोई भी अंग जब अतिरिक्त श्रम करता है तब उसके ऊर्जा का प्रवाह अधिक हो जाता है। आहार के पाचन के लिए पाचन संस्थान को अतिरिक्त या अधिक श्रम करना पड़ता है तब उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति अन्य संस्थान या अवयव से होती है। अतः किसी एक अवयव को अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति होने पर जिस अवयव से पूर्ति होती है उस अवयव में ऊर्जा की कमी हो जाती है जिससे निश्चित रूप से उस अवयव की क्रियाएँ प्रभावित होती है, परिणाम स्वरूप उस अवयव की क्रियाओं में मन्दता आ जाती है।
भोजन करने के तत्काल बाद कोई भी बौद्धिक कार्य नहीं करने का निर्देश विद्वानों ने दिया है। इसका कारण सम्भवतः यही है कि पाचन संस्थान में जाने वाली ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न नहीं हो और उस अवरोध या ऊर्जा की अल्पता के कारण पाचन में कोई विकृति नहीं हो सामान्यतः जब सादा और संतुलित भोजन लिया जाता है तब शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को संतुलित ऊर्जा का प्रवाह सतत बना रहता है, क्योंकि पाचन के लिए अपेक्षित ऊर्जा वहाँ स्वतः ही विद्यमान रहती है, उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु जब गुरु (भारी) और असन्तुलित भोजन (बार-बार खाना या अधिक मात्रा में खाना) लिया जाता है तब पाचन संस्थान को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो वह अन्य अंगोंअवयवों से खींचता है। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि आकृष्ट ऊर्जा वहीं से आती है। अतः यह स्वाभाविक है कि जब पाचन संस्थान की ऊर्जा बढ़ेगी तो मस्तिष्क की ऊर्जा क्षीण होगी। ऐसी स्थिति में अधिक या असन्तुलित खाने वाले का मस्तिष्क या बुद्धि उतनी तीव्र या कुशाग्र नहीं होती है। जितनी कम और संतुलित खाने वाले की होती है। अधिक खाने वाले का पेट तो बड़ा होता है, किन्तु मस्तिष्क छोटा होता है। यही कारण है कि न तो उनकी बुद्धि विकसित होती है और न ही प्रतिभा का विकास होता है। अतः यह आवश्यक है कि ऊर्जा का अनावश्यक व्यय या अपव्यय न हो। पाचन के लिए कम से कम व्यय हो, ताकि चिन्तन-मनन आदि मस्तिष्कीय एवं मानसिक गतिविधियों में उसका उपयोग अधिकाधिक हो सके जो मनुष्य के बौद्धिक व मानसिक स्तर तथा प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है।
பிஜியில்
8
SPE
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
आहार सात्विक हो
दैनिक रूप से हम जो भी आहार लेते हैं वह तीन प्रकार का होता है- सात्विक, राजसिक और तामसिक शुद्ध, लघु, सुपाच्य आहार सात्विक आहार होता है। जिस आहार के सेवन से सत्व (मन) बुद्धि और विचार शुद्ध, निर्मल और सरल होते हैं, वह आहार सात्विक होता है। सात्विक आहार के सेवन से हृदय में सरलता और निर्मलता आती है, विचारों में पवित्रता आती है और मानसिक भाव या परिणाम शुद्ध होते हैं। सात्विक आहार के अन्तर्गत सभी प्रकार का अनाज, दलहन, साग-सब्जियाँ, फलियाँ, फल, सूखे मेवे तथा उचित मात्रा में दूध, मक्खन, पनीर आदि आते हैं। ऐसा आहार मानसिक शान्ति और समरसता उत्पन्न करता है, चित्त और मस्तिष्क में विकार उत्पन्न नहीं होने देता तथा मनोभावों को दूषित नहीं होने देता।
अधिक मात्रा में मिर्च-मसाले, अचार, चटनी, खट्टे तीखे, उष्ण, तीक्ष्ण पदार्थों वाले भोजन का सेवन करना राजसिक आहार के अन्तर्गत आता है। राजसिक आहार स्वभाव को उग्र बनाता है। उत्तेजक होने से मन, मस्तिष्क और इन्द्रियों को उत्तेजित करता है। राजसिक आहार सेवन करने वालों का मन अशान्त और असन्तुलित होता है, उन्हें क्रोध जल्दी आता है। मन और मस्तिष्क में चंचलता होने से उनके विचार अस्थिर होते हैं, ऐसे व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं।
बासा खाना, मांस, मछली, अण्डा, मुर्गे का चूजा, स्मैक, हेराइन, गांजा, भांग, धतूरा आदि विभिन्न नशीले द्रव्यों का सेवन एवं मदिरा आदि नशीले पेयों का सेवन तामसिक आहार में परिगणित होता है। तामसिक भोजन मन एवं बुद्धि को मन्द करता है, विचारों को कुण्ठित करता है तथा शारीरिक कार्यक्षमता को मन्द करता है। सतत रूप से तामसिक आहार लेने वाले व्यक्ति हिंसक एवं क्रूर प्रकृति के होते हैं, उनकी विचार शक्ति कुण्ठित हो जाती है, उनके हृदय में स्वाभाविक सहज भाव उत्पन्न नहीं हो पाते। वे सतत दुर्भावना से ग्रस्त रहते हैं और उनके विचारों की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी कुण्ठाग्रस्त हो जाते हैं।
उपर्युक्त तीन प्रकार के आहार में सात्विक आहार सर्वोत्तम होता है, राजसिक आहार मध्यम और तामसिक आहार अधम होता है। निर्मल बुद्धि एवं सात्विक विचारवान् लोग सर्वथा सात्विक आहार को ही ग्राह्य मानते हैं वे अपने आचार-विचार एवं व्यवहार को सरल एवं निर्मल बनाने के लिए सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भी सात्विक आहार ही अनुकूल होता है। व्यक्ति चाहे किसी धर्म या सम्प्रदाय से जुड़ा हो, ईश्वराराधन के लिए उसे सात्विक होना आवश्यक है और सात्विक होने के लिए सात्विक आहार का ही ग्रहण करना आवश्यक है विभिन्न धर्मो का सन्देश भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम सात्विक बनें और सात्विक आहार ही ग्रहण करें।
70 AARO