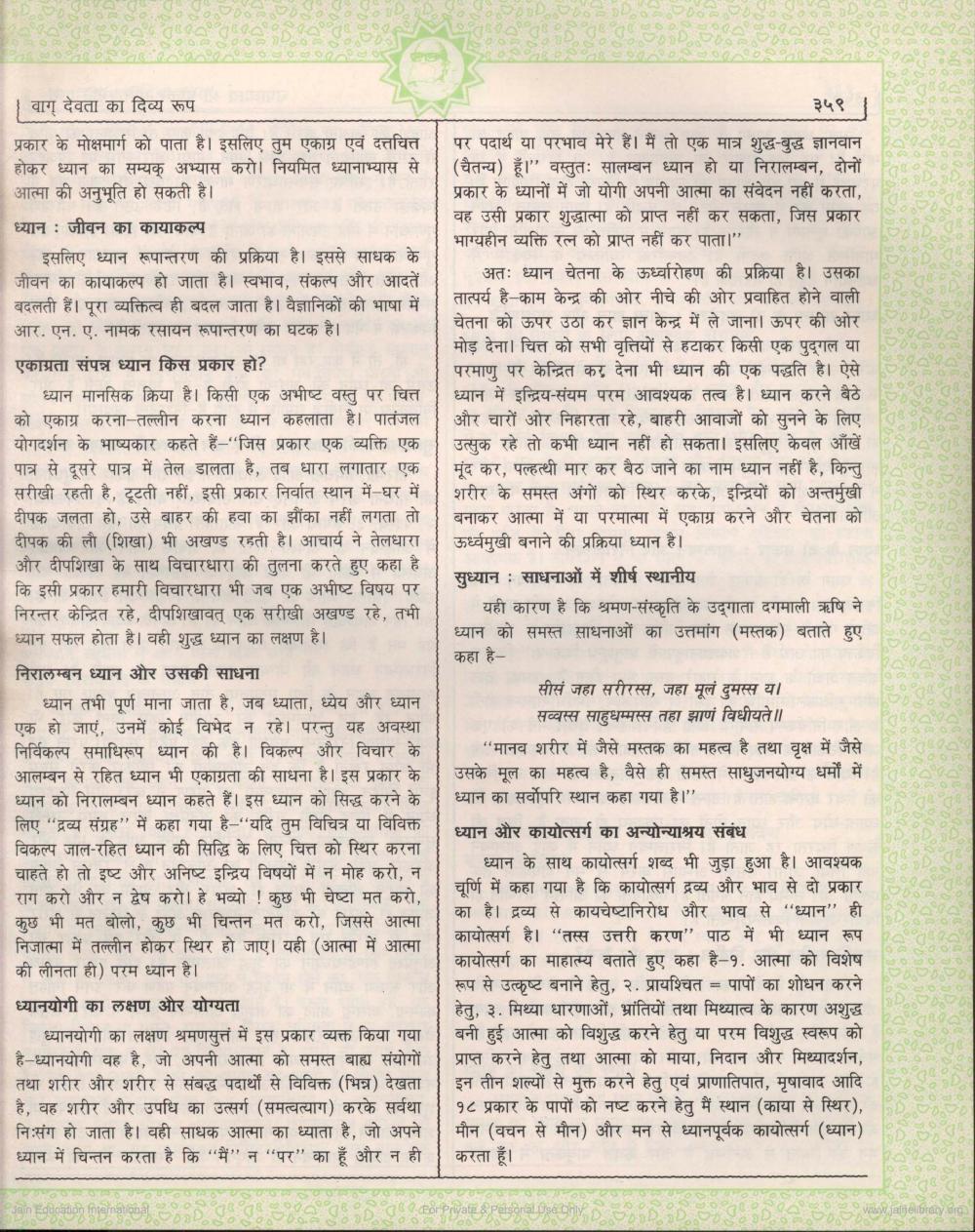________________
DOOODDE 200202000
वागू देवता का दिव्य रूप
३५९ ।
90.00.00 प्रकार के मोक्षमार्ग को पाता है। इसलिए तुम एकाग्र एवं दत्तचित्त । पर पदार्थ या परभाव मेरे हैं। मैं तो एक मात्र शुद्ध-बुद्ध ज्ञानवान होकर ध्यान का सम्यक् अभ्यास करो। नियमित ध्यानाभ्यास से । (चैतन्य) हूँ।" वस्तुतः सालम्बन ध्यान हो या निरालम्बन, दोनों आत्मा की अनुभूति हो सकती है।
प्रकार के ध्यानों में जो योगी अपनी आत्मा का संवेदन नहीं करता, ध्यान : जीवन का कायाकल्प
वह उसी प्रकार शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जिस प्रकार
भाग्यहीन व्यक्ति रत्न को प्राप्त नहीं कर पाता।" इसलिए ध्यान रूपान्तरण की प्रक्रिया है। इससे साधक के जीवन का कायाकल्प हो जाता है। स्वभाव, संकल्प और आदतें
अतः ध्यान चेतना के ऊर्ध्वारोहण की प्रक्रिया है। उसका बदलती हैं। पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। वैज्ञानिकों की भाषा में
तात्पर्य है-काम केन्द्र की ओर नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली आर. एन. ए. नामक रसायन रूपान्तरण का घटक है।
चेतना को ऊपर उठा कर ज्ञान केन्द्र में ले जाना। ऊपर की ओर
मोड़ देना। चित्त को सभी वृत्तियों से हटाकर किसी एक पुद्गल या एकाग्रता संपन्न ध्यान किस प्रकार हो?
परमाणु पर केन्द्रित कर देना भी ध्यान की एक पद्धति है। ऐसे ध्यान मानसिक क्रिया है। किसी एक अभीष्ट वस्तु पर चित्त ध्यान में इन्द्रिय-संयम परम आवश्यक तत्व है। ध्यान करने बैठे को एकाग्र करना-तल्लीन करना ध्यान कहलाता है। पातंजल और चारों ओर निहारता रहे, बाहरी आवाजों को सुनने के लिए योगदर्शन के भाष्यकार कहते हैं-"जिस प्रकार एक व्यक्ति एक उत्सुक रहे तो कभी ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए केवल आँखें पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालता है, तब धारा लगातार एक मूंद कर, पल्हत्थी मार कर बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है, किन्तु सरीखी रहती है, टूटती नहीं, इसी प्रकार निर्वात स्थान में घर में शरीर के समस्त अंगों को स्थिर करके, इन्द्रियों को अन्तर्मुखी दीपक जलता हो, उसे बाहर की हवा का झोंका नहीं लगता तो बनाकर आत्मा में या परमात्मा में एकाग्र करने और चेतना को दीपक की लौ (शिखा) भी अखण्ड रहती है। आचार्य ने तेलधारा । ऊर्ध्वमुखी बनाने की प्रक्रिया ध्यान है। और दीपशिखा के साथ विचारधारा की तुलना करते हुए कहा है
सुध्यान : साधनाओं में शीर्ष स्थानीय कि इसी प्रकार हमारी विचारधारा भी जब एक अभीष्ट विषय पर निरन्तर केन्द्रित रहे, दीपशिखावत् एक सरीखी अखण्ड रहे, तभी
यही कारण है कि श्रमण-संस्कृति के उद्गाता दगमाली ऋषि ने ध्यान सफल होता है। वही शुद्ध ध्यान का लक्षण है।
ध्यान को समस्त साधनाओं का उत्तमांग (मस्तक) बताते हुए
कहा हैनिरालम्बन ध्यान और उसकी साधना
सीसं जहा सरीरस्स, जहा मूलं दुमस्स य। ध्यान तभी पूर्ण माना जाता है, जब ध्याता, ध्येय और ध्यान एक हो जाएं, उनमें कोई विभेद न रहे। परन्तु यह अवस्था
सव्वस्स साहुधम्मस्स तहा झाणं विधीयते॥ निर्विकल्प समाधिरूप ध्यान की है। विकल्प और विचार के "मानव शरीर में जैसे मस्तक का महत्व है तथा वृक्ष में जैसे आलम्बन से रहित ध्यान भी एकाग्रता की साधना है। इस प्रकार के उसके मूल का महत्व है, वैसे ही समस्त साधुजनयोग्य धर्मों में ध्यान को निरालम्बन ध्यान कहते हैं। इस ध्यान को सिद्ध करने के । ध्यान का सर्वोपरि स्थान कहा गया है।" लिए "द्रव्य संग्रह" में कहा गया है-“यदि तुम विचित्र या विविक्त
| ध्यान और कायोत्सर्ग का अन्योन्याश्रय संबंध विकल्प जाल-रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इन्द्रिय विषयों में न मोह करो, न
ध्यान के साथ कायोत्सर्ग शब्द भी जुड़ा हुआ है। आवश्यक राग करो और न द्वेष करो। हे भव्यो ! कुछ भी चेष्टा मत करो,
चूर्णि में कहा गया है कि कायोत्सर्ग द्रव्य और भाव से दो प्रकार कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिन्तन मत करो, जिससे आत्मा
का है। द्रव्य से कायचेष्टानिरोध और भाव से "ध्यान" ही निजात्मा में तल्लीन होकर स्थिर हो जाए। यही (आत्मा में आत्मा
कायोत्सर्ग है। "तस्स उत्तरी करण" पाठ में भी ध्यान रूप की लीनता ही) परम ध्यान है।
कायोत्सर्ग का माहात्म्य बताते हुए कहा है-१. आत्मा को विशेष 100.00 | रूप से उत्कृष्ट बनाने हेतु, २. प्रायश्चित = पापों का शोधन करने
20909 ध्यानयोगी का लक्षण और योग्यता
हेतु, ३. मिथ्या धारणाओं, भ्रांतियों तथा मिथ्यात्व के कारण अशुद्ध ध्यानयोगी का लक्षण श्रमणसुत्तं में इस प्रकार व्यक्त किया गया बनी हुई आत्मा को विशुद्ध करने हेतु या परम विशुद्ध स्वरूप को है-ध्यानयोगी वह है, जो अपनी आत्मा को समस्त बाह्य संयोगों प्राप्त करने हेतु तथा आत्मा को माया, निदान और मिथ्यादर्शन, तथा शरीर और शरीर से संबद्ध पदार्थों से विविक्त (भिन्न) देखता । इन तीन शल्यों से मुक्त करने हेतु एवं प्राणातिपात, मृषावाद आदि है, वह शरीर और उपधि का उत्सर्ग (समत्वत्याग) करके सर्वथा १८ प्रकार के पापों को नष्ट करने हेतु मैं स्थान (काया से स्थिर), निःसंग हो जाता है। वही साधक आत्मा का ध्याता है, जो अपने | मौन (वचन से मौन) और मन से ध्यानपूर्वक कायोत्सर्ग (ध्यान) ध्यान में चिन्तन करता है कि "मैं" न “पर" का हूँ और न ही } करता हूँ।
Jain dedition international
636Private spelsaralegIVDIODDO 10046600.
00
929 Vijayeubrary.ro
Docu
020