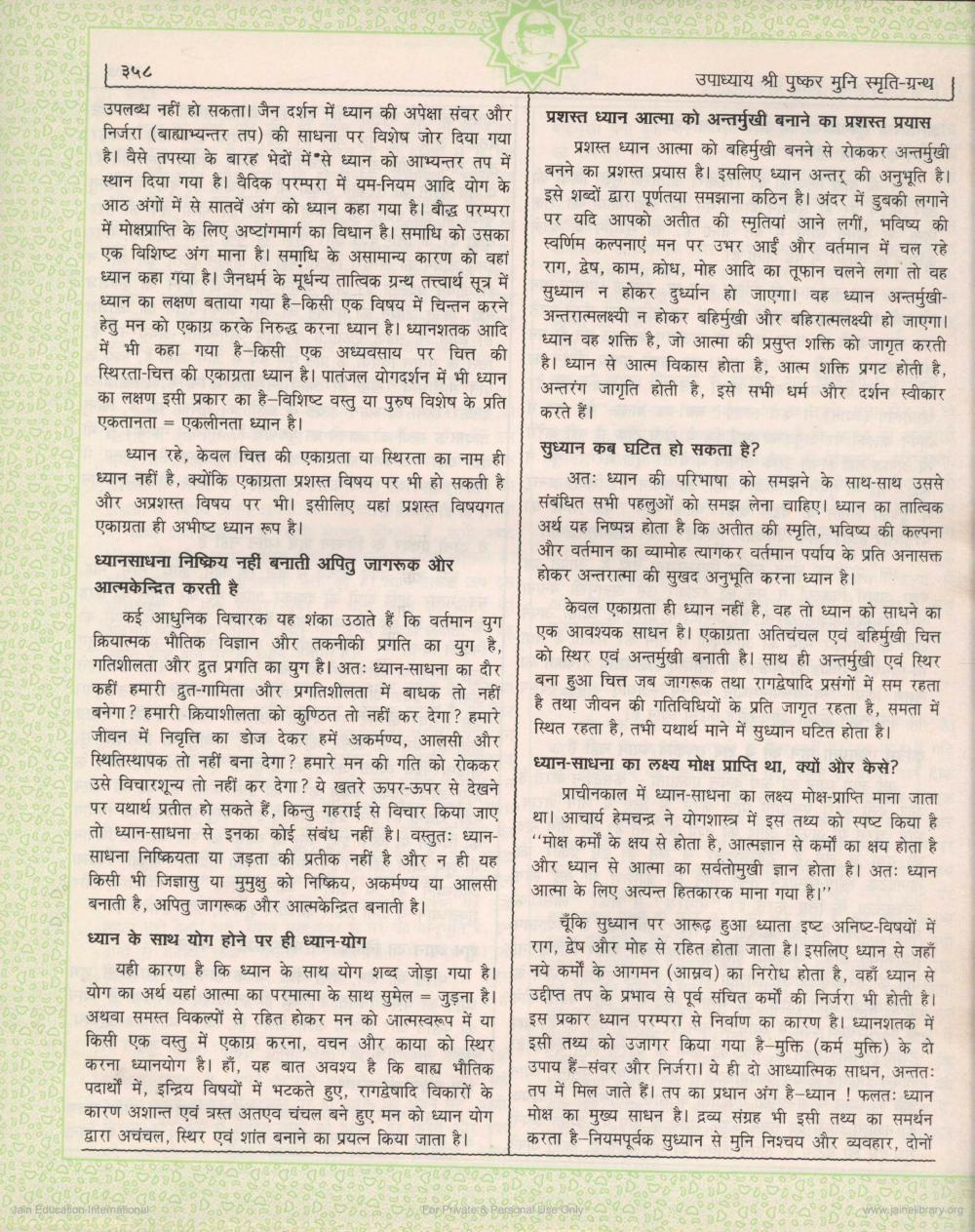________________
३५८
उपलब्ध नहीं हो सकता। जैन दर्शन में ध्यान की अपेक्षा संवर और निर्जरा (बाह्याभ्यन्तर तप) की साधना पर विशेष जोर दिया गया है। वैसे तपस्या के बारह भेदों में से ध्यान को आभ्यन्तर तप में स्थान दिया गया है। वैदिक परम्परा में यम-नियम आदि योग के आठ अंगों में से सातवें अंग को ध्यान कहा गया है। बौद्ध परम्परा में मोक्षप्राप्ति के लिए अष्टांगमार्ग का विधान है। समाधि को उसका एक विशिष्ट अंग माना है। समाधि के असामान्य कारण को वहां ध्यान कहा गया है। जैनधर्म के मूर्धन्य तात्विक ग्रन्थ तत्त्वार्थ सूत्र में ध्यान का लक्षण बताया गया है-किसी एक विषय में चिन्तन करने हेतु मन को एकाग्र करके निरुद्ध करना ध्यान है। ध्यानशतक आदि में भी कहा गया है किसी एक अध्यवसाय पर चित्त की स्थिरता चित्त की एकाग्रता ध्यान है पातंजल योगदर्शन में भी ध्यान का लक्षण इसी प्रकार का है-विशिष्ट वस्तु या पुरुष विशेष के प्रति एकतानता = एकलीनता ध्यान है।
ध्यान रहे, केवल चित्त की एकाग्रता या स्थिरता का नाम ही ध्यान नहीं है, क्योंकि एकाग्रता प्रशस्त विषय पर भी हो सकती है। और अप्रशस्त विषय पर भी इसीलिए यहां प्रशस्त विषयगत एकाग्रता ही अभीष्ट ध्यान रूप है।
ध्यानसाधना निष्क्रिय नहीं बनाती अपितु जागरूक और आत्मकेन्द्रित करती है
कई आधुनिक विचारक यह शंका उठाते हैं कि वर्तमान युग क्रियात्मक भौतिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति का युग है, गतिशीलता और द्रुत प्रगति का युग है अतः ध्यान-साधना का दौर कहीं हमारी द्रुत-गामिता और प्रगतिशीलता में बाधक तो नहीं बनेगा ? हमारी क्रियाशीलता को कुण्ठित तो नहीं कर देगा? हमारे जीवन में निवृत्ति का डोज देकर हमें अकर्मण्य, आलसी और स्थितिस्थापक तो नहीं बना देगा? हमारे मन की गति को रोककर उसे विचारशून्य तो नहीं कर देगा? ये खतरे ऊपर-ऊपर से देखने पर यथार्थ प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु गहराई से विचार किया जाए तो ध्यान-साधना से इनका कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः ध्यानसाधना निष्क्रियता या जड़ता की प्रतीक नहीं है और न ही यह किसी भी जिज्ञासु या मुमुक्षु को निष्क्रिय, अकर्मण्य या आलसी बनाती है, अपितु जागरूक और आत्मकेन्द्रित बनाती है।
ध्यान के साथ योग होने पर ही ध्यान-योग
यही कारण है कि ध्यान के साथ योग शब्द जोड़ा गया है। योग का अर्थ यहां आत्मा का परमात्मा के साथ सुमेल - जुड़ना है। अथवा समस्त विकल्पों से रहित होकर मन को आत्मस्वरूप में या किसी एक वस्तु में एकाग्र करना, वचन और काया को स्थिर करना ध्यानयोग है। हाँ, यह बात अवश्य है कि बाह्य भौतिक पदार्थों में, इन्द्रिय विषयों में भटकते हुए, रागद्वेषादि विकारों के कारण अशान्त एवं त्रस्त अतएव चंचल बने हुए मन को ध्यान योग द्वारा अचंचल, स्थिर एवं शांत बनाने का प्रयत्न किया जाता है।
Jain Education International
SOUR 1900
2008
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
प्रशस्त ध्यान आत्मा को अन्तर्मुखी बनाने का प्रशस्त प्रयास
प्रशस्त ध्यान आत्मा को बहिर्मुखी बनने से रोककर अन्तर्मुखी बनने का प्रशस्त प्रयास है। इसलिए ध्यान अन्तर् की अनुभूति है। इसे शब्दों द्वारा पूर्णतया समझाना कठिन है। अंदर में डुबकी लगाने पर यदि आपको अतीत की स्मृतियां आने लगी, भविष्य की स्वर्णिम कल्पनाएं मन पर उभर आई और वर्तमान में चल रहे राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि का तूफान चलने लगा तो वह सुध्यान न होकर दुर्ध्यान हो जाएगा। यह ध्यान अन्तर्मुखीअन्तरात्मलक्ष्यी न होकर बहिर्मुखी और बहिरात्मलक्ष्यी हो जाएगा। ध्यान वह शक्ति है, जो आत्मा की प्रसुप्त शक्ति को जागृत करती है। ध्यान से आत्म विकास होता है, आत्म शक्ति प्रगट होती है, अन्तरंग जागृति होती है, इसे सभी धर्म और दर्शन स्वीकार करते हैं।
सुध्यान कब घटित हो सकता है?
अतः ध्यान की परिभाषा को समझने के साथ-साथ उससे संबंधित सभी पहलुओं को समझ लेना चाहिए। ध्यान का तात्विक अर्थ यह निष्पन्न होता है कि अतीत की स्मृति भविष्य की कल्पना और वर्तमान का व्यामोह त्यागकर वर्तमान पर्याय के प्रति अनासक्त होकर अन्तरात्मा की सुखद अनुभूति करना ध्यान है।
केवल एकाग्रता ही ध्यान नहीं है, वह तो ध्यान को साधने का एक आवश्यक साधन है। एकाग्रता अतिचंचल एवं बहिर्मुखी चित्त को स्थिर एवं अन्तर्मुखी बनाती है। साथ ही अन्तर्मुखी एवं स्थिर बना हुआ चित्त जब जागरूक तथा रागद्वेषादि प्रसंगों में सम रहता है तथा जीवन की गतिविधियों के प्रति जागृत रहता है, समता में स्थित रहता है, तभी यथार्थ माने में सुध्यान घटित होता है। ध्यान-साधना का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, क्यों और कैसे?
प्राचीनकाल में ध्यान-साधना का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति माना जाता था। आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में इस तथ्य को स्पष्ट किया है। "मोक्ष कर्मों के क्षय से होता है, आत्मज्ञान से कर्मों का क्षय होता है और ध्यान से आत्मा का सर्वतोमुखी ज्ञान होता है। अतः ध्यान आत्मा के लिए अत्यन्त हितकारक माना गया है।"
Cop Private & Personal
चूँकि सुध्यान पर आरूढ़ हुआ ध्याता इष्ट अनिष्ट विषयों में राग, द्वेष और मोह से रहित होता जाता है। इसलिए ध्यान से जहाँ नये कर्मों के आगमन (आस्रव) का निरोध होता है, वहाँ ध्यान से उद्दीप्त तप के प्रभाव से पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार ध्यान परम्परा से निर्वाण का कारण है। ध्यानशतक में इसी तथ्य को उजागर किया गया है मुक्ति (कर्म मुक्ति) के दो उपाय है-संबर और निर्जरा ये ही दो आध्यात्मिक साधन, अन्ततः तप में मिल जाते हैं। तप का प्रधान अंग है-ध्यान ! फलतः ध्यान मोक्ष का मुख्य साधन है। द्रव्य संग्रह भी इसी तथ्य का समर्थन करता है-नियमपूर्वक सुध्यान से मुनि निश्चय और व्यवहार, दोनों
www.jainelibrary.org