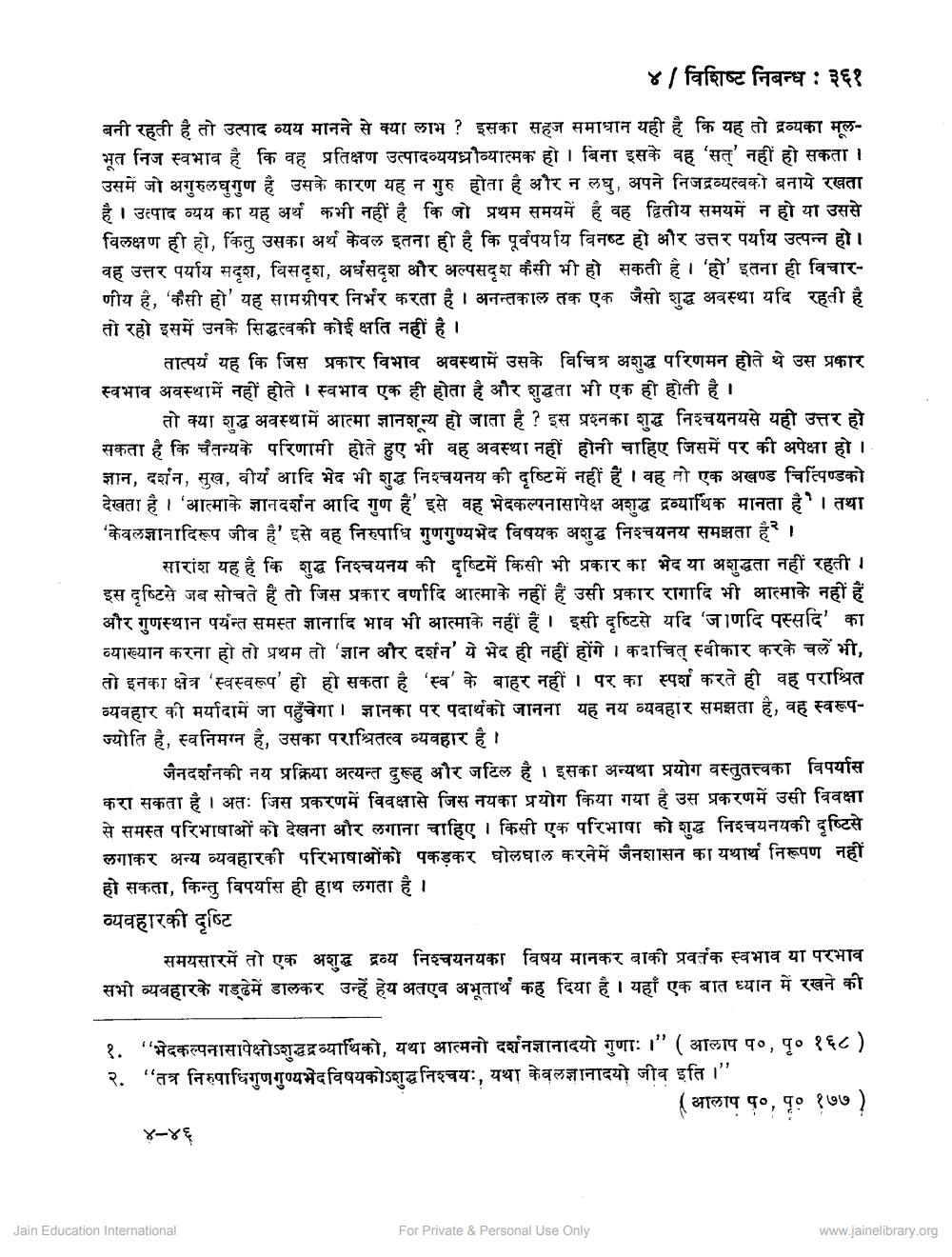________________
४/ विशिष्ट निबन्ध : ३६१
बनी रहती है तो उत्पाद व्यय मानने से क्या लाभ ? इसका सहज समाधान यही है कि यह तो द्रव्यका मूलभूत निज स्वभाव है कि वह प्रतिक्षण उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक हो । बिना इसके वह 'सत्' नहीं हो सकता। उसमें जो अगुरुलघुगुण है उसके कारण यह न गुरु होता है और न लघु, अपने निजद्रव्यत्वको बनाये रखता है । उत्पाद व्यय का यह अर्थ कभी नहीं है कि जो प्रथम समयमें है वह द्वितीय समयमें न हो या उससे विलक्षण ही हो, किंतु उसका अर्थ केवल इतना ही है कि पूर्वपर्याय विनष्ट हो और उत्तर पर्याय उत्पन्न हो। वह उत्तर पर्याय सदृश, विसदृश, अर्धसदृश और अल्पसदृश कैसी भी हो सकती है । 'हो' इतना ही विचारणीय है, 'कैसी हो' यह सामग्रीपर निर्भर करता है । अनन्तकाल तक एक जैसो शुद्ध अवस्था यदि रहती है तो रहो इसमें उनके सिद्धत्वकी कोई क्षति नहीं है ।
तात्पर्य यह कि जिस प्रकार विभाव अवस्थामें उसके विचित्र अशुद्ध परिणमन होते थे उस प्रकार स्वभाव अवस्थामें नहीं होते । स्वभाव एक ही होता है और शुद्धता भी एक ही होती है ।
तो क्या शुद्ध अवस्थामें आत्मा ज्ञानशन्य हो जाता है ? इस प्रश्नका शुद्ध निश्चयनयसे यही उत्तर हो सकता है कि चैतन्यके परिणामी होते हुए भी वह अवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें पर की अपेक्षा हो । ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि भेद भी शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि में नहीं है। वह तो एक अखण्ड चित्पिण्डको देखता है । 'आत्माके ज्ञानदर्शन आदि गुण हैं' इसे वह भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक मानता है । तथा 'केवलज्ञानादिरूप जीव है' इसे वह निरुपाधि गुणगुण्यभेद विषयक अशुद्ध निश्चयनय समझता है ।
सारांश यह है कि शुद्ध निश्चयनय की दृष्टिमें किसी भी प्रकार का भेद या अशुद्धता नहीं रहती। इस दृष्टिसे जब सोचते हैं तो जिस प्रकार वर्णादि आत्माके नहीं है उसी प्रकार रागादि भी आत्माके नहीं है और गुणस्थान पर्यन्त समस्त ज्ञानादि भाव भी आत्माके नहीं हैं। इसी दृष्टिसे यदि 'जाणदि पस्सदि' का व्याख्यान करना हो तो प्रथम तो 'ज्ञान और दर्शन' ये भेद ही नहीं होंगे। कदाचित् स्वीकार करके चलें भी, तो इनका क्षेत्र 'स्वस्वरूप' हो हो सकता है 'स्व' के बाहर नहीं। पर का स्पर्श करते ही वह पराश्रित व्यवहार की मर्यादामें जा पहुँचेगा। ज्ञानका पर पदार्थको जानना यह नय व्यवहार समझता है, वह स्वरूपज्योति है, स्वनिमग्न है, उसका पराश्रितत्व व्यवहार है।
जैनदर्शनकी नय प्रक्रिया अत्यन्त दुरूह और जटिल है । इसका अन्यथा प्रयोग वस्तुतत्त्वका विपर्यास करा सकता है । अतः जिस प्रकरणमें विवक्षासे जिस नयका प्रयोग किया गया है उस प्रकरणमें उसी विवक्षा से समस्त परिभाषाओं को देखना और लगाना चाहिए। किसी एक परिभाषा को शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे लगाकर अन्य व्यवहारकी परिभाषाओंको पकड़कर घोलघाल करने में जैनशासन का यथार्थ निरूपण नहीं हो सकता, किन्तु विपर्यास ही हाथ लगता है । व्यवहारकी दृष्टि
समयसारमें तो एक अशुद्ध द्रव्य निश्चयनयका विषय मानकर बाकी प्रवर्तक स्वभाव या परभाव सभी व्यवहारके गड्ढेमें डालकर उन्हें हेय अतएव अभूतार्थ कह दिया है । यहाँ एक बात ध्यान में रखने की
१. "भेदकल्पनासापेक्षोऽशद्धद्रव्याथिको, यथा आत्मनो दर्शनज्ञानादयो गुणाः ।" (आलाप प०, पृ० १६८) २. “तत्र निरुपाधिगुणगुण्यभेदविषयकोऽशुद्ध निश्चयः, यथा केवलज्ञानादयो जीव इति ।"
( आलाप प०, पृ० १७७)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org