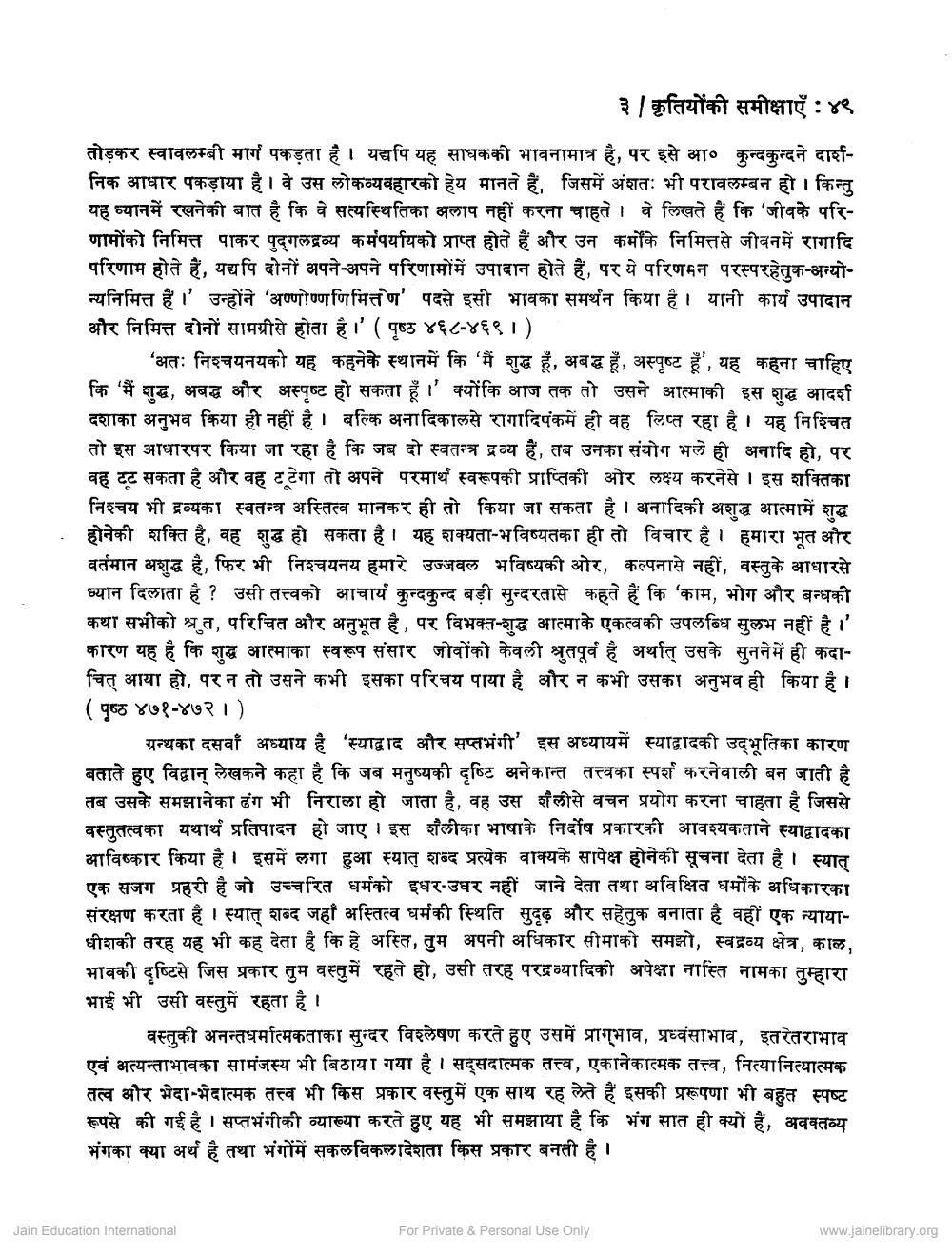________________
३ / कृतियोंकी समीक्षाएँ : ४९ तोड़कर स्वावलम्बी मार्ग पकड़ता है । यद्यपि यह साधकको भावनामात्र है, पर इसे आ० कुन्दकुन्दने दार्शनिक आधार पकड़ाया है। वे उस लोकव्यवहारको हेय मानते हैं, जिसमें अंशतः भी परावलम्बन हो । किन्तु यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि वे सत्यस्थितिका अलाप नहीं करना चाहते। वे लिखते हैं कि 'जीवके परिणामोंको निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य कर्मपर्यायको प्राप्त होते हैं और उन कर्मोंके निमित्तसे जीवन में रागादि परिणाम होते हैं, यद्यपि दोनों अपने-अपने परिणामोंमें उपादान होते हैं, पर ये परिणमन परस्परहेतुक-अन्योन्यनिमित्त है।' उन्होंने 'अण्णोण्णणि मित्तण' पदसे इसी भावका समर्थन किया है। यानी कार्य उपादान और निमित्त दोनों सामग्रीसे होता है।' ( पृष्ठ ४६८-४६९ । )
'अतः निश्चयनयको यह कहनेके स्थानमें कि 'मैं शुद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ', यह कहना चाहिए कि 'मैं शुद्ध, अबद्ध और अस्पृष्ट हो सकता हूँ।' क्योंकि आज तक तो उसने आत्माकी इस शद्ध आदर्श दशाका अनुभव किया ही नहीं है। बल्कि अनादिकालसे रागादिपंकमें ही वह लिप्त रहा है। यह निश्चित
इस आधारपर किया जा रहा है कि जब दो स्वतन्त्र द्रव्य है, तब उनका संयोग भले ही अनादि हो, पर वह टट सकता है और वह ट टेगा तो अपने परमार्थ स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर लक्ष्य करनेसे । इस शक्तिका निश्चय भी द्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व मानकर ही तो किया जा सकता है । अनादिकी अशुद्ध आत्मामें शद्ध होनेकी शक्ति है, वह शुद्ध हो सकता है। यह शक्यता-भविष्यतका ही तो विचार है। हमारा भूत और वर्तमान अशुद्ध है, फिर भी निश्चयनय हमारे उज्जवल भविष्यकी ओर, कल्पनासे नहीं, वस्तुके आधारसे ध्यान दिलाता है ? उसी तत्त्वको आचार्य कुन्दकुन्द बड़ी सुन्दरतासे कहते हैं कि 'काम, भोग और बन्धकी कथा सभीको श्रत, परिचित और अनुभूत है, पर विभक्त-शुद्ध आत्माके एकत्वकी उपलब्धि सुलभ नहीं है।' कारण यह है कि शुद्ध आत्माका स्वरूप संसार जीवोंको केवली श्रुतपूर्व है अर्थात् उसके सुनने में ही कदाचित् आया हो, पर न तो उसने कभी इसका परिचय पाया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। (पृष्ठ ४७१-४७२ । )
ग्रन्थका दसवाँ अध्याय है 'स्याद्वाद और सप्तभंगी' इस अध्यायमें स्याद्वादकी उद्भतिका कारण बताते हुए विद्वान् लेखकने कहा है कि जब मनुष्यकी दृष्टि अनेकान्त तत्त्वका स्पर्श करनेवाली बन जाती है तब उसके समझानेका ढंग भी निराला हो जाता है, वह उस शैलीसे वचन प्रयोग करना चाहता है जिससे वस्ततत्वका यथार्थ प्रतिपादन हो जाए । इस शैलीका भाषाके निर्दोष प्रकारकी आवश्यकताने स्याद्वादका आविष्कार किया है। इसमें लगा हुआ स्यात् शब्द प्रत्येक वाक्यके सापेक्ष होनेकी सूचना देता है। स्यात एक सजग प्रहरी है जो उच्चरित धर्मको इधर-उधर नहीं जाने देता तथा अविक्षित धर्मों के अधिकारका संरक्षण करता है । स्यात् शब्द जहाँ अस्तित्व धर्मकी स्थिति सुदृढ़ और सहेतुक बनाता है वहीं एक न्यायाधीशकी तरह यह भी कह देता है कि हे अस्ति, तुम अपनी अधिकार सीमाको समझो, स्वद्रव्य क्षेत्र, काल. भावकी दृष्टिसे जिस प्रकार तुम वस्तुमें रहते हो, उसी तरह परद्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति नामका तुम्हारा भाई भी उसी वस्तुमें रहता है।
वस्तूकी अनन्तधर्मात्मकताका सुन्दर विश्लेषण करते हुए उसमें प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव एवं अत्यन्ताभावका सामंजस्य भी बिठाया गया है । सद्सदात्मक तत्त्व, एकानेकात्मक तत्त्व, नित्यानित्यात्मक तत्व और भेदा-भेदात्मक तत्त्व भी किस प्रकार वस्तुमें एक साथ रह लेते हैं इसकी प्ररूपणा भी बहुत स्पष्ट रूपसे की गई है । सप्तभंगीकी व्याख्या करते हुए यह भी समझाया है कि भंग सात ही क्यों हैं, अवक्तव्य भंगका क्या अर्थ है तथा भंगोंमें सकलविकलादेशता किस प्रकार बनती है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org