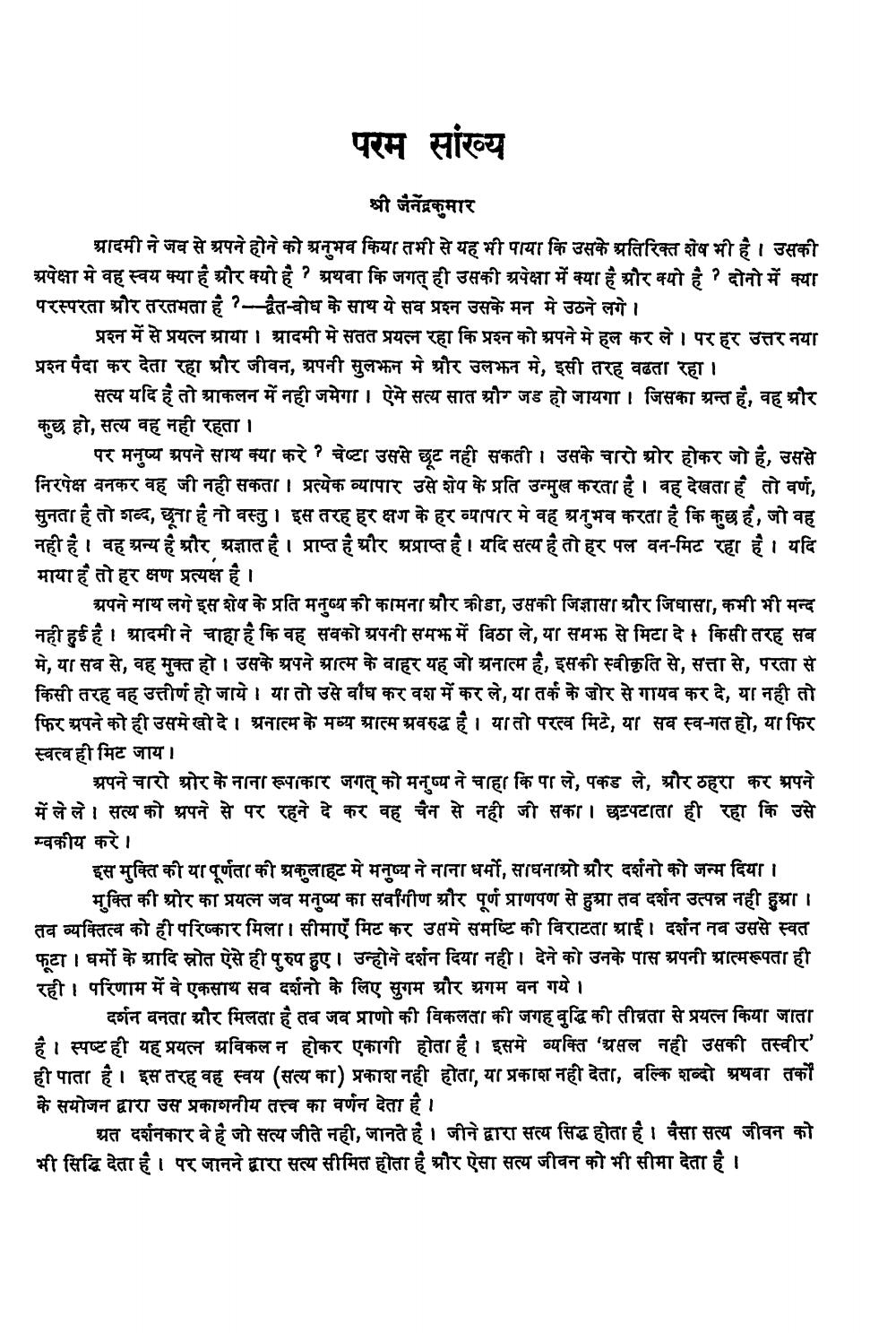________________
परम सांख्य
श्री जैनेंद्रकुमार आदमी ने जव से अपने होने को अनुभव किया तभी से यह भी पाया कि उसके अतिरिक्त शेष भी है । उसकी अपेक्षा मे वह स्वय क्या है और क्यो है ? अथवा कि जगत् ही उसकी अपेक्षा में क्या है और क्यो है ? दोनो में क्या परस्परता और तरतमता है ?--द्वैत-बोध के साथ ये सब प्रश्न उसके मन में उठने लगे।
प्रश्न में से प्रयत्न आया। आदमी मे सतत प्रयत्न रहा कि प्रश्न को अपने मे हल कर ले। पर हर उत्तर नया प्रश्न पैदा कर देता रहा और जीवन, अपनी सुलझन मे और उलझन मे, इसी तरह वढता रहा ।
सत्य यदि है तो आकलन में नही जमेगा । ऐमे सत्य सात और जड हो जायगा। जिसका अन्त है, वह और कुछ हो, सत्य वह नही रहता।
पर मनुष्य अपने साथ क्या करे? चेष्टा उससे छूट नही सकती। उसके चारो ओर होकर जो है, उससे निरपेक्ष बनकर वह जी नही सकता। प्रत्येक व्यापार उसे शेप के प्रति उन्मुख करता है। वह देखता है तो वर्ण, सुनता है तो शब्द, छूता है तो वस्तु। इस तरह हर क्षग के हर व्यापार मे वह अनुभव करता है कि कुछ है, जो वह नहीं है । वह अन्य है और अज्ञात है । प्राप्त है और अप्राप्त है। यदि सत्य है तो हर पल वन-मिट रहा है। यदि माया है तो हर क्षण प्रत्यक्ष है।
__ अपने माथ लगे इस शेष के प्रति मनुष्य की कामना और क्रीडा, उसकी जिज्ञासा और जिघासा, कभी भी मन्द नही हुई है। आदमी ने चाहा है कि वह सबको अपनी समझ में विठा ले, या समझ से मिटा दे। किसी तरह सब मे, या सव से, वह मुक्त हो । उसके अपने प्रात्म के बाहर यह जो अनात्म है, इसको स्वीकृति से, सत्ता से, परता से किसी तरह वह उत्तीर्ण हो जाये। या तो उसे बाँध कर वश में कर ले, या तर्क के ज़ोर से गायब कर दे, या नही तो फिर अपने को ही उसमेखो दे। अनात्म के मध्य आत्म अवरुद्ध है। या तो परत्व मिटे, या सव स्व-गत हो, या फिर स्वत्व ही मिट जाय।
अपने चारो ओर के नाना रूपाकार जगत् को मनुष्य ने चाहा कि पा ले, पकड ले, और ठहरा कर अपने में ले ले। सत्य को अपने से पर रहने दे कर वह चैन से नहीं जी सका। छटपटाता ही रहा कि उसे म्वकीय करे।
इस मुक्ति की या पूर्णता को अकुलाहट मे मनुष्य ने नाना धर्मो, साधनाओ और दर्शनो को जन्म दिया।
मुक्ति की अोर का प्रयल जव मनुष्य का सर्वांगीण और पूर्ण प्राणपण से हुआ तव दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ। तव व्यक्तित्व को ही परिष्कार मिला। सीमाएँ मिट कर उसमे समष्टि को विराटता आई। दर्शन नब उससे स्वत फूटा । धर्मों के आदि स्रोत ऐसे ही पुरुष हुए। उन्होने दर्शन दिया नही। देने को उनके पास अपनी आत्मरूपता ही रही। परिणाम में वे एकसाथ सव दर्शनो के लिए सुगम और अगम वन गये।
दर्शन वनता और मिलता है तब जब प्राणो की विकलता की जगह बुद्धि की तीव्रता से प्रयत्न किया जाता है। स्पष्ट ही यह प्रयत्न अविकल न होकर एकागी होता है। इसमें व्यक्ति 'असल नहीं उसकी तस्वीर' ही पाता है। इस तरह वह स्वय (सत्य का) प्रकाश नहीं होता, या प्रकाश नहीं देता, बल्कि शब्दो अथवा तों के सयोजन द्वारा उस प्रकाशनीय तत्त्व का वर्णन देता है।
। अत दर्शनकार वे है जो सत्य जीते नही, जानते है । जीने द्वारा सत्य सिद्ध होता है। वैसा सत्य जीवन को भी सिद्धि देता है। पर जानने द्वारा सत्य सीमित होता है और ऐसा सत्य जीवन को भी सीमा देता है।