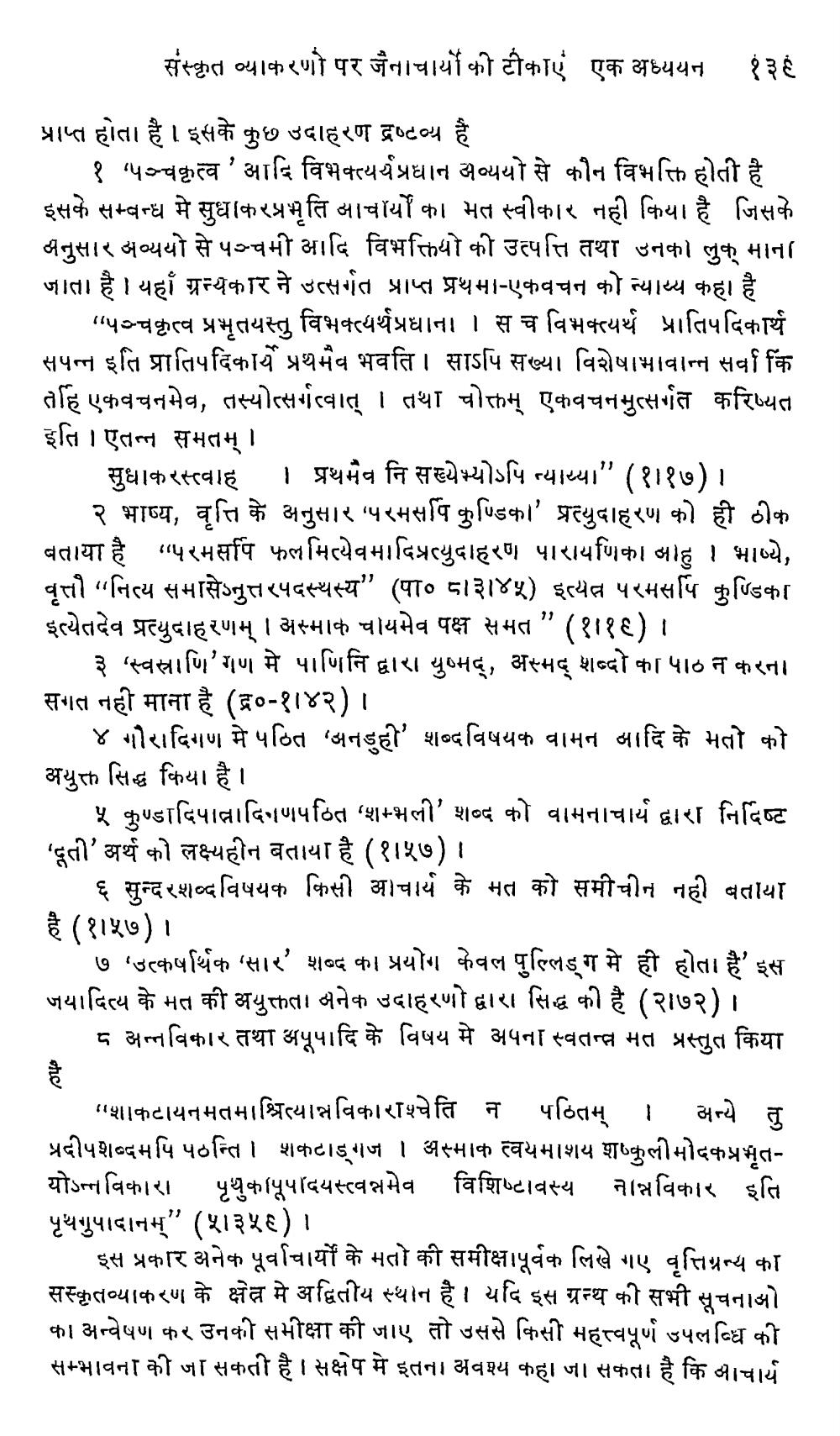________________
संस्कृत व्याकरणो पर जैनाचार्यों की टीकाएं एक अध्ययन १३६
प्राप्त होता है । इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है
१ ५ञ्चकृत्व' आदि विभक्त्यर्थप्रधान अव्ययो से कौन विभक्ति होती है इसके सम्बन्ध मे सुधाकरप्रभृति आचार्यों का मत स्वीकार नही किया है जिसके अनुसार अव्ययो से पञ्चमी आदि विभक्तियो की उत्पत्ति तथा उनका लुक माना जाता है। यहाँ ग्रन्यकार ने उत्सर्गत प्राप्त प्रथमा-एकवचन को न्याय्य कहा है
"५-चकृत्व प्रभृतयस्तु विभक्त्यर्थप्रधाना । स च विभक्त्यर्थ प्रातिपदिकार्थ सपन्न इति प्रातिपदिकार्य प्रथमेव भवति । साऽपि सख्या विशेषाभावान्न सर्वा कि तहि एकवचनमेव, तस्योत्सर्गत्वात् । तथा चोक्तम् एकवचनमुत्सर्गत करिष्यत इति । एतन्न समतम् ।
सुधाकरस्वाह । प्रथमैन नि सख्येभ्योऽपि न्याय्या" (१११७)।
२ भाष्य, वृत्ति के अनुसार परमसपि कुण्डिका' प्रत्युदाहरण को ही ठीक बताया है "परमसपि फलमित्येवमादिप्रत्युदाहरण पारायणिका आहु । भाष्ये, वृत्ती "नित्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्य" (पा० ८।३।४५) इत्यत्र परमसपि कुण्डिका इत्येतदेव प्रत्युदाहरणम् । अस्माक चायमेव पक्ष समत" (१३१६) ।
३ 'स्वस्राणि गण मे पाणिनि द्वारा युष्मद्, अस्मद् शब्दो का पा० न करना सगत नही माना है (द्र०-११४२)।
४ गौरादिगण मे पठित 'अनही' शब्दविषयक वामन आदि के मतो को अयुक्त सिद्ध किया है।
५ कुण्डादिपानादिगणपठित 'शम्भली' शब्द को वामनाचार्य द्वारा निर्दिष्ट 'दूती' अर्थ को लक्ष्यहीन बताया है (१९५७) ।
६ सुन्दर शब्दविषयक किसी आचार्य के मत को समीचीन नही बताया है (११५७)।
७ 'उत्कर्थिक 'सार' शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिड्ग मे ही होता है। इस जयादित्य के मत की अयुक्तता अनेक उदाहरणो द्वारा सिद्ध की है (२०७२) ।
८ अन्नविकार तथा अपूपादि के विषय मे अपना स्वतन्न मत प्रस्तुत किया
"शाकटायनमतमाश्रित्यान्न विकाराश्चेति न पठितम् । अन्ये तु प्रदीपशब्दमपि ५०न्ति। शकटाड्गज । अस्माक त्वयमाशय शकुलीमोदकप्रभूतयोऽनविकारा पृथु कापूपादयस्वनमेव विशिष्टावस्य नानविकार इति पृथगुपादानम्" (५।३५६)।
इस प्रकार अनेक पूर्वाचार्यों के मतो की समीक्षापूर्वक लिखे गए वृत्तिअन्य का सस्कृतव्याकरण के क्षेत्र मे अद्वितीय स्थान है। यदि इस ग्रन्थ की सभी सूचनाओ का अन्वेषण कर उनकी समीक्षा की जाए तो उससे किसी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि की सम्भावना की जा सकती है । संक्षेप मे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आचार्य