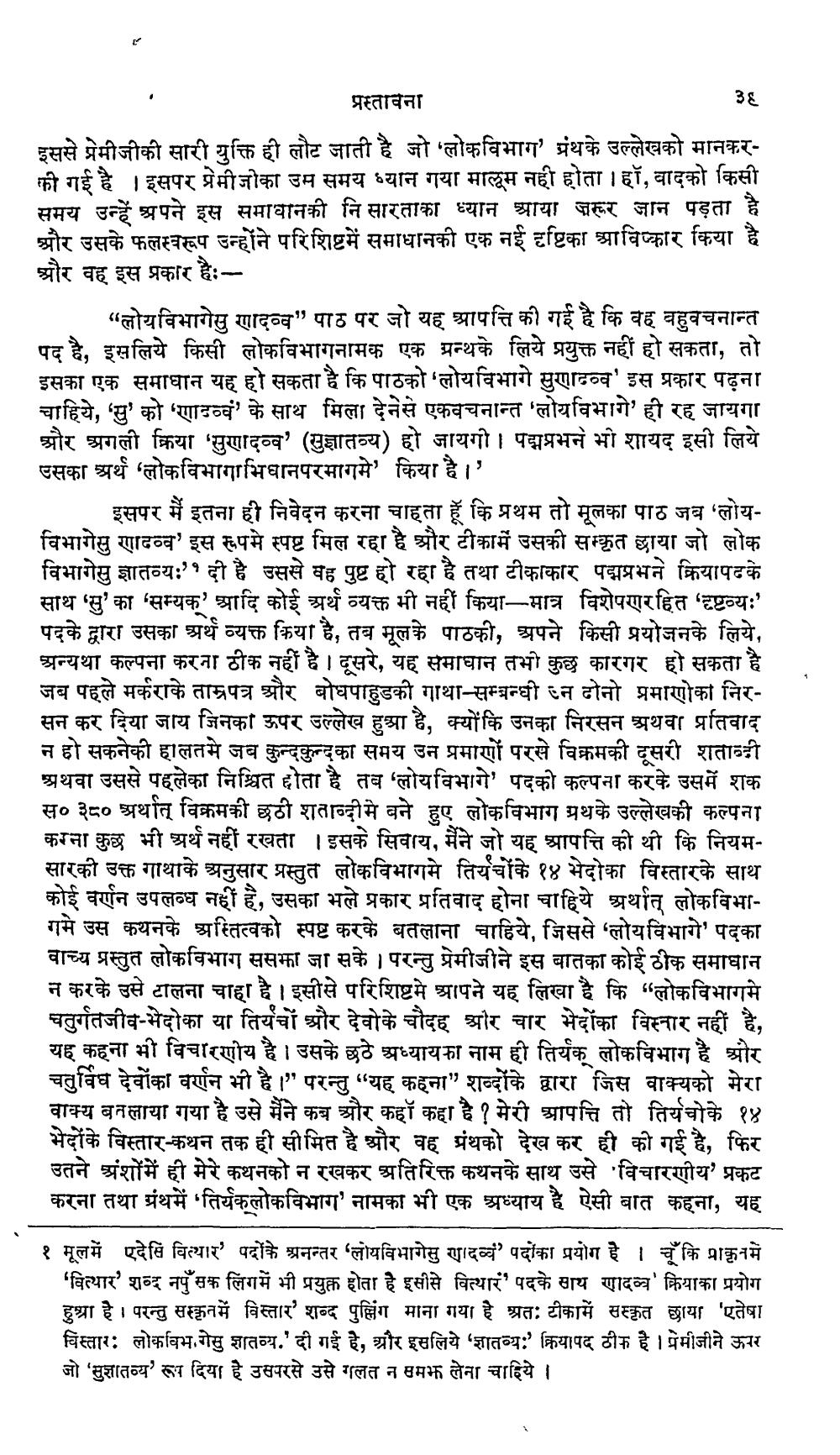________________
३६
प्रस्तावना इससे प्रेमीजीकी सारी युक्ति ही लौट जाती है जो 'लोकविभाग' ग्रंथके उल्लेखको मानकरकी गई है । इसपर प्रेमीजोका उम समय ध्यान गया मालूम नहीं होता । हाँ, वादको किसी समय उन्हें अपने इस समाधानकी नि सारताका ध्यान आया जरूर जान पड़ता है और उसके फलस्वरूप उन्होंने परिशिष्टमें समाधानकी एक नई दृष्टिका आविष्कार किया है और वह इस प्रकार है:
"लोयविभागेसु णादव" पाठ पर जो यह आपत्ति की गई है कि वह बहुवचनान्त पद है, इसलिये किसी लोकविभागनामक एक ग्रन्थके लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता, तो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठको 'लोयविभागे सुणाढव्व' इस प्रकार पढ़ना चाहिये, 'सु' को 'णादव्वं' के साथ मिला देनेसे एकवचनान्त 'लोयविभागे' ही रह जायगा
और अगली क्रिया 'सुणादव' (सुज्ञातव्य) हो जायगी। पद्मप्रभने भो शायद इसी लिये उसका अर्थ 'लोकविभागाभिधानपरमागमे' किया है।'
इसपर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम तो मूलका पाठ जब 'लोयविभागेसु णादव्व' इस रूपमे स्पष्ट मिल रहा है और टीकामें उसकी सस्कृत छाया जो लोक विभागेसु ज्ञातव्यः'' दी है उससे वह पुष्ट हो रहा है तथा टीकाकार पद्मप्रभने क्रियापदके साथ 'सु' का 'सम्यक' आदि कोई अर्थ व्यक्त भी नहीं किया-मात्र विशेषणरहित 'दृष्टव्यः' पदके द्वारा उसका अर्थ व्यक्त किया है, तब मूल के पाठकी, अपने किसी प्रयोजनके लिये, अन्यथा कल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मर्कराके ताम्रपत्र और बोधपाहुडकी गाथा-सम्बन्धी उन दोनो प्रमाणोका निरसन कर दिया जाय जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है, क्योंकि उनका निरसन अथवा प्रतिवाद न हो सकनेकी हालतमे जब कुन्दकुन्दका समय उन प्रमाणों परसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी अथवा उससे पहलेका निश्चित होता है तब 'लोयविभागे' पदको कल्पना करके उसमें शक स० ३८० अर्थात् विक्रमकी छठी शताब्दीमे बने हुए लोकविभाग अथके उल्लेखकी कल्पना करना कुछ भी अर्थ नहीं रखता । इसके सिवाय, मैंने जो यह आपत्ति की थी कि नियमसारकी उक्त गाथाके अनुसार प्रस्तुत लोकविभागमे तियचोंके १४ भेदोका विस्तारके साथ कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है, उसका भले प्रकार प्रतिवाद होना चाहिये अर्थात् लोकविभागमे उस कथनके अस्तित्वको स्पष्ट करके बतलाना चाहिये, जिससे 'लोयविभागे' पदका वाच्य प्रस्तुत लोकविभाग ससमा जा सके । परन्तु प्रेमीजीने इस बातका कोई ठीक समाधान न करके उसे टालना चाहा है। इसीसे परिशिष्टमे आपने यह लिखा है कि "लोकविभागमे चतुर्गतजीव-भेदोका या तियंचों और देवोके चौदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कहना भी विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तिर्यक् लोकविभाग है और चतुर्विध देवोंका वर्णन भी है।" परन्तु “यह कहना" शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यको मेरा वाक्य बतलाया गया है उसे मैंने कब और कहाँ कहा है ? मेरी आपत्ति तो तिर्यचोके १४ भेदोंके विस्तार-कथन तक ही सीमित है और वह ग्रंथको देख कर ही की गई है, फिर उतने अंशोंमें ही मेरे कथनको न रखकर अतिरिक्त कथनके साथ उसे 'विचारणीय' प्रकट करना तथा ग्रंथमें 'तिर्यकलोकविभाग' नामका भी एक अध्याय है ऐसी बात कहना, यह
१ मूलमें एदेसि वित्यार' पदोंके अनन्तर 'लोयविभागेसु णादव्य' पदोंका प्रयोग है । चूँकि प्राकृनमें 'वित्यार' शब्द नपुंसक लिंगमें भी प्रयुक्त होता है इसीसे वित्यारं' पदके साथ णादव्य' क्रियाका प्रयोग हुश्रा है। परन्तु सस्कृतमें विस्तार' शब्द पुल्लिंग माना गया है अतः टीकामें सस्कृत छाया 'एतेषा विस्तार: लोकविभागेसु ज्ञातव्य.' दी गई है, और इसलिये 'ज्ञातव्यः' क्रियापद ठीक है । प्रेमीजीने ऊपर जो 'सुज्ञातव्य' रूप दिया है उसपरसे उसे गलत न समझ लेना चाहिये ।