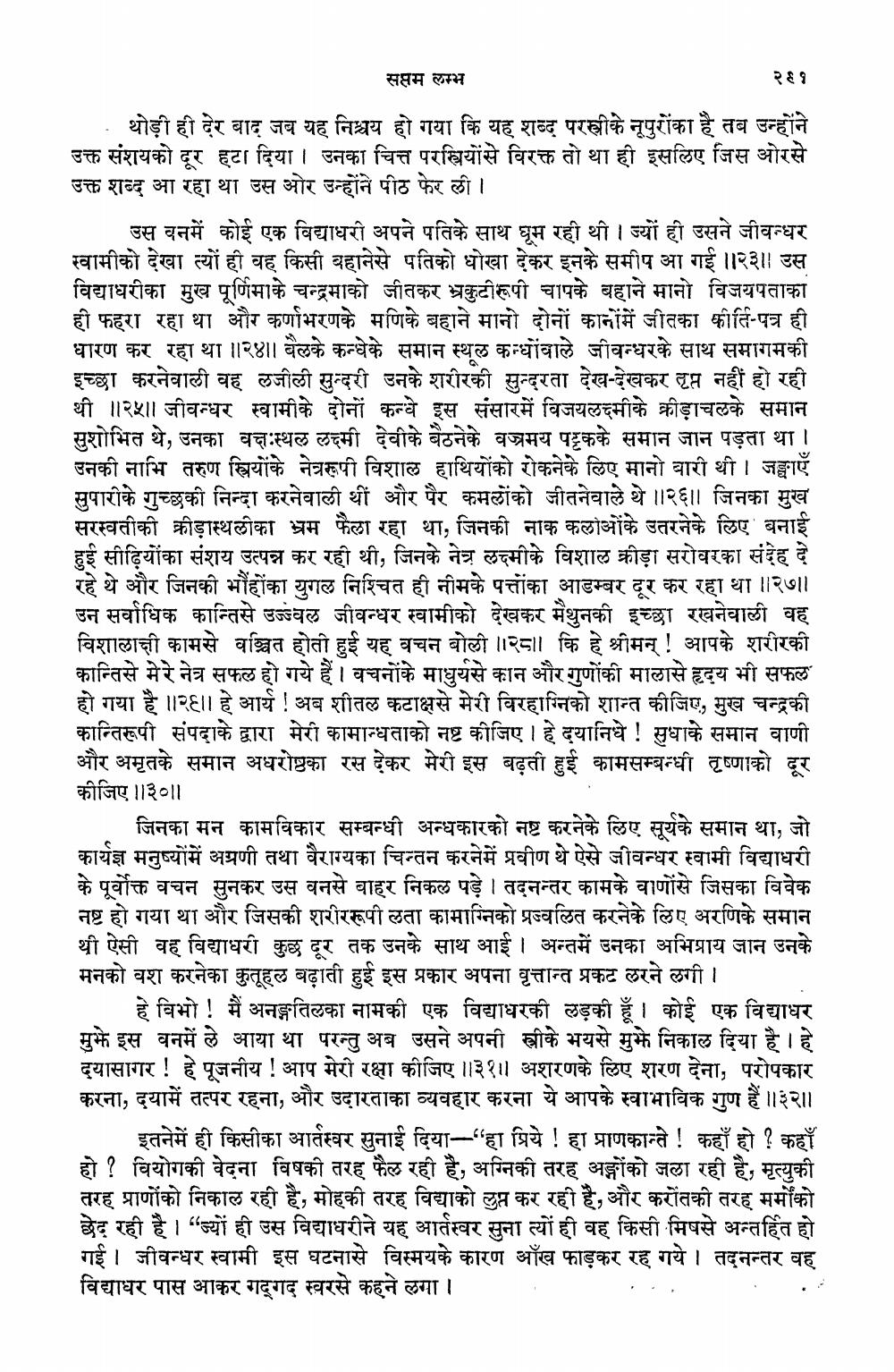________________
सप्तम लम्भ
२६१
थोड़ी ही देर बाद जब यह निश्चय हो गया कि यह शब्द परस्त्रीके नूपुरोंका है तब उन्होंने उक्त संशयको दूर हटा दिया। उनका चित्त परस्त्रियोंसे विरक्त तो था ही इसलिए जिस ओरसे उक्त शब्द आ रहा था उस ओर उन्होंने पीठ फेर ली।
उस वनमें कोई एक विद्याधरी अपने पतिके साथ घूम रही थी। ज्यों ही उसने जीवन्धर स्वामीको देखा त्यों ही वह किसी बहानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गई ॥२३॥ उस विद्याधरीका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको जीतकर भ्रकुटीरूपी चापके बहाने मानो विजयपताका ही फहरा रहा था और कर्णाभरणके मणिके बहाने मानो दोनों कानों में जीतका कीर्ति-पत्र ही धारण कर रहा था ॥२४।। बैलके कन्धेके समान स्थूल कन्धोंवाले जीवन्धरके साथ समागमकी इच्छा करनेवाली वह लजीली सुन्दरी उनके शरीरकी सुन्दरता देख-देखकर तृप्त नहीं हो रही थी ॥२५॥ जीवन्धर स्वामीके दोनों कन्वे इस संसार में विजयलक्ष्मीके क्रीड़ाचलके समान सुशोभित थे, उनका वक्षःस्थल लक्ष्मी देवीके बैठनेके वज्रमय पट्टकके समान जान पड़ता था। उनकी नाभि तरुण स्त्रियोंके नेत्ररूपी विशाल हाथियोंको रोकनेके लिए मानो बारी थी। जवाएँ सुपारीके गुच्छकी निन्दा करनेवाली थीं और पैर कमलोंको जीतनेवाले थे ॥२६।। जिनका मुख सरस्वतीकी क्रीड़ास्थलीका भ्रम फैला रहा था, जिनकी नाक कलोओंके उतरनेके लिए बनाई हुई सीढ़ियोंका संशय उत्पन्न कर रही थी, जिनके नेत्र लक्ष्मीके विशाल क्रीड़ा सरोवरका संदेह दे रहे थे और जिनकी भौंहोंका युगल निश्चित ही नीमके पत्तोंका आडम्बर दूर कर रहा था ॥२७॥ उन सर्वाधिक कान्तिसे उज्ज्वल जीवन्धर स्वामीको देखकर मैथुनकी इच्छा रखनेवाली वह विशालाक्षी कामसे वञ्चित होती हुई यह वचन बोली ॥२८॥ कि हे श्रीमन् ! आपके शरीरकी कान्तिसे मेरे नेत्र सफल हो गये हैं । वचनोंके माधुयसे कान और गुणोंकी मालासे हृदय भी सफल हो गया है ॥२६।। हे आर्य ! अब शीतल कटाक्षसे मेरी विरहाग्निको शान्त कीजिए, मुख चन्द्रकी कान्तिरूपी संपदाके द्वारा मेरी कामान्धताको नष्ट कीजिए । हे दयानिधे ! सुधाके समान वाणी
और अमृतके समान अधरोष्ठका रस देकर मेरी इस बढ़ती हुई कामसम्बन्धी तृष्णाको दूर कीजिए ॥३०॥
जिनका मन कामविकार सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यके समान था, जो कार्यज्ञ मनुष्योंमें अग्रणी तथा वैराग्यका चिन्तन करनेमें प्रवीण थे ऐसे जीवन्धर स्वामी विद्याधरी के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस वनसे बाहर निकल पड़े । तदनन्तर कामके वाणोंसे जिसका विवेक नष्ट हो गया था और जिसकी शरीररूपी लता कामाग्निको प्रज्वलित करनेके लिए अरणिके समान थी ऐसी वह विद्याधरी कुछ दूर तक उनके साथ आई । अन्तमें उनका अभिप्राय जान उनके मनको वश करनेका कुतूहल बढ़ाती हुई इस प्रकार अपना वृत्तान्त प्रकट लरने लगी।
हे विभो ! मैं अनङ्गतिलका नामकी एक विद्याधरकी लड़की हूँ। कोई एक विद्याधर मुझे इस वनमें ले आया था परन्तु अब उसने अपनी स्त्रीके भयसे मुझे निकाल दिया है । हे दयासागर ! हे पूजनीय ! आप मेरी रक्षा कीजिए ॥३१॥ अशरणके लिए शरण देना, परोपकार करना, दयामें तत्पर रहना, और उदारताका व्यवहार करना ये आपके स्वाभाविक गुण हैं ॥३२॥
इतनेमें ही किसीका आर्तस्वर सुनाई दिया-"हा प्रिये ! हा प्राणकान्ते ! कहाँ हो ? कहाँ हो ? वियोगकी वेदना विषकी तरह फैल रही है, अग्निकी तरह अङ्गोंको जला रही है, मृत्युकी तरह प्राणोंको निकाल रही है, मोहकी तरह विद्याको लुप्त कर रही है, और करॊतकी तरह मर्मोको छेद रही है । "ज्यों ही उस विद्याधरीने यह आर्तस्वर सुना त्यों ही वह किसी मिषसे अन्तर्हित हो गई । जीवन्धर स्वामी इस घटनासे विस्मयके कारण आँख फाड़कर रह गये । तदनन्तर वह विद्याधर पास आकर गद्गद स्वरसे कहने लगा।