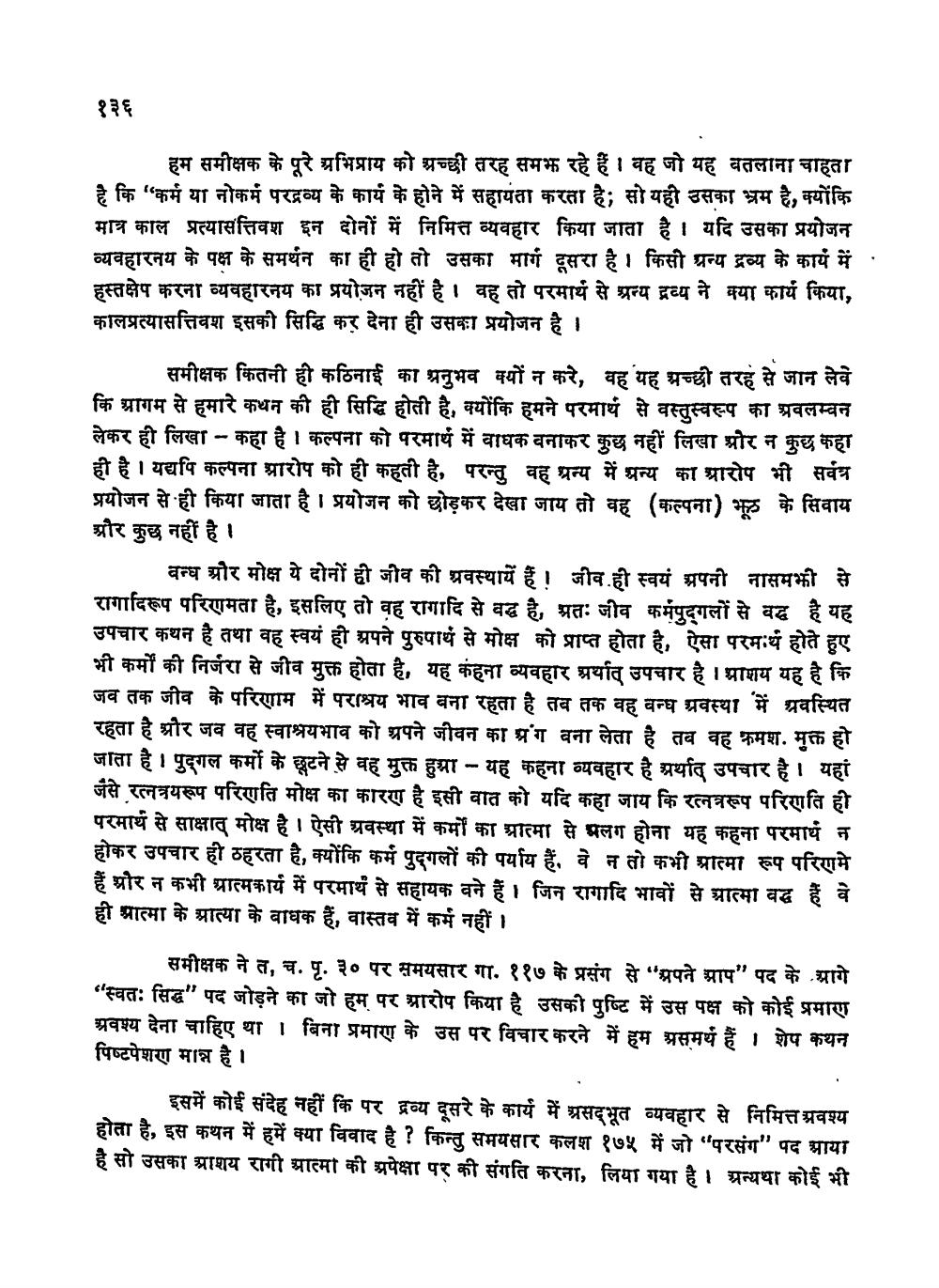________________
१३६
हम समीक्षक के पूरे अभिप्राय को अच्छी तरह समझ रहे हैं । वह जो यह बतलाना चाहता है कि “कर्म या नोकर्म परद्रव्य के कार्य के होने में सहायता करता है; सो यही उसका भ्रम है, क्योंकि मात्र काल प्रत्यासत्तिवश इन दोनों में निमित्त व्यवहार किया जाता है। यदि उसका प्रयोजन व्यवहारनय के पक्ष के समर्थन का ही हो तो उसका मार्ग दूसरा है । किसी ग्रन्थ द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप करना व्यवहारनय का प्रयोजन नहीं है । वह तो परमार्थ से अन्य द्रव्य ने क्या कार्य किया, कालप्रत्यासत्तिवश इसकी सिद्धि कर देना ही उसका प्रयोजन है ।
समीक्षक कितनी ही कठिनाई का अनुभव क्यों न करे, वह यह अच्छी तरह से जान लेवे कि श्रागम से हमारे कथन की ही सिद्धि होती है, क्योंकि हमने परमार्थ से वस्तुस्वरूप का अवलम्वन लेकर ही लिखा - कहा है । कल्पना को परमार्थ में वाधक बनाकर कुछ नहीं लिखा और न कुछ कहा ही है । यद्यपि कल्पना श्रारोप को ही कहती है, परन्तु वह श्रन्य में अन्य का श्रारोप भी सर्वत्र प्रयोजन से ही किया जाता है । प्रयोजन को छोड़कर देखा जाय तो वह (कल्पना) झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है ।
वन्ध और मोक्ष ये दोनों ही जीव की श्रवस्थायें हैं ! जीव ही स्वयं अपनी नासमझी से रागादिरूप परिणमता है, इसलिए तो वह रागादि से वद्ध है, अतः जीव कर्मपुद्गलों से वह है यह उपचार कथन है तथा वह स्वयं ही अपने पुरुषार्थं से मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा परमार्थ होते हुए भी कर्मों की निर्जरा से जीव मुक्त होता है, यह कहना व्यवहार अर्थात् उपचार है । आशय यह है कि जब तक जीव के परिणाम में पराश्रय भाव बना रहता है तब तक वह बन्ध अवस्था में अवस्थित रहता है और जब वह स्वाश्रयभाव को अपने जीवन का अंग बना लेता है तब वह क्रमश. मुक्त हो जाता है। पुद्गल कर्मों के छूटने से वह मुक्त हुन - यह कहना व्यवहार है अर्थात् उपचार है। यहां जैसे रत्नत्रयरूप परिणति मोक्ष का कारण है इसी बात को यदि कहा जाय कि रत्नत्ररूप परिणति ही परमार्थ से साक्षात् मोक्ष है। ऐसी अवस्था में कर्मों का श्रात्मा से अलग होना यह कहना परमार्थं न होकर उपचार ही ठहरता है, क्योंकि कर्म पुद्गलों की पर्याय हैं, वे न तो कभी श्रात्मा रूप परिणमे हैं और न कभी श्रात्मकार्य में परमार्थ से सहायक बने हैं। जिन रागादि भावों से आत्मा वद्ध हैं वे ही आत्मा के प्रात्या के वाधक हैं, वास्तव में कर्म नहीं ।
समीक्षक ने त, च. पू. ३० पर समयसार गा. ११७ के प्रसंग से "अपने आप" पद के आगे "स्वतः सिद्ध" पद जोड़ने का जो हम पर श्रारोप किया है उसकी पुष्टि में उस पक्ष को कोई प्रमाण अवश्य देना चाहिए था । बिना प्रमारण के उस पर विचार करने में हम असमर्थ हैं । शेप कथन पिष्टपेशरण मान्न है |
इसमें कोई संदेह नहीं कि पर द्रव्य दूसरे के कार्य में प्रसद्भूत व्यवहार से निमित्त अवश्य होता है, इस कथन में हमें क्या विवाद है ? किन्तु समयसार कलश १७५ में जो "परसंग" पद आया है सो उसका आशय रागी आत्मा की अपेक्षा पर की संगति करना, लिया गया है । अन्यथा कोई भी