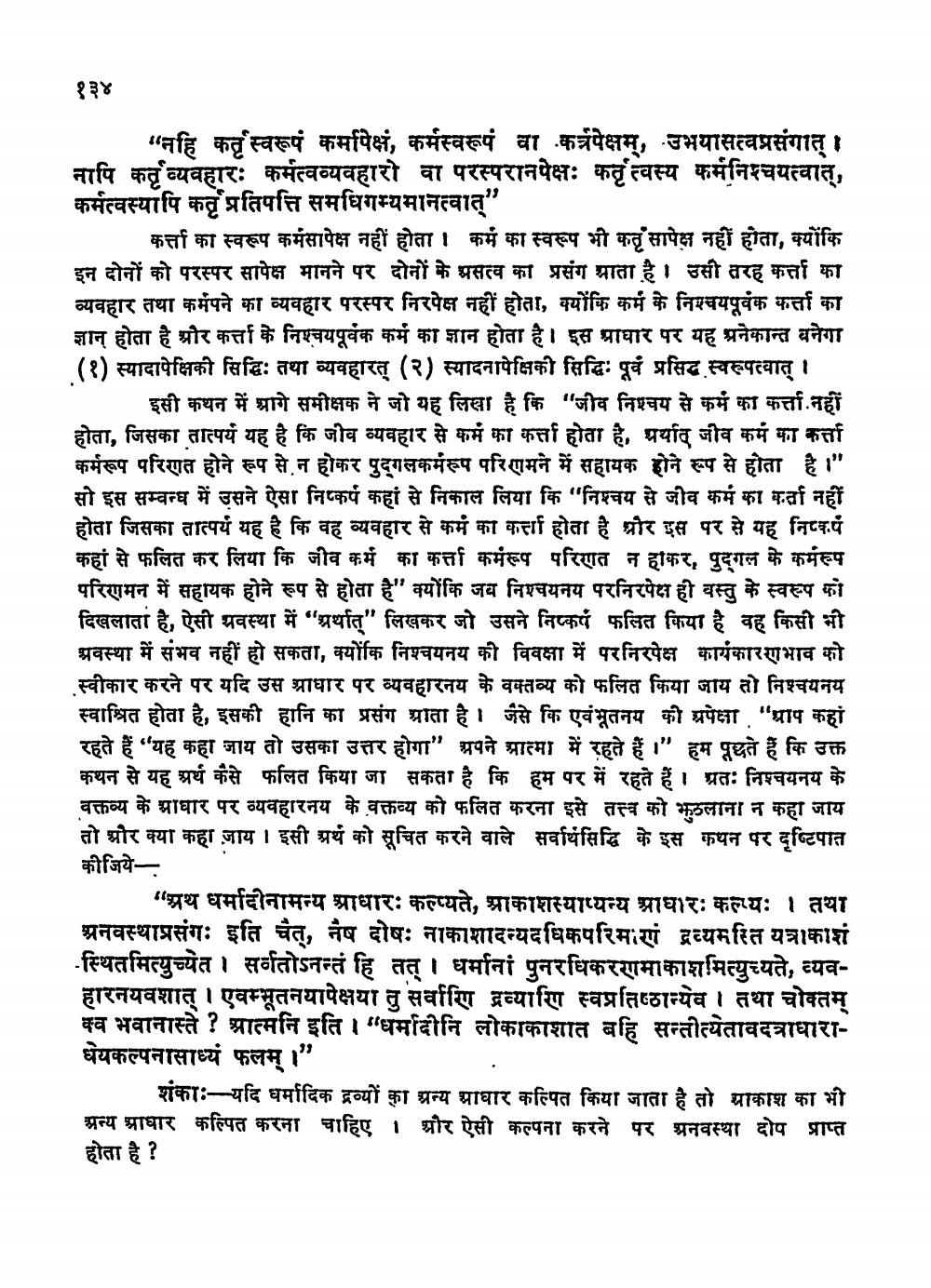________________
१३४
"नहि कर्तृ स्वरूपं कर्मापेक्षं, कर्मस्वरूपं वा कर्त्रपेक्षम्, उभयासत्वप्रसंगात् । नापि कर्तृ व्यवहारः कर्मत्वव्यवहारो वा परस्परानपेक्षः कर्तृत्वस्य कर्मनिश्चयत्वात्, कर्मत्वस्यापि कर्तृ प्रतिपत्ति समधिगम्यमानत्वात्”
कर्त्ता का स्वरूप कर्मसापेक्ष नहीं होता । कर्म का स्वरूप भी कर्तृ सापेक्ष नहीं होता, क्योंकि इन दोनों को परस्पर सापेक्ष मानने पर दोनों के असत्व का प्रसंग श्राता है । उसी तरह कर्ता का व्यवहार तथा कर्मपने का व्यवहार परस्पर निरपेक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्म के निश्चयपूर्वक कर्ता का ज्ञान होता है और कर्त्ता के निश्चयपूर्वक कर्म का ज्ञान होता है। इस प्राधार पर यह श्रनेकान्त बनेगा (१) स्यादापेक्षिकी सिद्धिः तथा व्यवहारत् (२) स्यादनापेक्षिकी सिद्धिः पूर्व प्रसिद्ध स्वरूपत्वात् । इसी कथन में श्रागे समीक्षक ने जो यह लिखा है कि "जीव निश्चय से कर्म का कर्ता नहीं होता, जिसका तात्पर्य यह है कि जीव व्यवहार से कर्म का कर्त्ता होता है, अर्थात् जीव कर्म का कर्ता कर्मरूप परिणत होने रूप से न होकर पुद्गलकर्मरूप परिणमने में सहायक होने रूप से होता है ।" सो इस सम्बन्ध में उसने ऐसा निष्कर्ष कहां से निकाल लिया कि " निश्चय से जीव कर्म का कर्ता नहीं होता जिसका तात्पर्य यह है कि वह व्यवहार से कर्म का कर्ता होता है और इस पर से यह निष्क कहां से फलित कर लिया कि जीव कर्म का कर्ता कर्मरूप परिणत न होकर, पुद्गल के कर्मरूप परिणमन में सहायक होने रूप से होता है" क्योंकि जब निश्चयनय परनिरपेक्ष ही वस्तु स्वरूप की दिखलाता है, ऐसी अवस्था में " अर्थात् " लिखकर जो उसने निष्कर्ष फलित किया है वह किसी भी अवस्था में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चयनय की विवक्षा में परनिरपेक्ष कार्यकारणभाव को . स्वीकार करने पर यदि उस श्राधार पर व्यवहारनय के वक्तव्य को फलित किया जाय तो निश्चयनय स्वाश्रित होता है, इसकी हानि का प्रसंग श्राता है । जैसे कि एवंभूतनय की अपेक्षा "श्राप कहां रहते हैं "यह कहा जाय तो उसका उत्तर होगा" अपने आत्मा में रहते हैं ।" हम पूछते हैं कि उक्त कथन से यह अर्थ कैसे फलित किया जा सकता है कि हम पर में रहते हैं । ग्रतः निश्चयनय के वक्तव्य के आधार पर व्यवहारनय के वक्तव्य को फलित करना इसे तत्त्व को झुठलाना न कहा जाय तो और क्या कहा जाय । इसी अर्थ को सूचित करने वाले सर्वार्थसिद्धि के इस कथन पर दृष्टिपात कीजिये -
*
"अथ धर्मादीनामन्य श्राधारः कल्प्यते, श्राकाशस्याप्यन्य आधारः कल्प्यः । तथा अनवस्थाप्रसंग : इति चेत्, नैष दोषः नाकाशादन्यदधिकपरिमाणं द्रव्यमस्ति यत्राकाशं - स्थित मित्युच्येत | सर्वतोऽनन्तं हि तत् । धर्मानां पुनरधिकरणमाकाश मित्युच्यते, व्यवहारनयवशात् । एवम्भूतनयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्यारिण स्वप्रतिष्ठान्येव । तथा चोक्तम् क्व भवानास्ते ? श्रात्मनि इति । "धर्मादीनि लोकाकाशात बहि सन्तीत्येतावदत्राधाराधेयकल्पनासाध्यं फलम् ।"
शंका: यदि धर्मादिक द्रव्यों का अन्य आधार कल्पित किया जाता है तो श्राकाश का भी अन्य आधार कल्पित करना चाहिए । और ऐसी कल्पना करने पर अनवस्था दोप प्राप्त होता है ?