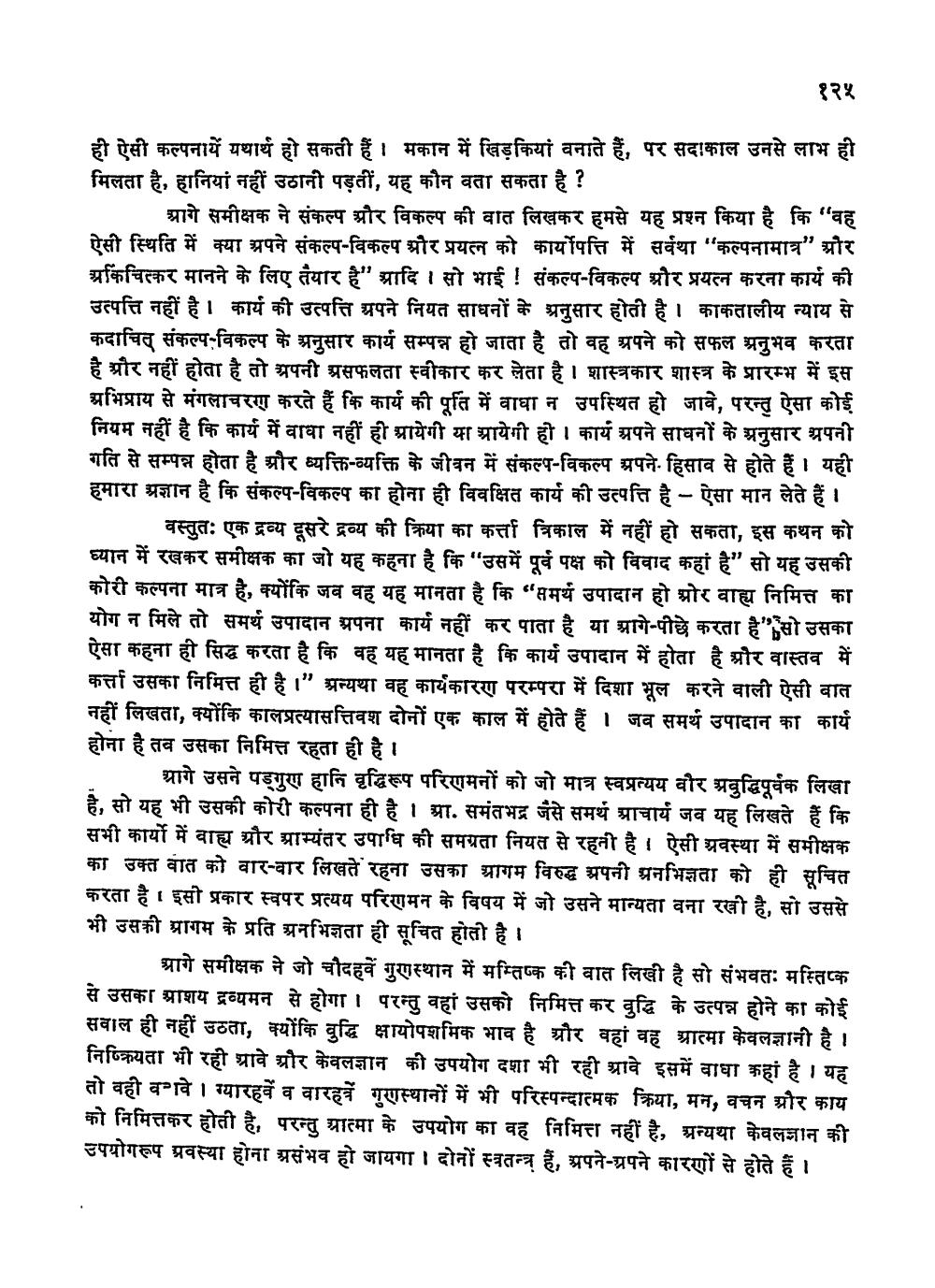________________
१२५
ही ऐसी कल्पनायें यथार्थ हो सकती हैं। मकान में खिड़कियां बनाते हैं, पर सदाकाल उनसे लाभ ही मिलता है, हानियां नहीं उठानी पड़तीं, यह कौन बता सकता है ?
आगे समीक्षक ने संकल्प और विकल्प की बात लिखकर हमसे यह प्रश्न किया है कि "वह ऐसी स्थिति में क्या अपने संकल्प-विकल्प और प्रयत्न को कार्योपत्ति में सर्वथा "कल्पनामात्र" और किंचित्कर मानने के लिए तैयार है" आदि । सो भाई ! संकल्प-विकल्प और प्रयत्न करना कार्य की उत्पत्ति नहीं है । कार्य की उत्पत्ति अपने नियत साधनों के अनुसार होती है । काकतालीय न्याय से कदाचित् संकल्प-विकल्प के अनुसार कार्य सम्पन्न हो जाता है तो वह अपने को सफल अनुभव करता है और नहीं होता है तो अपनी असफलता स्वीकार कर लेता है । शास्त्रकार शास्त्र के प्रारम्भ में इस अभिप्राय से मंगलाचरण करते हैं कि कार्य की पूर्ति में वाघा न उपस्थित हो जावे, परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि कार्य में वावा नहीं ही आयेगी या आयेगी ही । कार्य अपने साधनों के अनुसार अपनी गति से सम्पन्न होता है और व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में संकल्प-विकल्प अपने हिसाव से होते हैं । यही हमारा अज्ञान है कि संकल्प-विकल्प का होना ही विवक्षित कार्य की उत्पत्ति है - ऐसा मान लेते हैं ।
वस्तुत: एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का कर्ता त्रिकाल में नहीं हो सकता, इस कथन को ध्यान में रखकर समीक्षक का जो यह कहना है कि "उसमें पूर्व पक्ष को विवाद कहां है" सो यह उसकी कोरी कल्पना मात्र है, क्योंकि जब वह यह मानता है कि " समर्थ उपादान हो र वाह्य निमित्त का योग न मिले तो समर्थ उपादान अपना कार्य नहीं कर पाता है या आगे-पीछे करता है" सो उसका ऐसा कहना ही सिद्ध करता है कि वह यह मानता है कि कार्य उपादान में होता है और वास्तव में कर्त्ता उसका निमित्त ही है ।" अन्यथा वह कार्यकारण परम्परा में दिशा भूल करने वाली ऐसी बात नहीं लिखता, क्योंकि कालप्रत्यासत्तिवश दोनों एक काल में होते हैं । जब समर्थ उपादान का कार्य होना है तब उसका निमित्त रहता ही है ।
श्रागे उसने पड्गुण हानि वृद्धिरूप परिणमनों को जो मात्र स्वप्रत्यय वीर अबुद्धिपूर्वक लिखा है, सो यह भी उसकी कोरी कल्पना ही है । आ. समंतभद्र जैसे समर्थ प्राचार्य जब यह लिखते हैं कि सभी कार्यो में बाह्य और श्राभ्यंतर उपाधि की समग्रता नियत से रहती है । ऐसी अवस्था में समीक्षक का उक्त वात को बार-बार लिखते रहना उसका ग्रागम विरुद्ध अपनी अनभिज्ञता को ही सूचित करता है । इसी प्रकार स्वपर प्रत्यय परिणमन के विषय में जो उसने मान्यता बना रखी है, सो उससे भी उसकी प्रागम के प्रति अनभिज्ञता ही सूचित होती है ।
प्रागे समीक्षक ने जो चौदहवें गुणस्थान में मस्तिष्क की बात लिखी है सो संभवतः मस्तिष्क से उसका आशय द्रव्यमन से होगा । परन्तु वहां उसको निमित्त कर बुद्धि के उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वुद्धि क्षायोपशमिक भाव है और वहां वह ग्रात्मा केवलज्ञानी है । निष्क्रियता भी रही श्रावे और केवलज्ञान की उपयोग दशा भी रही श्रावे इसमें बाधा कहां है । यह तो वही वगवे । ग्यारहवें व बारहवें गुणस्थानों में भी परिस्पन्दात्मक क्रिया, मन, वचन और काय को निमित्तकर होती है, परन्तु ग्रात्मा के उपयोग का वह निमित्त नहीं है, अन्यथा केवलज्ञान की उपयोगरूप प्रवस्था होना असंभव हो जायगा । दोनों स्वतन्त्र हैं, अपने-अपने कारणों से होते हैं ।