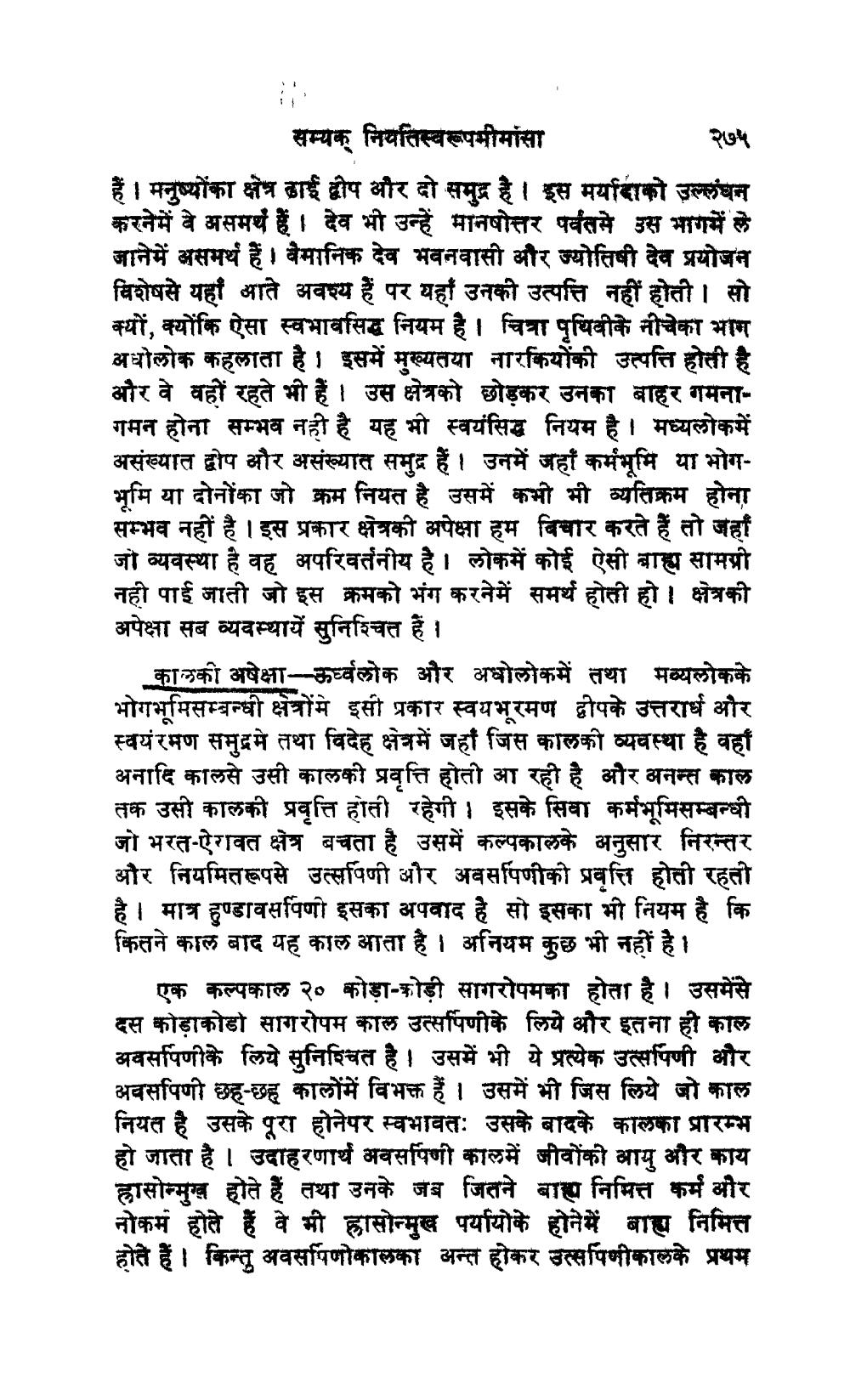________________
२७५
सम्यक् नियतिस्वरूपमीमांसा हैं। मनुष्योंका क्षेत्र ढाई द्वीप और दो समुद्र है। इस मर्यादाको उल्लंघन करने में वे असमर्थ हैं। देव भी उन्हें मानषोत्तर पर्वतसे उस भागमें ले जाने में असमर्थ हैं । वैमानिक देव भवनवासी और ज्योतिषी देव प्रयोजन विशेषसे यहां आते अवश्य हैं पर यहां उनकी उत्पत्ति नहीं होती। सो क्यों, क्योंकि ऐसा स्वभावसिद्ध नियम है। चित्रा पृथिवीके नीचेका भाग अधोलोक कहलाता है। इसमें मुख्यतया नारकियोंकी उत्पत्ति होती है और वे वहीं रहते भी हैं। उस क्षेत्रको छोड़कर उनका बाहर गमनागमन होना सम्भव नही है यह भी स्वयंसिद्ध नियम है। मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उनमें जहाँ कर्मभूमि या भोगभूमि या दोनोंका जो क्रम नियत है उसमें कभी भी व्यतिक्रम होना सम्भव नहीं है । इस प्रकार क्षेत्रकी अपेक्षा हम विचार करते हैं तो जहाँ जो व्यवस्था है वह अपरिवर्तनीय है। लोकमें कोई ऐसी बाह्य सामग्री नही पाई जाती जो इस क्रमको भंग करनेमें समर्थ होती हो। क्षेत्रकी अपेक्षा सब व्यवस्थायें सुनिश्चित हैं ।
कालकी अपेक्षा-कललोक और अधोलोकमें तथा मव्यलोकके भोगभूमिसम्बन्धी क्षेत्रोंमे इसी प्रकार स्वयभूरमण द्वीपके उत्तरार्ध और स्वयंरमण समुद्रमे तथा विदेह क्षेत्र में जहां जिस कालकी व्यवस्था है वहाँ अनादि कालसे उसी कालकी प्रवृत्ति होती आ रही है और अनन्त काल तक उसी कालकी प्रवृत्ति होती रहेगी। इसके सिवा कर्मभूमिसम्बन्धी जो भरत-ऐगवत क्षेत्र बचता है उसमें कल्पकालके अनुसार निरन्तर और नियमितरूपसे उत्सर्पिणी और अवसपिणीको प्रवत्ति होती रहती है। मात्र हुण्डावसर्पिणी इसका अपवाद है सो इसका भी नियम है कि कितने काल बाद यह काल आता है। अनियम कुछ भी नहीं है।
एक कल्पकाल २० कोड़ा-कोड़ी सागरोपमका होता है। उसमेंसे दस कोड़ाकोडो सागरोपम काल उत्सर्पिणीके लिये और इतना ही काल अवसर्पिणीके लिये सुनिश्चित है। उसमें भी ये प्रत्येक उत्सपिणी और अवसपिणी छह-छह कालोंमें विभक्त हैं। उसमें भी जिस लिये जो काल नियत है उसके पूरा होनेपर स्वभावतः उसके बादके कालका प्रारम्भ हो जाता है। उदाहरणार्थ अवसर्पिणी कालमें जीवोंकी आयु और काय हासोन्मुख होते हैं तथा उनके जब जितने बाह्य निमित्त कर्म और नोकर्म होते हैं वे भी ह्रासोन्मुख पर्यायोके होनेमें बाह्य निमित्त होते हैं। किन्तु अवसर्पिणोकालका अन्त होकर उत्सपिणीकालके प्रथम