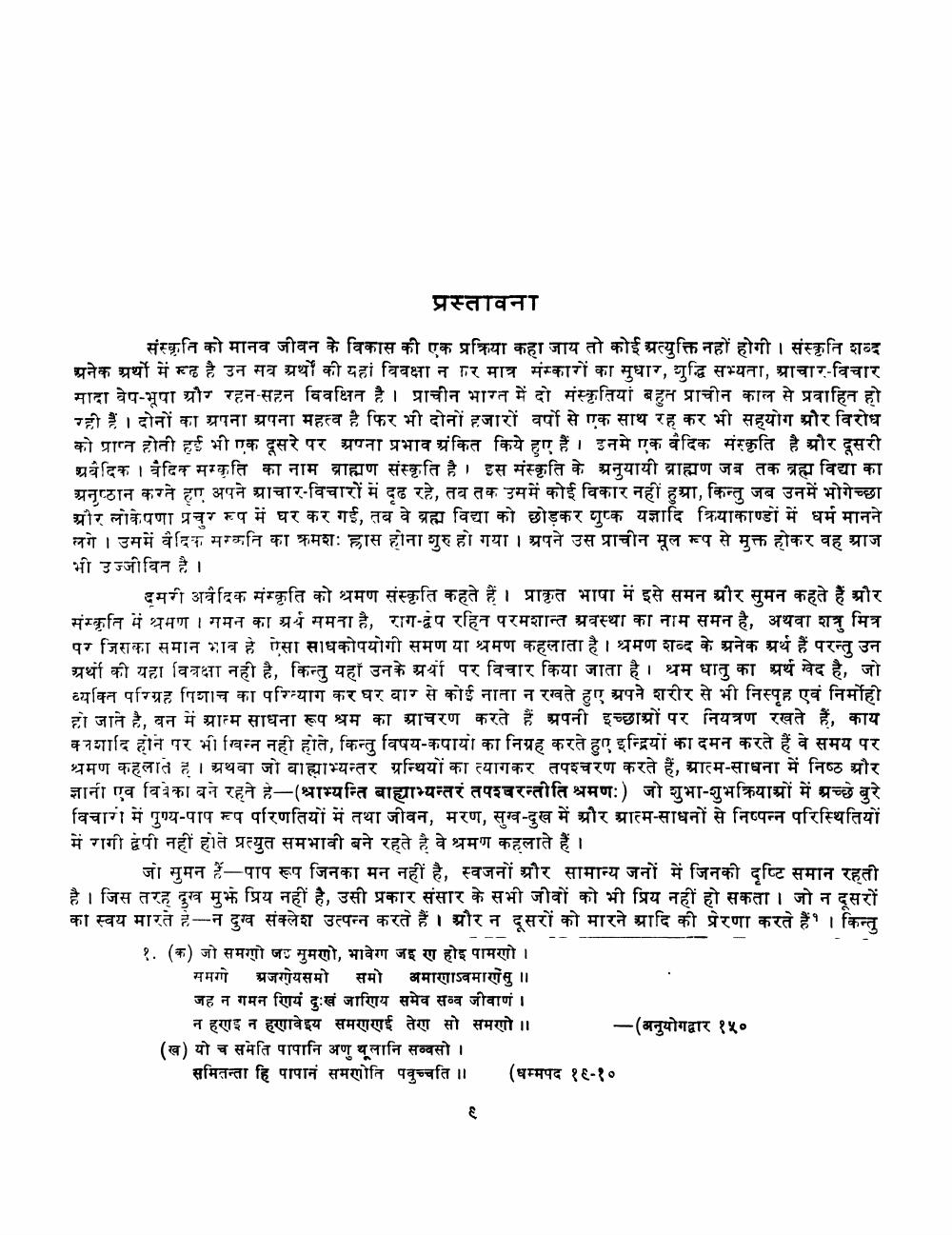________________
प्रस्तावना
संस्कृति को मानव जीवन के विकास की एक प्रक्रिया कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। संस्कृति शब्द अनेक अर्थों में मढ है उन सब अर्थों की यहां विवक्षा न कर मात्र संस्कारों का सुधार, शुद्धि सभ्यता, आचार-विचार मादा वेप-भूपा और रहन-सहन विवक्षित है। प्राचीन भारत में दो संस्कृतियां बहुत प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही है। दोनों का अपना अपना महत्व है फिर भी दोनों हजारों वर्षों से एक साथ रह कर भी सहयोग और विरोध को प्राप्त होती हई भी एक दूसरे पर अपना प्रभाव अंकित किये हए हैं। इनमे एक वैदिक संस्कृति है और दूसरी अवैदिक । वैदिक मस्कृति का नाम ब्राह्मण संस्कृति है। इस मंस्कृति के अनुयायी ब्राह्मण जब तक ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करते हए अपने प्राचार-विचारों में दृढ रहे, तब तक उममें कोई विकार नहीं हुआ, किन्तु जब उनमें भोगेच्छा और लोकेपणा प्रचर रूप में घर कर गई, तब वे ब्रह्म विद्या को छोड़कर गुप्क यज्ञादि क्रियाकाण्डों में धर्म मानने लगे । उममें वैदिक मरकति का क्रमशः ह्रास होना शुरु हो गया। अपने उस प्राचीन मूल रूप से मुक्त होकर वह आज भी उज्जीवित है।
दमरी अवैदिक संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहते हैं। प्राकृत भाषा में इसे समन और सुमन कहते हैं और संस्कृति में श्रमण । गमन का अर्थ ममता है, राग-द्वेप रहित परमशान्त अवस्था का नाम समन है, अथवा शत्रु मित्र पर जिसका समान भाव है ऐसा साधकोपयोगी समण या श्रमण कहलाता है। श्रमण शब्द के अनेक अर्थ हैं परन्तु उन अर्थो की यहा विवक्षा नही है, किन्तु यहाँ उनके प्रों पर विचार किया जाता है। श्रम धातु का अर्थ ग्वेद है, जो व्यक्ति परिग्रह पिगाच का परित्याग कर घर वार से कोई नाता न रखते हुए अपने शरीर से भी निस्पृह एवं निर्मोही हो जाते है, वन में प्रात्म साधना रूप श्रम का आचरण करते हैं अपनी इच्छाओं पर नियत्रण रखते हैं, काय कनगादि होने पर भी खिन्न नही होते, किन्तु विषय-कपायो का निग्रह करते हुए इन्द्रियों का दमन करते हैं वे समय पर श्रमण कहलाते है । अथवा जो बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थियों का त्यागकर तपश्चरण करते हैं, आत्म-साधना में निष्ठ और ज्ञानी एव विवेका बने रहते है-(श्राभ्यन्ति बाह्याभ्यन्तरं तपश्चरन्तीति श्रमणः) जो शुभा-शुभक्रियाओं में अच्छे बुरे विचाग में पुण्य-पाप रूप परिणतियों में तथा जीवन, मरण, सुख-दुख में और आत्म-साधनों से निष्पन्न परिस्थितियों में रागी द्वपी नहीं होते प्रत्युत समभावी बने रहते है वे श्रमण कहलाते हैं।
जो मुमन हैं-पाप रूप जिनका मन नहीं है, स्वजनों और सामान्य जनों में जिनकी दृष्टि समान रहती है। जिस तरह दुख मुझे प्रिय नहीं है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवों को भी प्रिय नहीं हो सकता। जो न दसरों का स्वय मारते हे-न दुग्ख संक्लेश उत्पन्न करते हैं। और न दूसरों को मारने आदि की प्रेरणा करते हैं । किन्तु
१. (क) जो समगो जमुमणो, भावेण जइ ण होइ पामणो ।
ममगगे अजणेयसमो समो अमाणाऽवमाणेसु ।। जह न गमन णियं दुःखं जारिणय समेव सव्व जीवाणं । न हणइ न हणावेइय समणगई तेण सो समणो ।।
-(अनुयोगद्वार १५० (ख) यो च समेति पापानि अणु थूलानि सव्वसो ।
समितन्ता हि पापानं समणोति पवुच्चति ॥ (धम्मपद १६-१०