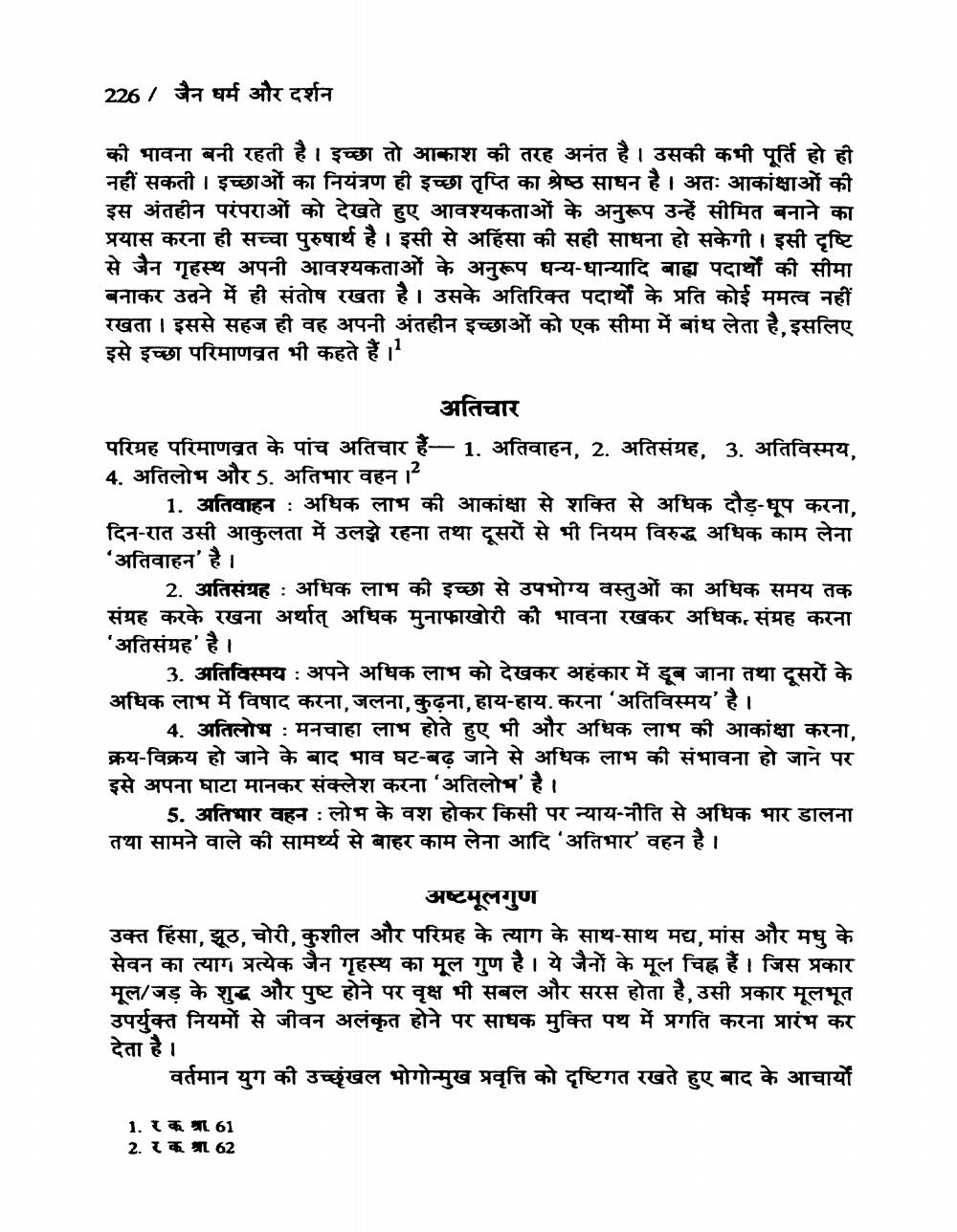________________
226/ जैन धर्म और दर्शन
की भावना बनी रहती है । इच्छा तो आकाश की तरह अनंत है। उसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती । इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा तृप्ति का श्रेष्ठ साधन है। अतः आकांक्षाओं की इस अंतहीन परंपराओं को देखते हुए आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें सीमित बनाने का प्रयास करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। इसी से अहिंसा की सही साधना हो सकेगी। इसी दृष्टि से जैन गहस्थ अपनी आवश्यकताओं के अनरूप धन्य-धान्यादि बाह्य पदार्थों की सीमा बनाकर उतने में ही संतोष रखता है। उसके अतिरिक्त पदार्थों के प्रति कोई ममत्व नहीं रखता । इससे सहज ही वह अपनी अंतहीन इच्छाओं को एक सीमा में बांध लेता है, इसलिए इसे इच्छा परिमाणवत भी कहते हैं।
अतिचार परिग्रह परिमाणवत के पांच अतिचार हैं- 1. अतिवाहन, 2. अतिसंग्रह, 3. अतिविस्मय, 4. अतिलोभ और 5. अतिभार वहन ।
1. अतिवाहन : अधिक लाभ की आकांक्षा से शक्ति से अधिक दौड़-धूप करना, दिन-रात उसी आकुलता में उलझे रहना तथा दूसरों से भी नियम विरुद्ध अधिक काम लेना 'अतिवाहन' है।
2. अतिसंग्रह : अधिक लाभ की इच्छा से उपभोग्य वस्तुओं का अधिक समय तक संग्रह करके रखना अर्थात् अधिक मुनाफाखोरी को भावना रखकर अधिक, संग्रह करना 'अतिसंग्रह है।
. अतिविस्मय : अपने अधिक लाभ को देखकर अहंकार में डूब जाना तथा दूसरों के अधिक लाभ में विषाद करना,जलना,कुढ़ना, हाय-हाय. करना अतिविस्मय' है।
4. अतिलोभ : मनचाहा लाभ होते हुए भी और अधिक लाभ की आकांक्षा करना, क्रय-विक्रय हो जाने के बाद भाव घट-बढ़ जाने से अधिक लाभ की संभावना हो जाने पर इसे अपना घाटा मानकर संक्लेश करना 'अतिलोभ' है।
5. अतिभार वहन : लोभ के वश होकर किसी पर न्याय-नीति से अधिक भार डालना तथा सामने वाले की सामर्थ्य से बाहर काम लेना आदि 'अतिभार वहन है।
अष्टमूलगुण उक्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के त्याग के साथ-साथ मद्य, मांस और मधु के सेवन का त्याग प्रत्येक जैन गृहस्थ का मूल गुण है। ये जैनों के मूल चिह्न हैं। जिस प्रकार मूल/जड़ के शुद्ध और पुष्ट होने पर वृक्ष भी सबल और सरस होता है, उसी प्रकार मूलभूत उपर्युक्त नियमों से जीवन अलंकृत होने पर साधक मुक्ति पथ में प्रगति करना प्रारंभ कर देता है। ___ वर्तमान युग की उच्छंखल भोगोन्मुख प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए बाद के आचार्यों
1.र कश्रा61 2. रकबा 62