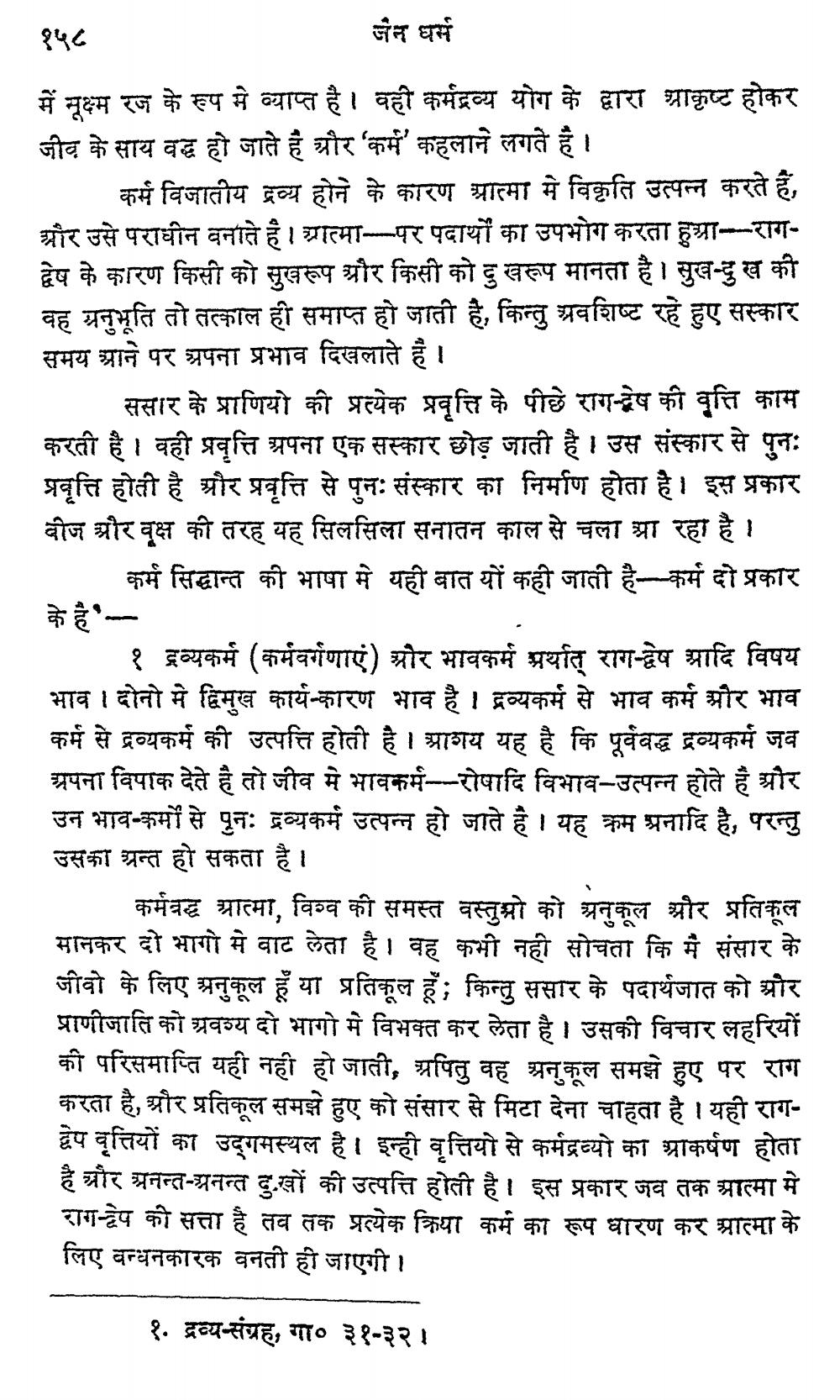________________
१५८
जैन धर्म
में मूक्ष्म रज के रूप में व्याप्त है। वही कर्मद्रव्य योग के द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ बद्ध हो जाते है और 'कर्म' कहलाने लगते है।
कर्म विजातीय द्रव्य होने के कारण आत्मा मे विकृति उत्पन्न करते हैं, और उसे पराधीन बनाते है । प्रात्मा-पर पदार्थों का उपभोग करता हुआ-रागद्वेष के कारण किसी को सुखरूप और किसी को दुखरूप मानता है। सुख-दुख की वह अनुभूति तो तत्काल ही समाप्त हो जाती है, किन्तु अवशिष्ट रहे हुए सस्कार समय आने पर अपना प्रभाव दिखलाते है ।
ससार के प्राणियो की प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे राग-द्वेष की वृत्ति काम करती है । वही प्रवृत्ति अपना एक सस्कार छोड़ जाती है । उस संस्कार से पुनः प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से पुनः संस्कार का निर्माण होता है। इस प्रकार वीज और वृक्ष की तरह यह सिलसिला सनातन काल से चला आ रहा है।
कर्म सिद्धान्त की भाषा मे यही बात यों कही जाती है-कर्म दो प्रकार के है'
१ द्रव्यकर्म (कर्मवर्गणाएं) और भावकर्म अर्थात् राग-द्वेष आदि विषय भाव । दोनो मे द्विमुख कार्य-कारण भाव है । द्रव्यकर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्यकर्म की उत्पत्ति होती है । आशय यह है कि पूर्ववद्ध द्रव्यकर्म जब अपना विपाक देते है तो जीव मे भावकर्म-रोषादि विभाव-उत्पन्न होते है और उन भाव-कर्मों से पुनः द्रव्यकर्म उत्पन्न हो जाते है। यह क्रम अनादि है, परन्तु उसका अन्त हो सकता है।
कर्मबद्ध आत्मा, विश्व की समस्त वस्तुओ को अनुकूल और प्रतिकूल मानकर दो भागो मे बाट लेता है। वह कभी नही सोचता कि मै संसार के जीवो के लिए अनुकूल हूँ या प्रतिकूल हूँ; किन्तु ससार के पदार्थजात को और प्राणीजाति को अवश्य दो भागो में विभक्त कर लेता है। उसकी विचार लहरियों की परिसमाप्ति यही नहीं हो जाती, अपितु वह अनुकूल समझे हुए पर राग करता है, और प्रतिकूल समझे हुए को संसार से मिटा देना चाहता है । यही रागद्वेप वृत्तियों का उद्गमस्थल है। इन्ही वृत्तियो से कर्मद्रव्यो का आकर्षण होता है और अनन्त-अनन्त दुःखों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जब तक आत्मा मे राग-द्वेप की सत्ता है तब तक प्रत्येक क्रिया कर्म का रूप धारण कर आत्मा के लिए वन्धनकारक वनती ही जाएगी।
१. द्रव्य-संग्रह, गा० ३१-३२॥