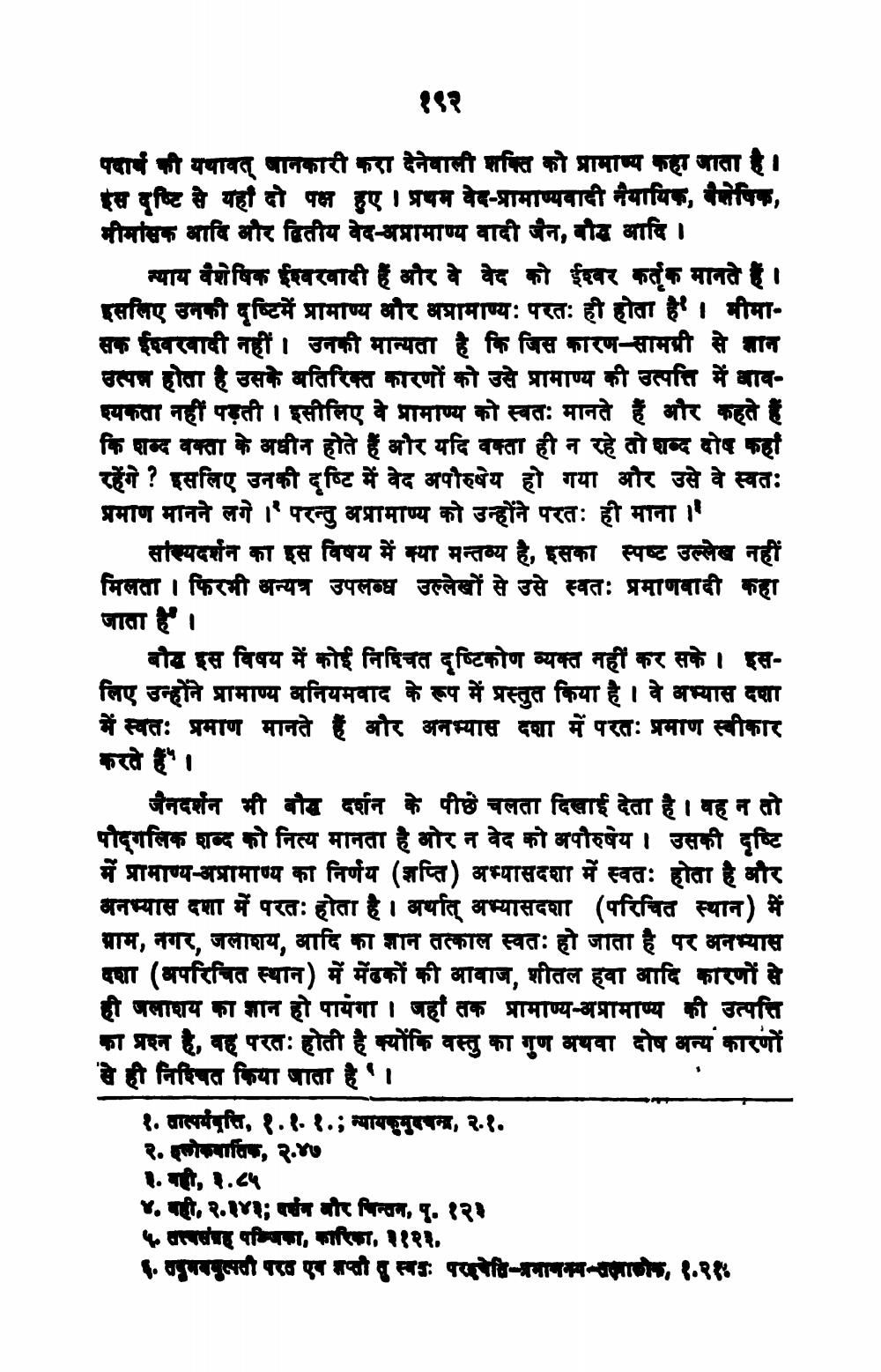________________
पदार्थ की यथावत् पानकारी करा देनेवाली शक्ति को प्रामाण्य कहा जाता है। इस दृष्टि से यहाँ दो पक्ष हुए । प्रथम वेद-प्रामाण्यवादी नैयायिक, बोषिक, मीमांसक मावि और द्वितीय वेद-अप्रामाण्य वादी जैन, बौर आदि ।
न्याय वैशेषिक ईश्वरवादी है और वे वेद को ईश्वर कर्तृक मानते हैं। इसलिए उनकी दृष्टिमें प्रामाण्य और अप्रामाण्यः परतः ही होता है। मीमासक ईश्वरवादी नहीं। उनकी मान्यता है कि जिस कारण-सामग्री से मान उत्पन्न होता है उसके बतिरिक्त कारणों को उसे प्रामाण्य की उत्पत्ति में बावश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए वे प्रामाण्य को स्वतः मानते हैं और कहते हैं कि शब्द वक्ता के अधीन होते हैं और यदि वक्ता ही न रहे तो शब्द दोष कहाँ रहेंगे? इसलिए उनकी दष्टि में वेद अपौरुषेय हो गया और उसे वे स्वतः प्रमाण मानने लगे। परन्तु अप्रामाण्य को उन्होंने परतः ही माना।।
सांस्यदर्शन का इस विषय में क्या मन्तव्य है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । फिरभी अन्यत्र उपलब्ध उल्लेखों से उसे स्वतः प्रमाणवादी कहा जाता है।
बौर इस विषय में कोई निश्चित दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने प्रामाण्य अनियमवाद के रूप में प्रस्तुत किया है । वे अभ्यास दशा में स्वतः प्रमाण मानते हैं और अनभ्यास दशा में परतः प्रमाण स्वीकार करते हैं।
जैनदर्शन भी बौद्ध दर्शन के पीछे चलता दिखाई देता है । वह न तो पोद्गलिक शब्द को नित्य मानता है बोर न वेद को अपौरुषेय । उसकी दृष्टि में प्रामाण्य-अप्रामाण्य का निर्णय (शप्ति) अभ्यासदशा में स्वतः होता है और अनभ्यास दशा में परतः होता है। अर्थात् अभ्यासदशा (परिचित स्थान) में ग्राम, नगर, जलाशय, आदि का ज्ञान तत्काल स्वतः हो जाता है पर अनभ्यास दशा (अपरिचित स्थान) में मेंढकों की आवाज, शीतल हवा आदि कारणों से ही जलाशय का ज्ञान हो पायंगा। जहां तक प्रामाण्य-अप्रामाण्य की उत्पत्ति का प्रश्न है, वह परतः होती है क्योंकि वस्तु का गुण अथवा दोष अन्य कारणों से ही निश्चित किया जाता है।
१. वात्पत्ति , १.१.१.; न्यायमुरुषमा, २.१. २. इलोकपातिक, २.७ ..बही१.८५ ४.ही.२. पन बीर चिन्तन, पृ. १२३
संबह पम्बिनकारिका, ११२१, नवयुल्लती परत एप सप्ती स्वरः पयरेकि-मानस-पास १.२१९
-
-