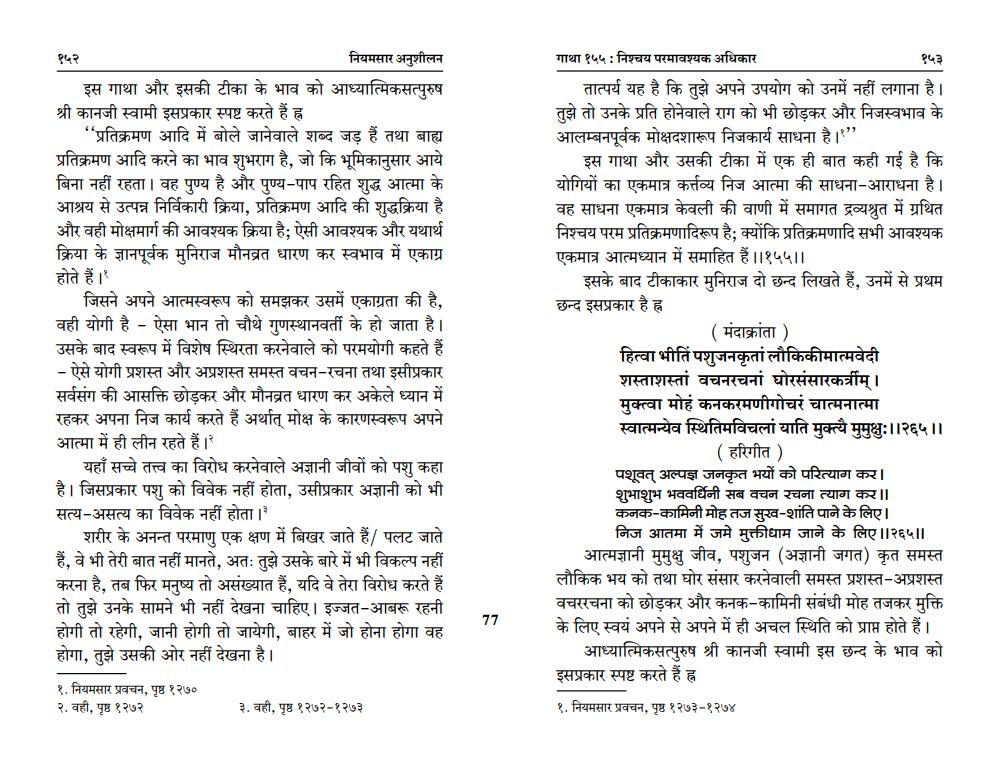________________
नियमसार अनुशीलन
इस गाथा और इसकी टीका के भाव को आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
" प्रतिक्रमण आदि में बोले जानेवाले शब्द जड़ हैं तथा बाह्य प्रतिक्रमण आदि करने का भाव शुभराग है, जो कि भूमिकानुसार आये बिना नहीं रहता। वह पुण्य है और पुण्य-पाप रहित शुद्ध आत्मा के आश्रय से उत्पन्न निर्विकारी क्रिया, प्रतिक्रमण आदि की शुद्धक्रिया है और वही मोक्षमार्ग की आवश्यक क्रिया है; ऐसी आवश्यक और यथार्थ क्रिया के ज्ञानपूर्वक मुनिराज मौनव्रत धारण कर स्वभाव में एकाग्र होते हैं।
जिसने अपने आत्मस्वरूप को समझकर उसमें एकाग्रता की है, वही योगी है - ऐसा भान तो चौथे गुणस्थानवर्ती के हो जाता है। उसके बाद स्वरूप में विशेष स्थिरता करनेवाले को परमयोगी कहते हैं ऐसे योगी प्रशस्त और अप्रशस्त समस्त वचन - रचना तथा इसीप्रकार सर्वसंग की आसक्ति छोड़कर और मौनव्रत धारण कर अकेले ध्यान में रहकर अपना निज कार्य करते हैं अर्थात् मोक्ष के कारणस्वरूप अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं।
१५२
-
यहाँ सच्चे तत्त्व का विरोध करनेवाले अज्ञानी जीवों को पशु कहा है। जिसप्रकार पशु को विवेक नहीं होता, उसीप्रकार अज्ञानी को भी सत्य-असत्य का विवेक नहीं होता।
शरीर के अनन्त परमाणु एक क्षण में बिखर जाते हैं / पलट जाते हैं, वे भी तेरी बात नहीं मानते, अतः तुझे उसके बारे में भी विकल्प नहीं करना है, तब फिर मनुष्य तो असंख्यात हैं, यदि वे तेरा विरोध करते हैं तो तुझे उनके सामने भी नहीं देखना चाहिए। इज्जत - आबरू रहनी होगी तो रहेगी, जानी होगी तो जायेगी, बाहर में जो होना होगा वह होगा, तुझे उसकी ओर नहीं देखना है ।
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १२७० २. वही, पृष्ठ १२७२
३. वही, पृष्ठ १२७२- १२७३
77
गाथा १५५ : निश्चय परमावश्यक अधिकार
१५३
तात्पर्य यह है कि तुझे अपने उपयोग को उनमें नहीं लगाना है। तुझे तो उनके प्रति होनेवाले राग को भी छोड़कर और निजस्वभाव के आलम्बनपूर्वक मोक्षदशारूप निजकार्य साधना है। "
इस गाथा और उसकी टीका में एक ही बात कही गई है कि योगियों का एकमात्र कर्तव्य निज आत्मा की साधना-आराधना है । वह साधना एकमात्र केवली की वाणी में समागत द्रव्यश्रुत में ग्रथित निश्चय परम प्रतिक्रमणादिरूप है; क्योंकि प्रतिक्रमणादि सभी आवश्यक एकमात्र आत्मध्यान में समाहित हैं ।। १५५ ।।
इसके बाद टीकाकार मुनिराज दो छन्द लिखते हैं, उनमें से प्रथम छन्द इसप्रकार है
( मंदाक्रांता )
हित्वा भीतिं पशुजनकृतां लौकिकीमात्मवेदी शस्ताशस्तां वचनरचनां घोरसंसारकर्त्रीम् । मुक्त्वा मोहं कनकरमणीगोचरं चात्मनात्मा स्वात्मन्येव स्थितिमविचलां याति मुक्त्यै मुमुक्षुः ।। २६५ ।। ( हरिगीत )
पशूवत् अल्पज्ञ जनकृत भयों को परित्याग कर । शुभाशुभ भववर्धिनी सब वचन रचना त्याग कर ॥ कनक कामिनी मोह तज सुख-शांति पाने के लिए । निज आतमा में जमे मुक्तीधाम जाने के लिए || २६५ || आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव, पशुजन (अज्ञानी जगत) कृत समस्त लौकिक भय को तथा घोर संसार करनेवाली समस्त प्रशस्त अप्रशस्त वचररचना को छोड़कर और कनक कामिनी संबंधी मोह तजकर मुक्ति के लिए स्वयं अपने से अपने में ही अचल स्थिति को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस छन्द के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १२७३-१२७४