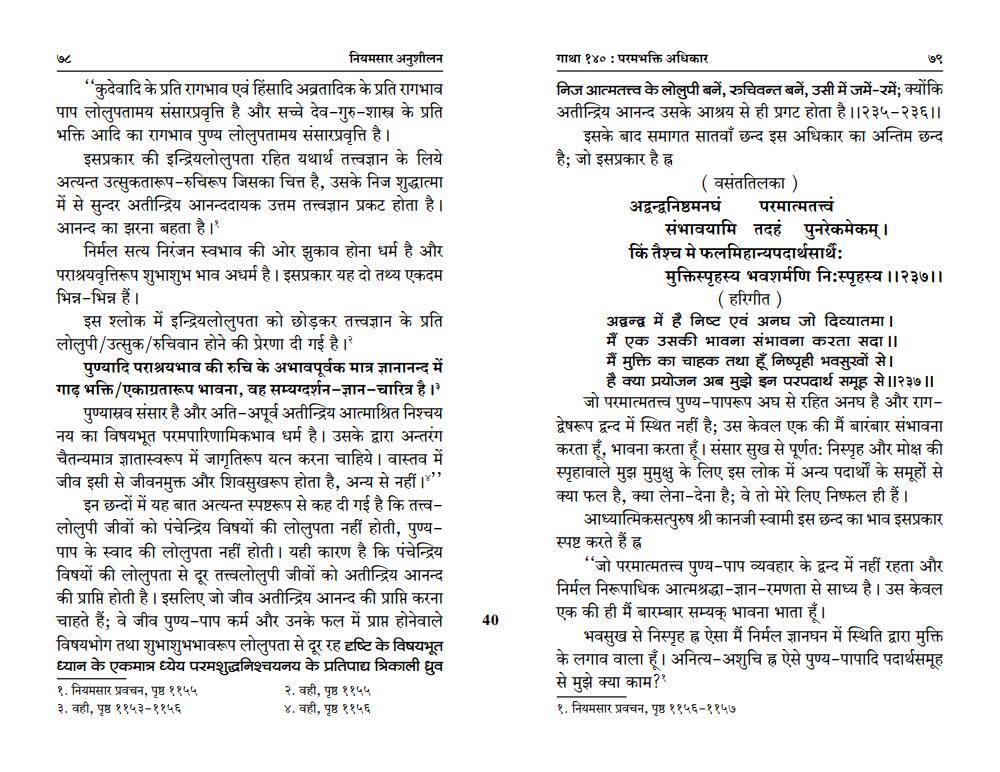________________
नियमसार अनुशीलन
“कुदेवादि के प्रति रागभाव एवं हिंसादि अव्रतादिक के प्रति रागभाव पाप लोलुपतामय संसारप्रवृत्ति है और सच्चे देव - गुरु-शास्त्र के प्रति भक्ति आदि का रागभाव पुण्य लोलुपतामय संसारप्रवृत्ति है ।
इसप्रकार की इन्द्रियलोलुपता रहित यथार्थ तत्त्वज्ञान के लिये अत्यन्त उत्सुकतारूप-रुचिरूप जिसका चित्त है, उसके निज शुद्धात्मा में से सुन्दर अतीन्द्रिय आनन्ददायक उत्तम तत्त्वज्ञान प्रकट होता है । आनन्द का झरना बहता है।"
निर्मल सत्य निरंजन स्वभाव की ओर झुकाव होना धर्म है और पराश्रयवृत्तिरूप शुभाशुभ भाव अधर्म है। इसप्रकार यह दो तथ्य एकदम भिन्न-भिन्न हैं।
७८
इस श्लोक में इन्द्रियलोलुपता को छोड़कर तत्त्वज्ञान के प्रति लोलुपी / उत्सुक / रुचिवान होने की प्रेरणा दी गई है।
पुण्यादि पराश्रयभाव की रुचि के अभावपूर्वक मात्र ज्ञानानन्द में गाढ़ भक्ति / एकाग्रतारूप भावना, वह सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र है ।"
पुण्यास्रव संसार है और अति-अपूर्व अतीन्द्रिय आत्माश्रित निश्चय नय का विषयभूत परमपारिणामिकभाव धर्म है। उसके द्वारा अन्तरंग चैतन्यमात्र ज्ञातास्वरूप में जागृतिरूप यत्न करना चाहिये । वास्तव में जीव इसी से जीवनमुक्त और शिवसुखरूप होता है, अन्य से नहीं । ४"
इन छन्दों में यह बात अत्यन्त स्पष्टरूप से कह दी गई है कि तत्त्वलोलुपी जीवों को पंचेन्द्रिय विषयों की लोलुपता नहीं होती, पुण्यपाप के स्वाद की लोलुपता नहीं होती। यही कारण है कि पंचेन्द्रिय विषयों की लोलुपता से दूर तत्त्वलोलुपी जीवों को अतीन्द्रिय आनन्द की प्राप्ति होती है। इसलिए जो जीव अतीन्द्रिय आनन्द की प्राप्ति करना चाहते हैं; वे जीव पुण्य-पाप कर्म और उनके फल में प्राप्त होनेवाले विषयभोग तथा शुभाशुभभावरूप लोलुपता से दूर रह दृष्टि के विषयभूत ध्यान के एकमात्र ध्येय परमशुद्धनिश्चयनय के प्रतिपाद्य त्रिकाली ध्रुव
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ ११५५ ३. वही, पृष्ठ १९५३ - ११५६
२. वही, पृष्ठ ११५५
४. वही, पृष्ठ १९५६
40
गाथा १४० : परमभक्ति अधिकार
७९
निज आत्मतत्त्व के लोलुपी बनें, रुचिवन्त बनें, उसी में जमें-रमें; क्योंकि अतीन्द्रिय आनन्द उसके आश्रय से ही प्रगट होता है ।। २३५-२३६ ।। इसके बाद समागत सातवाँ छन्द इस अधिकार का अन्तिम छन्द है; जो इसप्रकार है ह्र
( वसंततिलका ) अद्वन्द्वनिष्ठमनघं परमात्मतत्त्वं
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम् । किं तैश्च मे फलमिहान्यपदार्थसार्थैः
मुक्तिस्पृहस्य भवशर्मणि नि:स्पृहस्य ।। २३७ ।। ( हरिगीत )
अद्वन्द्व में है निष्ट एवं अनघ जो दिव्यातमा । मैं एक उसकी भावना संभावना करता सदा ॥ मैं मुक्ति का चाहक तथा हूँ निष्पृही भवसुखों से । है क्या प्रयोजन अब मुझे इन परपदार्थ समूह से || २३७ ॥ जो परमात्मतत्त्व पुण्य-पापरूप अघ से रहित अनघ है और रागद्वेषरूप द्वन्द में स्थित नहीं है; उस केवल एक की मैं बारंबार संभावना करता हूँ, भावना करता हूँ। संसार सुख से पूर्णत: निस्पृह और मोक्ष की स्पृहावाले मुझ मुमुक्षु के लिए इस लोक में अन्य पदार्थों के समूहों से क्या फल है, क्या लेना-देना है; वे तो मेरे लिए निष्फल ही हैं।
आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस छन्द का भाव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
"जो परमात्मतत्त्व पुण्य-पाप व्यवहार के द्वन्द में नहीं रहता और निर्मल निरूपाधिक आत्मश्रद्धा-ज्ञान- रमणता से साध्य है । उस केवल एक की ही मैं बारम्बार सम्यक् भावना भाता हूँ ।
भवसुख से निस्पृह ह्न ऐसा मैं निर्मल ज्ञानघन में स्थिति द्वारा के लगाव वाला हूँ। अनित्य-अशुचि ह्र ऐसे पुण्य-पापादि पदार्थसमूह से मुझे क्या काम ??
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ ११५६-११५७