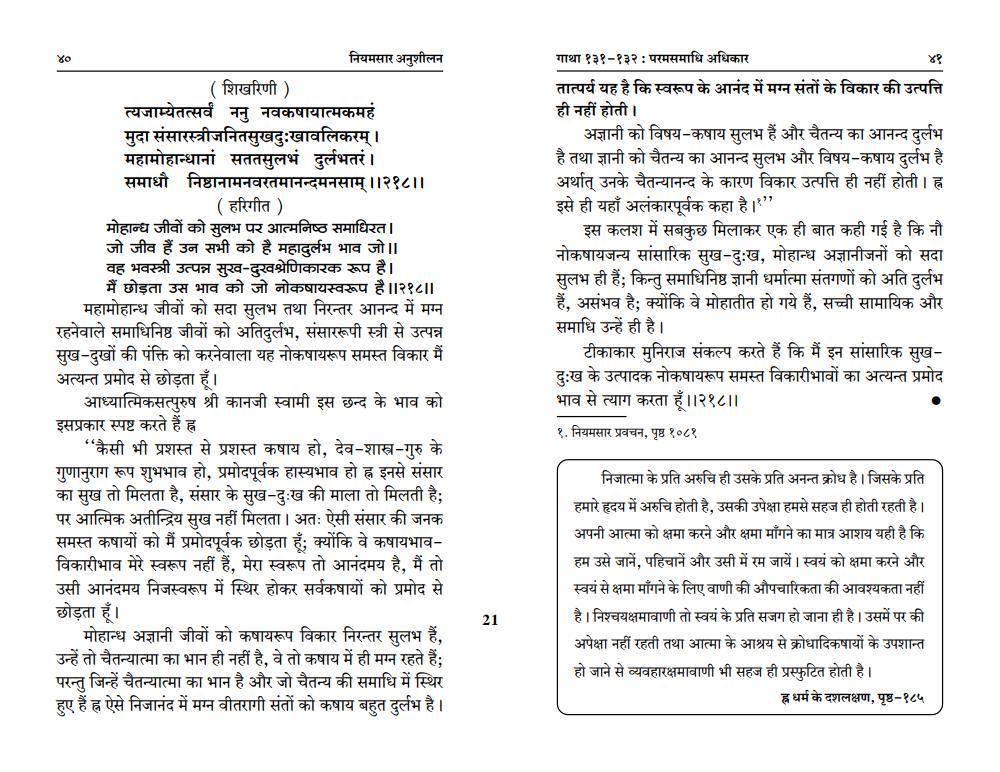________________
४०
नियमसार अनुशीलन
( शिखरिणी )
त्यजाम्येतत्सर्वं ननु नवकषायात्मकमहं मुदा संसारस्त्रीजनितसुखदुःखावलिकरम् । महामोहान्धानां सततसुलभं दुर्लभतरं । समाधौ निष्ठानामनवरतमानन्दमनसाम् ।।२१८ । । ( हरिगीत )
मोहान्ध जीवों को सुलभ पर आत्मनिष्ठ समाधिरत । जो जीव हैं उन सभी को है महादुर्लभ भाव जो ॥ वह भवस्त्री उत्पन्न सुख-दुखश्रेणिकारक रूप है। मैं छोड़ता उस भाव को जो नोकषायस्वरूप है || २१८|| महामोहान्ध जीवों को सदा सुलभ तथा निरन्तर आनन्द में मग्न रहनेवाले समाधिनिष्ठ जीवों को अतिदुर्लभ, संसाररूपी स्त्री से उत्पन्न सुख-दुखों की पंक्ति को करनेवाला यह नोकषायरूप समस्त विकार मैं अत्यन्त प्रमोद से छोड़ता हूँ।
आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस छन्द के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्न
"कैसी भी प्रशस्त से प्रशस्त कषाय हो, देव-शास्त्र-गुरु के गुणानुराग रूप शुभभाव हो, प्रमोदपूर्वक हास्यभाव हो ह्र इनसे संसार का सुख तो मिलता है, संसार के सुख-दुःख की माला तो मिलती है; पर आत्मिक अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता। अतः ऐसी संसार की जनक समस्त कषायों को मैं प्रमोदपूर्वक छोड़ता हूँ; क्योंकि वे कषायभावविकारीभाव मेरे स्वरूप नहीं हैं, मेरा स्वरूप तो आनंदमय है, मैं तो उसी आनंदमय निजस्वरूप में स्थिर होकर सर्वकषायों को प्रमोद से छोड़ता हूँ।
मोहान्ध अज्ञानी जीवों को कषायरूप विकार निरन्तर सुलभ हैं, उन्हें तो चैतन्यात्मा का भान ही नहीं है, वे तो कषाय में ही मग्न रहते हैं; परन्तु जिन्हें चैतन्यात्मा का भान है और जो चैतन्य की समाधि में स्थिर हुए हैं ह्र ऐसे निजानंद में मग्न वीतरागी संतों को कषाय बहुत दुर्लभ है।
21
गाथा १३१-१३२ : परमसमाधि अधिकार
४१
तात्पर्य यह है कि स्वरूप के आनंद में मग्न संतों के विकार की उत्पत्ति ही नहीं होती ।
अज्ञानी को विषय- कषाय सुलभ हैं और चैतन्य का आनन्द दुर्लभ है तथा ज्ञानी को चैतन्य का आनन्द सुलभ और विषय कषाय दुर्लभ है। अर्थात् उनके चैतन्यानन्द के कारण विकार उत्पत्ति ही नहीं होती । ह्र इसे ही यहाँ अलंकारपूर्वक कहा है। "
इस कलश में सबकुछ मिलाकर एक ही बात कही गई है कि नौ नोकषायजन्य सांसारिक सुख-दुःख, मोहान्ध अज्ञानीजनों को सदा सुलभ ही हैं; किन्तु समाधिनिष्ठ ज्ञानी धर्मात्मा संतगणों को अति दुर्लभ हैं, असंभव है; क्योंकि वे मोहातीत हो गये हैं, सच्ची सामायिक और समाधि उन्हें ही है।
टीकाकार मुनिराज संकल्प करते हैं कि मैं इन सांसारिक सुखदुःख के उत्पादक नोकषायरूप समस्त विकारीभावों का अत्यन्त प्रमोद भाव से त्याग करता हूँ।।२१८ ।।
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १०८१
निजात्मा के प्रति अरुचि ही उसके प्रति अनन्त क्रोध है। जिसके प्रति हमारे हृदय में अरुचि होती है, उसकी उपेक्षा हमसे सहज ही होती रहती है। अपनी आत्मा को क्षमा करने और क्षमा माँगने का मात्र आशय यही है कि हम उसे जानें, पहिचानें और उसी में रम जायें। स्वयं को क्षमा करने और स्वयं से क्षमा माँगने के लिए वाणी की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। निश्चयक्षमावाणी तो स्वयं के प्रति सजग हो जाना ही है। उसमें पर की अपेक्षा नहीं रहती तथा आत्मा के आश्रय से क्रोधादिकषायों के उपशान्त हो जाने से व्यवहारक्षमावाणी भी सहज ही प्रस्फुटित होती है। ह्न धर्म के दशलक्षण, पृष्ठ- १८५