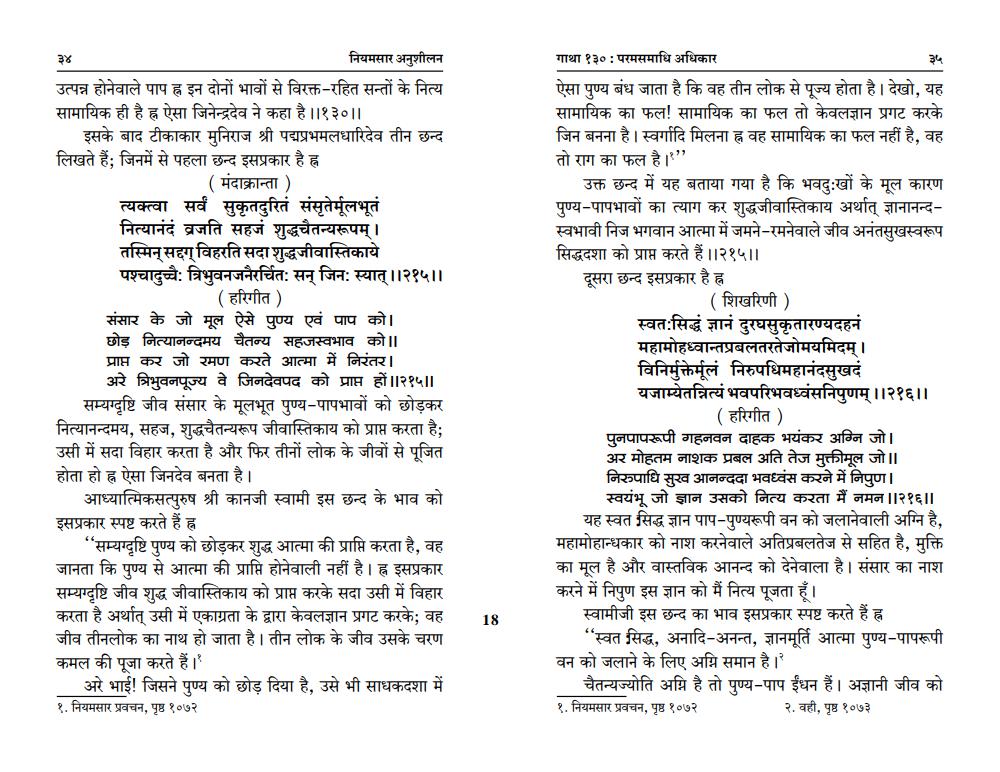________________
३४
नियमसार अनुशीलन उत्पन्न होनेवाले पाप ह्र इन दोनों भावों से विरक्त-रहित सन्तों के नित्य सामायिक ही है ह ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है।।१३०।।
इसके बाद टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव तीन छन्द लिखते हैं, जिनमें से पहला छन्द इसप्रकार है ह्र
(मंदाक्रान्ता ) त्यक्त्वा सर्वं सुकृतदुरितं संसृतेर्मूलभूतं नित्यानंदं व्रजति सहजं शुद्धचैतन्यरूपम् । तस्मिन् सद्द विहरति सदा शुद्धजीवास्तिकाये पश्चादुच्चै: त्रिभुवनजनैरर्चित: सन् जिन: स्यात् ।।२१५।।
(हरिगीत) संसार के जो मूल ऐसे पुण्य एवं पाप को। छोड़ नित्यानन्दमय चैतन्य सहजस्वभाव को। प्राप्त कर जो रमण करते आत्मा में निरंतर।
अरे त्रिभुवनपूज्य वे जिनदेवपद को प्राप्त हों।।२१५|| सम्यग्दृष्टि जीव संसार के मूलभूत पुण्य-पापभावों को छोड़कर नित्यानन्दमय, सहज, शुद्धचैतन्यरूप जीवास्तिकाय को प्राप्त करता है; उसी में सदा विहार करता है और फिर तीनों लोक के जीवों से पूजित होता हो ह ऐसा जिनदेव बनता है।
आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस छन्द के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र ___ “सम्यग्दृष्टि पुण्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है, वह जानता कि पुण्य से आत्मा की प्राप्ति होनेवाली नहीं है। ह्र इसप्रकार सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध जीवास्तिकाय को प्राप्त करके सदा उसी में विहार करता है अर्थात् उसी में एकाग्रता के द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके वह जीव तीनलोक का नाथ हो जाता है। तीन लोक के जीव उसके चरण कमल की पूजा करते हैं। ____ अरे भाई! जिसने पुण्य को छोड़ दिया है, उसे भी साधकदशा में १. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १०७२
गाथा १३० : परमसमाधि अधिकार ऐसा पुण्य बंध जाता है कि वह तीन लोक से पूज्य होता है। देखो, यह सामायिक का फल! सामायिक का फल तो केवलज्ञान प्रगट करके जिन बनना है। स्वर्गादि मिलना ह्न वह सामायिक का फल नहीं है, वह तो राग का फल है।"
उक्त छन्द में यह बताया गया है कि भवदुःखों के मूल कारण पुण्य-पापभावों का त्याग कर शुद्धजीवास्तिकाय अर्थात् ज्ञानानन्दस्वभावी निज भगवान आत्मा में जमने-रमनेवाले जीव अनंतसुखस्वरूप सिद्धदशा को प्राप्त करते हैं ।।२१५।। दूसरा छन्द इसप्रकार है तू
(शिखरिणी) स्वत:सिद्धं ज्ञानं दुरघसुकृतारण्यदहनं महामोहध्वान्तप्रबलतरतेजोमयमिदम् । विनिर्मुक्तेर्मूलं निरुपधिमहानंदसुखदं यजाम्येतन्नित्यं भवपरिभवध्वंसनिपुणम् ।।२१६।।
(हरिगीत ) पुनपापरूपी गहनवन दाहक भयंकर अग्नि जो। अर मोहतम नाशक प्रबल अति तेज मुक्तीमूल जो।। निरुपाधि सुख आनन्ददा भवध्वंस करने में निपण।
स्वयंभू जो ज्ञान उसको नित्य करता मैं नमन ||२१६।। यह स्वत सिद्ध ज्ञान पाप-पुण्यरूपी वन को जलानेवाली अग्नि है, महामोहान्धकार को नाश करनेवाले अतिप्रबलतेज से सहित है, मुक्ति का मूल है और वास्तविक आनन्द को देनेवाला है। संसार का नाश करने में निपुण इस ज्ञान को मैं नित्य पूजता हूँ।
स्वामीजी इस छन्द का भाव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
“स्वत सिद्ध, अनादि-अनन्त, ज्ञानमूर्ति आत्मा पुण्य-पापरूपी वन को जलाने के लिए अग्नि समान है। ____चैतन्यज्योति अग्नि है तो पुण्य-पाप ईंधन हैं। अज्ञानी जीव को १. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १०७२
२. वही, पृष्ठ १०७३
18