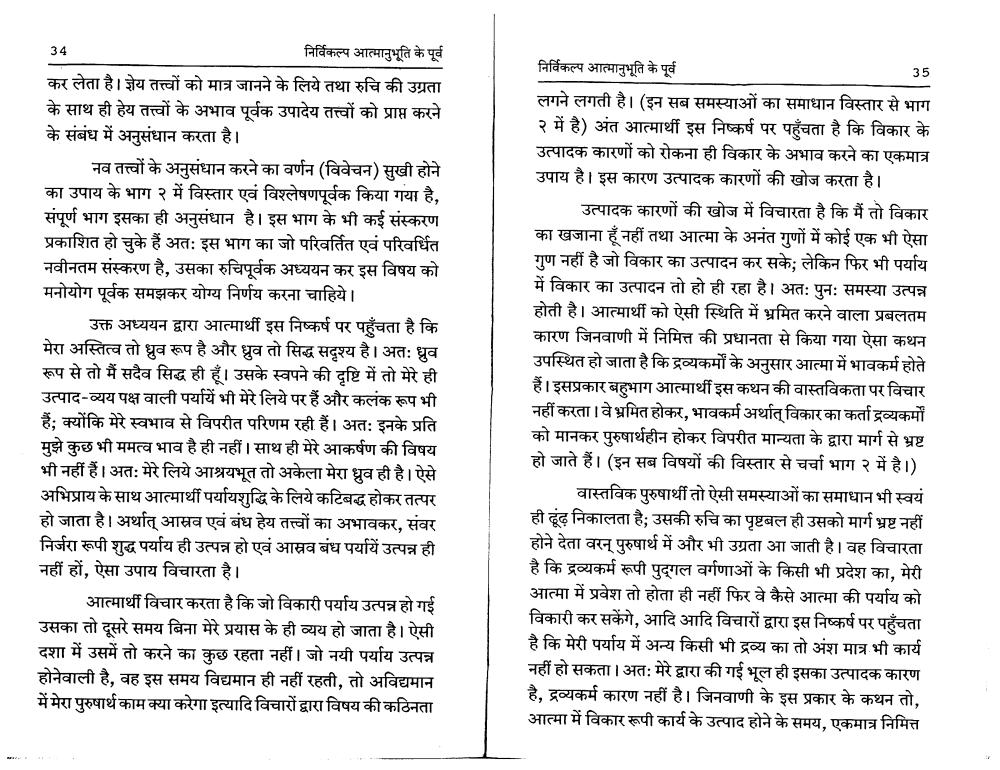________________
34
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व कर लेता है । ज्ञेय तत्त्वों को मात्र जानने के लिये तथा रुचि की उग्रता के साथ ही हेय तत्त्वों के अभाव पूर्वक उपादेय तत्त्वों को प्राप्त करने के संबंध में अनुसंधान करता है।
नव तत्त्वों के अनुसंधान करने का वर्णन (विवेचन) सुखी होने का उपाय के भाग २ में विस्तार एवं विश्लेषणपूर्वक किया गया है, संपूर्ण भाग इसका ही अनुसंधान है। इस भाग के भी कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं अतः इस भाग का जो परिवर्तित एवं परिवर्धित नवीनतम संस्करण है, उसका रुचिपूर्वक अध्ययन कर इस विषय को मनोयोग पूर्वक समझकर योग्य निर्णय करना चाहिये ।
उक्त अध्ययन द्वारा आत्मार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मेरा अस्तित्व तो ध्रुव रूप है और ध्रुव तो सिद्ध सदृश्य है। अतः ध्रुव रूप से तो मैं सदैव सिद्ध ही हूँ। उसके स्वपने की दृष्टि में तो मेरे ही उत्पाद - व्यय पक्ष वाली पर्यायें भी मेरे लिये पर हैं और कलंक रूप भी हैं; क्योंकि मेरे स्वभाव से विपरीत परिणम रही हैं। अतः इनके प्रति मुझे कुछ भी ममत्व भाव है ही नहीं। साथ ही मेरे आकर्षण की विषय भी नहीं हैं। अतः मेरे लिये आश्रयभूत तो अकेला मेरा ध्रुव ही है। ऐसे अभिप्राय के साथ आत्मार्थी पर्यायशुद्धि के लिये कटिबद्ध होकर तत्पर हो जाता है। अर्थात् आस्रव एवं बंध हेय तत्त्वों का अभावकर, संवर निर्जरा रूपी शुद्ध पर्याय ही उत्पन्न हो एवं आस्रव बंध पर्यायें उत्पन्न ही नहीं हों, ऐसा उपाय विचारता है।
आत्मार्थी विचार करता है कि जो विकारी पर्याय उत्पन्न हो गई उसका तो दूसरे समय बिना मेरे प्रयास के ही व्यय हो जाता है। ऐसी दशा में उसमें तो करने का कुछ रहता नहीं। जो नयी पर्याय उत्पन्न होनेवाली है, वह इस समय विद्यमान ही नहीं रहती, तो अविद्यमान
मेरा पुरुषार्थ काम क्या करेगा इत्यादि विचारों द्वारा विषय की कठिनता
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व
35
लगने लगती है। (इन सब समस्याओं का समाधान विस्तार से भाग २ में है) अंत आत्मार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विकार उत्पादक कारणों को रोकना ही विकार के अभाव करने का एकमात्र उपाय है। इस कारण उत्पादक कारणों की खोज करता है।
उत्पादक कारणों की खोज में विचारता है कि मैं तो विकार का खजाना हूँ नहीं तथा आत्मा के अनंत गुणों में कोई एक भी ऐसा गुण नहीं है जो विकार का उत्पादन कर सके; लेकिन फिर भी पर्याय में विकार का उत्पादन तो हो ही रहा है। अतः पुनः समस्या उत्पन्न होती है। आत्मार्थी को ऐसी स्थिति में भ्रमित करने वाला प्रबलतम कारण जिनवाणी में निमित्त की प्रधानता से किया गया ऐसा कथन उपस्थित हो जाता है कि द्रव्यकर्मों के अनुसार आत्मा में भावकर्म होते हैं। इसप्रकार बहुभाग आत्मार्थी इस कथन की वास्तविकता पर विचार नहीं करता। वे भ्रमित होकर, भावकर्म अर्थात् विकार का कर्ता द्रव्यकर्मों को मानकर पुरुषार्थहीन होकर विपरीत मान्यता के द्वारा मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। (इन सब विषयों की विस्तार से चर्चा भाग २ में है ।)
वास्तविक पुरुषार्थी तो ऐसी समस्याओं का समाधान भी स्वयं ही ढूंढ़ निकालता है; उसकी रुचि का पृष्टबल ही उसको मार्ग भ्रष्ट नहीं होने देता वरन् पुरुषार्थ में और भी उग्रता आ जाती है। वह विचारता है कि द्रव्यकर्म रूपी पुद्गल वर्गणाओं के किसी भी प्रदेश का, मेरी आत्मा में प्रवेश तो होता ही नहीं फिर वे कैसे आत्मा की पर्याय को विकारी कर सकेंगे, आदि आदि विचारों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मेरी पर्याय में अन्य किसी भी द्रव्य का तो अंश मात्र भी कार्य नहीं हो सकता । अतः मेरे द्वारा की गई भूल ही इसका उत्पादक कारण है, द्रव्यकर्म कारण नहीं है। जिनवाणी के इस प्रकार के कथन तो, आत्मा में विकार रूपी कार्य के उत्पाद होने के समय, एकमात्र निमित्त